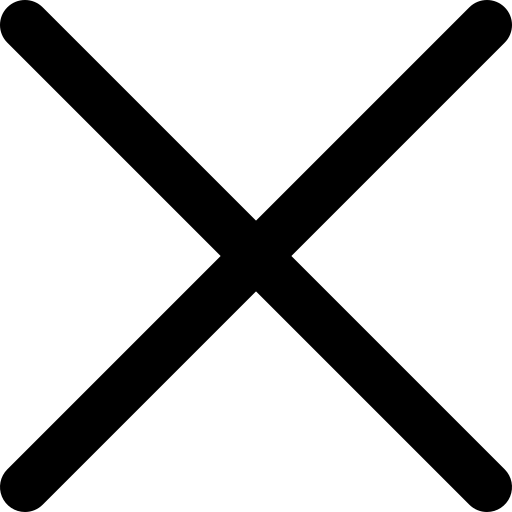डॉ. शुजात अली कादरी
हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की मजार (दरगाह) में गुलाब की खुशबू से सांप्रदायिक सौहार्द की मिठास घुल जाती है. गुलाबी और लाल रंग के गुलाबों से भरी टोकरी लेकर भक्तों के हाथ देश में अमन-चौन की दुआ के साथ प्रार्थना में फैल जाते हैं. सूफी हमीदुद्दीन के आस्ताना-ए-औलिया को जब पुष्कर और तपोस्थली की धूल में खिले गुलाब सूफियों द्वारा भेंट किए जाते हैं, तो धार्मिक दीवारें टूटने लगती हैं. गुलाब का कोई धार्मिक रंग नहीं होता, केवल राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और सद्भावना की सुगंध होती है. गुलाब की महक देश-विदेश में भाईचारे और सूफी का प्रचार कर रही है. नागौर का उर्स हो या अन्य मौकों पर गुलाब के फूलों की अपनी एक अलग ही पहचान होती है.
‘धर्मनिरपेक्ष’ गुलाबों की तरह, ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी भी अपने जीवन में शुद्ध शाकाहारी बने रहे और दरगाह में लोगों को परोसे जाने वाले भोजन की प्रकृति का वर्णन करने वाली वसीयत भी जोड़ दी. तब से पूरे वर्ष परिसर में भक्तों को केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है. यह सूफी-संतों और उनकी आस्थाओं की मिश्रित संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी प्रकाश डालता है.

कहा जाता है कि कुछ गैर-मुस्लिम भक्त ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी के पास आए और पूछा कि जब मांसाहारी भोजन पकाया जाता है, तो वे उनके यहां कैसे आ सकते हैं? ख्वाजा साहब ने तब आदेश दिया कि केवल शाकाहारी भोजन परोसा जाए, जो सभी खा सकें और किसी की धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे. यह नियम ख्वाजा साहब के धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के सम्मान के प्रतीक का वर्णन करता है.
राजस्थान के नागौर में हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतउल्लाह अलैह के उर्स में हर साल नमाज के साथ हजारों तीर्थयात्री आते हैं. दरगाह पूजा के साथ-साथ दरगाह में बने बड़े गुंबद और उसमें की गई शानदार नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है. दरगाह के अंदर प्रवेश करने से पहले शानदार बुलंद दरवाजा दिखाई देता है. इस बुलंद दरवाजे का निर्माण सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था. दरवाजे से अंदर जाने पर मुख्य दरगाह यानी सूफी साहब की मजार पर कोई गुम्बद नहीं मिलता. हालांकि, ज्यादातर दरगाहों में जाने पर मुख्य दरगाह के ऊपर एक गुंबद होता है. कहा जाता है कि पूर्व में कई भक्तों ने इसे बनवाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ. सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे ही अनुयायियों में से एक था.

बुलंद दरवाजा
दरगाह के नायब सज्जादानशीं जमाल अहमद बताते हैं कि सूफी साहब की दरगाह के चमत्कारों को सुनकर सुल्तान तुगलक लाव-लश्कर के साथ यहां पहुंचा था. यहां उन्हें मुख्य मकबरे यानी ख्वाजा हमीदुद्दीन की दरगाह पर गुंबद नहीं दिखा, तो उन्होंने इसे बनवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली. सुल्तान इस बात पर अड़ा था कि वह इसे बनवाएगा, लेकिन इसी दौरान उसे नींद आ गई और उसे फारसी लिपि में एक पत्र मिला. जिस पर लिखा था कि मुझे खुला आसमान और पक्षी पसंद हैं. इसलिए गुंबद बनाने का प्रयास न करें. इसके बाद मुख्य द्वार का बुलंद दरवाजा और दरगाह परिसर की चहारदीवारी बनवाकर सुल्तान निराश लौटा. दरगाह के भीतर अनेक स्थानों विशेषकर बुलंद दरवाजे पर की गई नक्काशी की कलात्मकता और शैली उस काल की निर्माण कला की विशेषताओं को दर्शाती है. दरवाजे पर कुरान की आयत भी खुदी हुई है. सूफी साहब के वंशजों की 22वीं पीढ़ी में नायब सज्जादानशीन जमाल अहमद हैं.

दरगाह
ख्वाजा हमीदुद्दीन का जन्म 588 हिजरी यानी 1139 ई. में दिल्ली में हुआ था. उस समय शहाबुद्दीन गोरी दिल्ली का शासक था. परिवार की दृष्टि से उनका सिलसिला 18 पीढ़ियों के बाद हजरत मोहम्मद साहब उमर फारूक से मिलता है. इस लिहाज से आपको ‘फारूकी’ भी कहा जाता है. सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को अमानुलार्ड, सफी, मोहम्मद, सावली, बलिदान के बादशाह आदि नामों से भी जाना जाता है. सूफी साहब के पिता शेख अहमद तारिक लाहौरी बुखारा से लाहौर आए थे. फिर वह दिल्ली आ गया और यहीं रहने लगे. चालीस साल की उम्र में राजस्थान अलाए सूफी साहब के दो बेटे और दो बेटियां हुईं. सूफी साहब की मृत्यु इस्लामिक वर्ष के चौथे महीने की 28 तारीख को अस्र और मगरिब की नमाज के दौरान हुई थी. उन्होंने कहा कि दरगाह में मोठ बाजरा खिचड़ा, मीठे चावल, आलू चावल, सोयाबीन-चावल, खीर-पूरी आदि शाकाहारी भोजन बनाया जाता है. समाधि के पास एक पेड़ लगा है. इस पेड़ की पत्तियों को जायरीन प्रसाद के रूप में अपने साथ ले जाते हैं.
दरगाह में सुबह तीन से चार बजे तक सूफी साहब की खिदमत होती है. इसके बाद आम लोगों की पूजा शुरू होती है. यहां दिन भर पूजा का दौर चलता रहता है. हर साल उर्स के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से तीर्थयात्री दरगाह आते हैं.
(लेखक भारतीय मुस्लिम छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं.)