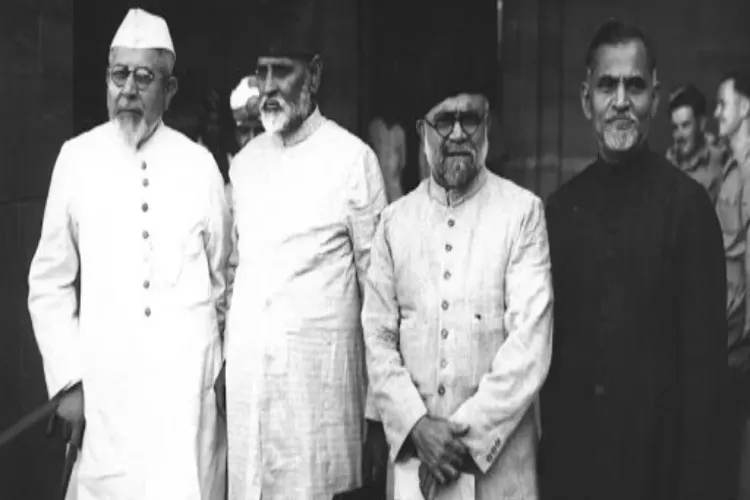
~ अब्दुल्लाह मंसूर
भारत के बंटवारे की कहानी अक्सर सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम टकराव और मुस्लिम लीग की राजनीति तक सीमित कर दी जाती है, लेकिन यह तस्वीर पूरी नहीं है. जब देश बंटवारे की ओर बढ़ रहा था, तब मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था, जो पाकिस्तान के खिलाफ था और मुस्लिम लीग की राजनीति और दावों की खुलकर मुख़ालिफ़त कर रहा था.
इस विरोध को सबसे संगठित और मज़बूती से आवाज़ देने वाला आंदोलन था — मोमिन कॉन्फ्रेंस. यह वही तहरीक थी जिसने सबसे पहले और बुलंद आवाज़ में कहा कि मुसलमान कोई एकसां नहीं हैं, उनमें भी जातीय भेदभाव मौजूद है.
जब चारों ओर पाकिस्तान की बातें हो रही थीं, तब मोमिन कॉन्फ्रेंस ने साफ कहा — "मोमिन जिस ज़मीन पर रहते हैं, वहीं उनका पाक स्थान है, हमें किसी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं."
मोमिन कॉन्फ्रेंस कोई छोटा संगठन नहीं था, बल्कि मेहनतकश, पेशेवर और पसमांदा तबक़ों — यानी निचली मुस्लिम जातियों — से निकला एक मजबूत आंदोलन था. इसका मकसद सिर्फ़ राजनीति करना नहीं था, बल्कि अपने हक़, इज़्ज़त और वतन से मोहब्बत का इज़हार करना था.
भारतीय मुस्लिम समाज में सदियों से जातीय भेदभाव रहा है. अशराफ — यानी सैयद, शेख़, पठान, मुग़ल — खुद को ऊँची नस्ल मानते थे और तालीम, नौकरियों और सत्ता पर कब्ज़ा रखते थे. दूसरी ओर बड़ी तादाद में जुलाहा, राइन, सलमानी, कसाई, दर्ज़ी, कुंजड़, मोची, नाई, लोहार जैसे पेशों से जुड़े तबके थे, जिन्हें नीचा समझा जाता था.
इन्हीं पसमांदा तबकों ने अपने लिए अलग रास्ता चुना और 1926 में कोलकाता में मोमिन कॉन्फ्रेंस की नींव रखी। इसके बीज 1914 में फलाह-उल-मोमिनीन और 1923 में जमाअत-उल-मोमिनीन जैसी कोशिशों से पहले ही बोए जा चुके थे.
आसिम बिहारी ने पसमांदा समाज को संगठित किया, उन्हें उनके हक़ और वजूद का एहसास कराया और यह भी सुनिश्चित किया कि यह संगठन किसी दूसरी पार्टी की बी-टीम न बने। 1928 में कोलकाता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसका मकसद था — यह संगठन सिर्फ जुलाहों यानी अंसारियों का नहीं, बल्कि सभी मजलूम जातियों की आवाज़ बने.
1937 के बाद मुस्लिम लीग ने यह माहौल बनाना शुरू किया कि वह पूरे मुस्लिम समाज की नुमाइंदा है. लेकिन बिहार, यूपी, बंगाल और दिल्ली जैसे इलाकों में मोमिन कॉन्फ्रेंस जमीन पर बेरोज़गारी, शिक्षा, पेशे की सुरक्षा और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ काम कर रही थी.
लीग जहां मज़हबी खतरे की बात करती थी, वहीं मोमिन कॉन्फ्रेंस कहती थी — "हमारा रोज़गार खतरे में है, हमारी जातियों की इज़्ज़त नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं."
कांग्रेस ने जब मुस्लिम जनसंपर्क अभियान शुरू किया, तो गाजीपुर, मिर्जापुर और आसपास के अंसारी तबकों को संगठित किया. नेहरू और डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी मानते थे कि लीग सभी मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, इसलिए मोमिन कॉन्फ्रेंस और जमीयत-उल-उलेमा जैसे संगठनों को आगे लाया गया.
मोमिन कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप भी इन्हीं पसमांदा तबकों से आई। आसिम बिहारी, अब्दुल क़य्यूम अंसारी जैसे नेता पसमांदा घरों से थे, और सलमानी, धुनिया, कसाई, मोची, राइन, रंगरेज़ जैसे तबकों के लोग इसमें शामिल थे। अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने जब लीग का यह ताना सुना कि "अब जुलाहे भी MLA बनने लगे?", तो उन्होंने लीग से किनारा कर लिया.
21 अप्रैल 1940 को पटना में हुई बैठक में पाकिस्तान के विचार को इस्लाम-विरोधी बताया गया और साफ कहा गया कि मोमिन मुस्लिम लीग के साथ नहीं हैं. क़य्यूम अंसारी ने यह भी कहा कि "हम गांधीवादी नहीं हैं, हमला हुआ तो जवाब देंगे." आसिम बिहारी ने साफ किया कि मोमिनों को कोई धार्मिक, भाषाई या सांस्कृतिक डर नहीं है — जहां वे रहते हैं, वही उनका पाकिस्तान है.
27 अप्रैल 1940 को दिल्ली में ‘आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस’ हुई, जिसमें मजलिसे अहरार, खुदाई खिदमतगार, जमीयत अहले हदीस और मोमिन कॉन्फ्रेंस जैसे संगठनों ने हिस्सा लिया.
मोमिन कॉन्फ्रेंस 40,000 बुनकरों के साथ यहां उतरी. लेकिन कांग्रेस ने इनकी चेतावनी को अनदेखा किया और लीग से बातचीत में इन संगठनों को शामिल नहीं किया. यही चूक बंटवारे की ज़मीन बनी.
इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अल्लाह बख़्श सूमरो ने कहा — "धर्म चाहे अलग हो, वतन एक है। नौ करोड़ मुसलमान भारत के बेटे हैं और उन्हें कोई इस ज़मीन से जुदा नहीं कर सकता." मगर जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया, उन्हें इतिहास ने भुला दिया, क्योंकि अंग्रेजों को सिर्फ़ कांग्रेस और लीग से मतलब था.
1936 से 1946 के बीच मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम समाज में एक नई सोच पैदा की. इसने मज़हब के बजाय जाति, रोज़गार और सामाजिक न्याय की बात की. इस आंदोलन ने पसमांदा तबकों को पहचान, इज़्ज़त और राजनीतिक जगह दी। 1946 के चुनावों ने साबित किया कि सारे मुसलमान लीग के साथ नहीं थे.
बिहार, यूपी, बंगाल के आम मुस्लिम — जुलाहे, दर्ज़ी, कसाई, लोहार, नाई, रंगरेज़ — मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ थे. लीग को वही वोट मिले जिनका ताल्लुक़ ज़मींदारों और ऊँची जातियों से था.
उस समय सिर्फ तेरह फीसदी लोगों को वोट देने का हक़ था, और एक रुपया टैक्स देने वाला ही वोटर बन सकता था. अगर सभी पसमांदा मुसलमानों को वोट का अधिकार मिला होता, तो शायद बंटवारा टल सकता था.
मोमिन कॉन्फ्रेंस ने ‘मुसलमान’ की परिभाषा को चुनौती दी और कहा कि इस्लाम के नाम पर जातिवादी हुकूमत मंज़ूर नहीं. पाकिस्तान की मांग असल में अशराफ तबकों की मांग थी, क्योंकि उन्हें डर था कि भारतीय लोकतंत्र में उनके विशेषाधिकार खत्म हो सकते हैं.
यह मांग पसमांदा जातियों के खिलाफ थी, जो सदियों से शोषित थीं. आज जब पसमांदा आंदोलन की बात होती है, तो यह जानना जरूरी है कि इसकी जड़ें मोमिन कॉन्फ्रेंस में हैं.
उस दौर में इनके पास एक मुकम्मल सियासी एजेंडा था — जातीय बराबरी, संसाधनों की न्यायपूर्ण तक्सीम और लोकतांत्रिक भागीदारी। उनका कहना था — "मज़हब हमारे लिए अहम है, मगर उससे ज़्यादा अहम हमारी इज़्ज़त, हमारी रोज़ी और हमारा वतन है."
अगर आज भारत एक सेकुलर देश है, तो उसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस की भी एक मजबूत भूमिका है. जिसे सियासत ने भुला दिया, इसलिए आज इसे फिर से याद करना ज़रूरी है.
(लेखक पसमांदा चिंतक हैं )
