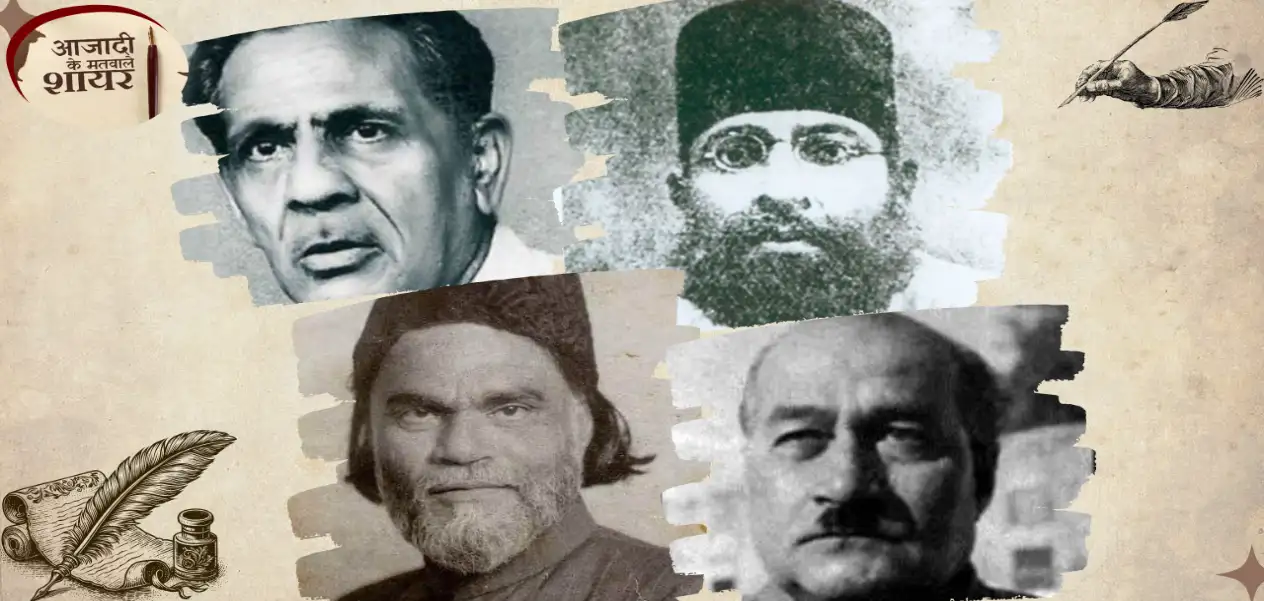
ज़ाहिद ख़ान
मुल्क की आज़ादी लाखों-लाख लोगों की क़ुर्बानियों का नतीजा है. जिसमें लेखक, कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों ने भी अहम रोल निभाया. उर्दू अदब के बड़े शायर आज़ादी के आंदोलन में पेश-पेश रहे. मौलाना हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलीहाबादी और फ़िराक़ गोरखपुरी जैसे क़द—आवर शायर अपने अदब और तख़्लीक़ के ज़रिए आज़ादी की तहरीक में हिस्सा ले रहे थे.
दर हक़ीक़त यह है कि इन शायरों की ग़ज़ल, नज़्मों ने मुल्क में आज़ादी के हक़ में एक समां बना दिया. अवाम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ गोलबंद हो गई.
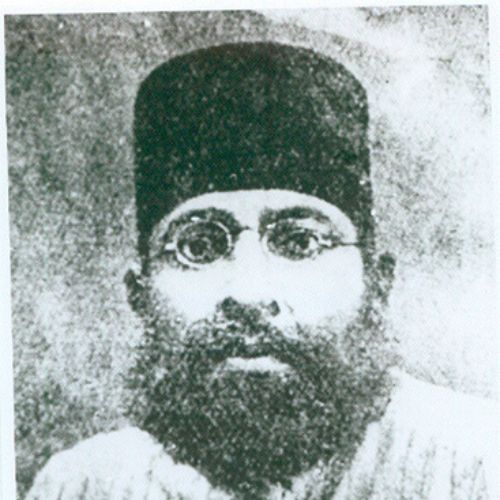 मौलाना हसरत मोहानी
मौलाना हसरत मोहानी
मौलाना हसरत मोहानी वह शख़्स थे, जिनके ख़यालात बड़े इंक़लाबी थे. उन्होंने उस ज़माने में सहाफ़त और क़लम की अहमियत को पहचाना और साल 1903 में अलीगढ़ से एक सियासी-अदबी रिसाला ‘उर्दू-ए-मुअल्ला’ निकाला. जिसमें अंग्रेज़ी हुकूमत की पॉलसियों की सख़्त तनक़ीद की जाती थी.
इस मैगज़ीन में हसरत मोहानी ने हमेशा आज़ादी—पसंदों के लेखों, शायरों की इंक़लाबी ग़ज़लों-नज़्मों को तरजीह दी, जिसकी वजह से वे अंग्रेज़ सरकार की आंखों में खटकने लगे.
साल 1907 में अपने एक मज़मून में मौलाना हसरत मोहानी ने सरकार की तीख़ी आलोचना कर दी. जिसके एवज़ में उन्हें जेल जाना पड़ा और सज़ा, दो साल क़ैद-ए-बा-मशक़्क़त. जिसमें उनसे रोज़ाना एक मन गेहूँ पिसवाया जाता था. क़ैद के हालात में ही उन्होंने अपना यह मशहूर शे’र कहा था--
है मश्क़-ए-सुख़न जारी, चक्की की मशक़्क़त भी
इक तुर्फ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी.
साल 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने न सिर्फ़ ‘इंक़लाब जिंदाबाद’ नारा दिया, बल्कि अहमदाबाद में हुए कांग्रेस सम्मलेन में 'आज़ादी—ए—कामिल’ यानी पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी रखा.
कांग्रेस की उस ऐतिहासिक बैठक में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफ़ाक़उल्ला ख़ॉं के साथ-साथ कई और क्रांतिकारी भी मौजूद थे. महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया.
बावजूद इसके हसरत मोहानी ‘पूर्ण स्वराज्य’ का नारा बुलंद करते रहे. आख़िरकार यह प्रस्ताव साल 1929 में पारित हुआ. शहीद—ए—आज़म भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद समेत तमाम इंक़लाबियों ने आगे चलकर मौलाना हसरत मोहानी के नारे ‘इंक़लाब जिंदाबाद’ की अहमियत समझी और देखते-देखते यह नारा आज़ादी की लड़ाई में मक़बूल हो गया.
एक समय आलम यह था कि देश भर में बच्चे-बच्चे की ज़बान पर यह नारा था. इस बात का भी बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि महात्मा गांधी को स्वदेशी आंदोलन की राह मौलाना हसरत मोहानी ने ही सुझाई थी. ख़ुद उन्होंने इसका ख़ूब प्रचार-प्रसार किया. यहॉं तक कि एक खद्दर भण्डार भी खोला, जो कि बहुत मक़बूल हुआ था.
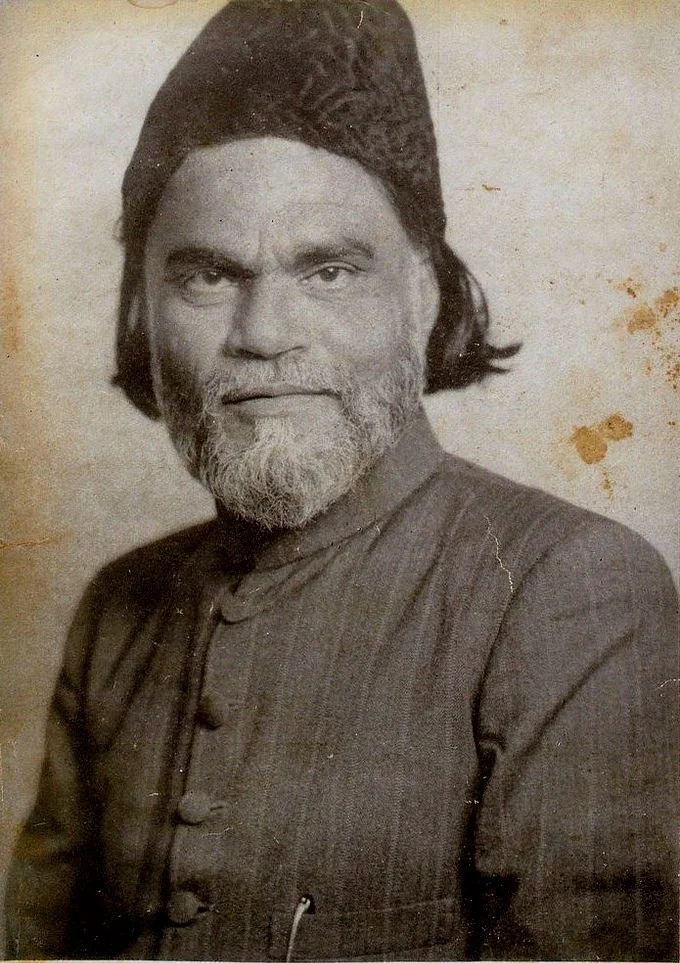 जिगर मुरादाबादी
जिगर मुरादाबादी
ग़ज़ल के शहंशाह जिगर मुरादाबादी ने सिर्फ़ इश्क़-ओ-मुहब्बत, विसाल—ओ—फ़िराक़ को ही अल्फ़ाज़ों में नहीं ढाला, अपने आख़िरी समय में वे ज़िंदगी की हक़ीक़तों के क़रीब आये और अपने वक़्त के बड़े मसाइल को ग़ज़ल का मौज़ूअ बनाया. बंगाल के भयानक अकाल पर उन्होंने ‘क़हत-ए-बंगाल’ जैसी दिल-दोज़ नज़्म लिखी--
बंगाल की मैं शाम-ओ-सहर देख रहा हूँ
हर चंद कि हूँ दूर मगर देख रहा हूँ
इफ़्लास की मारी हुई मख़्लूक़ सर-ए-राह
बे-गोर-ओ-कफ़न ख़ाक-ब-सर देख रहा हूँ.
तो वहीं साल 1946-47 में जो देशव्यापी फ़िरक़ावाराना फ़सादात हुए, उसने जिगर मुरादाबादी की रूह को ज़ख़्मी कर दिया. इन परेशान—कुन हालात को उन्होंने अपनी ग़ज़ल में कुछ इस तरह से पिरोया--
फ़िक्र-ए-जमील ख़्वाब-ए-परेशाँ है आज-कल
शायर नहीं है वो, जो ग़ज़ल-ख्वाँ है आज-कल
इंसानियत के जिससे इबारत है ज़िंदगी
इंसां के साये से भी गुरेज़ाँ है आज—कल
दिल की जराहतों के खिले हैं चमन-चमन
और उसका नाम फ़स्ल-ए-बहाराँ है आज—कल.
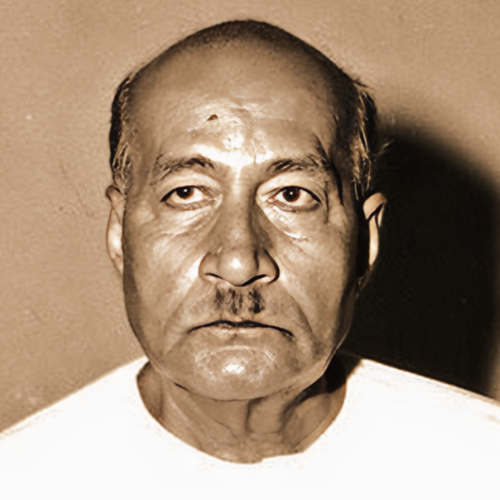 जोश मलीहाबादी
जोश मलीहाबादी
उर्दू अदब में जोश मलीहाबादी वह आला नाम है, जो अपने इंक़लाबी कलाम से 'शायर-ए-इंक़लाब' कहलाए. जोश मलीहाबादी की ज़िंदगानी का इब्तिदाई दौर, मुल्क की ग़ुलामी का दौर था। ज़ाहिर है कि इस दौर के असरात उनकी शायरी पर भी पड़े.
हुब्ब-उल-वतनी और बग़ावत उनके मिज़ाज का हिस्सा बन गई. उनकी एक नहीं, कई ऐसी कई ग़ज़लें-नज़्में हैं, जो वतन—परस्ती के रंग में रंगी हुई हैं. ‘मातम—ए-आज़ादी’, ‘निज़ाम—ए—लौ’, ‘इंसानियत का कोरस’, ‘ज़वाल—ए—जहाँ-बानी’ के नाम अव्वल नम्बर पर लिए जा सकते हैं--
जूतियॉं तक छीन ले इंसान की जो सामराज
क्या उसे यह हक़ पहुचता है कि रक्खे सर पै ताज.
इंक़लाब और बग़ावत में डूबी हुई जोश की ये ग़ज़लें-नज़्में, जंग-ए-आज़ादी के दौरान नौजवानों के दिलों में गहरा असर डालती थीं. वे आंदोलित हो उठते थे. यही वजह है कि जोश मलीहाबादी को अपनी इंक़लाबी ग़ज़लों-नज़्मों के चलते कई बार जेल भी जाना पड़ा.
लेकिन उन्होंने अपना मिज़ाज और रहगुज़र नहीं बदली. दूसरी आलमी जंग के दौरान जोश मलीहाबादी ने ‘ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़रजंदों के नाम’, ‘वफ़ादारान—ए-अजली का पयाम शहंशाह—ए-हिंदोस्तॉं के नाम’ और ‘शिकस्त—ए-जिंदॉं का ख़्वाब’ जैसी साम्राज्यवाद विरोधी नज़्में लिखीं--
क्या हिन्द का ज़िंदाँ काँप रहा है गूँज रही हैं तक्बीरें
उकताए हैं शायद कुछ क़ैदी और तोड़ रहे हैं ज़ंजीरें.
जोश के कलाम में सियासी चेतना साफ़ दिखलाई देती है और यह सियासी चेतना मुल्क की आज़ादी के लिए इंक़लाब का आहृान करती है.

रघुपति सहाय उर्फ़ फ़िराक़ गोरखपुरी
शायर—ए—आज़म रघुपति सहाय उर्फ़ फ़िराक़ गोरखपुरी भी अपनी अदबी ज़िंदगी के आग़ाज़ में ही आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए थे. साल 1920 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा की मुख़ालफ़त के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था.
वे इस ज़ुर्म में ढाई साल तक आगरा और लखनऊ की जेलों में रहे. फ़िराक़ गोरखपुरी ने गु़लाम मुल्क में किसानों-मज़दूरों के दुःख-दर्द को समझा और अपनी शायरी में उनको आवाज़ दी. जोश मलीहाबादी की तरह उनकी इन नज़्मों का फ़लक बड़ा होता था. मज़दूरों का आहृान करते हुए वे लिखते हैं--
तोड़ा धरती का सन्नाटा किसने ? हम मज़दूरों ने
डंका बजा दिया आदम का किसने ? हम मज़दूरों ने
इसी तरह वे अपनी नज़्म ‘धरती की करवट’ में किसानों को भी ख़िताब करते हैं. फ़िराक़ गोरखपुरी के कलाम में साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और साम्प्रदायिकता की मुख़ालफ़त साफ़ दिखलाई देती है--
बेकारी, भुखमरी, लड़ाई, रिश्वत और चोरबज़ारी
बेबस जनता की यह दुर्गत, सब की जड़ सरमायादारी.
फ़िराक़ गोरखपुरी की किताब ‘गुल—ए—नग़्मा’ में इस तरह की ग़ज़लें और नज़्में इफ़रात में हैं. साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ कई नज़्मों में उनका लहज़ा काफी तल्ख़ भी हो जाता है. उनकी ऐसी ही एक नज़्म का मुलाहिज़ा करें--
ये सब मर्दखोर हैं साथी इनके साथ मुरव्वत कैसी
यह दुनिया है इनकी मिलकिय्यत इस दुनिया की ऐसी तैसी
दुनिया भर बाज़ार है जिसका इक मंडी हेराफेरी की
उस अमेरिका की यह हालत यह बेकारी धत तेरे की.
 लेखक के बारे में : भारतीय साहित्य में चले प्रगतिशील आंदोलन पर लेखक, पत्रकार ज़ाहिद ख़ान का विस्तृत कार्य है. उनकी कुछ अहम किताबों की फ़ेहरिस्त इस तरह है-‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’, ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र’, ‘तहरीक-ए-आज़ादी और तरक़्क़ीपसंद शायर’ और ‘आधी आबादी अधूरा सफ़र’. ज़ाहिद ख़ान ने कृश्न चंदर के ऐतिहासिक रिपोर्ताज ‘पौदे’, अली सरदार जाफ़री का ड्रामा ‘यह किसका ख़ून है’ और हमीद अख़्तर की किताब ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ का उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण किया है. ‘शैलेन्द्र हर ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर में’ और ‘बलराज साहनी एक समर्पित और सृजनात्मक जीवन’ किताबों का संपादन भी उनके नाम है. उनकी चर्चित किताब ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’ मराठी और उर्दू ज़़बान में अनुवाद हो, प्रकाशित हो चुकी हैं. इस किताब के लिए उन्हें ‘मध्य प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ के ‘वागीश्वरी पुरस्कार’ से भी नवाज़ा गया.
लेखक के बारे में : भारतीय साहित्य में चले प्रगतिशील आंदोलन पर लेखक, पत्रकार ज़ाहिद ख़ान का विस्तृत कार्य है. उनकी कुछ अहम किताबों की फ़ेहरिस्त इस तरह है-‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’, ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र’, ‘तहरीक-ए-आज़ादी और तरक़्क़ीपसंद शायर’ और ‘आधी आबादी अधूरा सफ़र’. ज़ाहिद ख़ान ने कृश्न चंदर के ऐतिहासिक रिपोर्ताज ‘पौदे’, अली सरदार जाफ़री का ड्रामा ‘यह किसका ख़ून है’ और हमीद अख़्तर की किताब ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ का उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण किया है. ‘शैलेन्द्र हर ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर में’ और ‘बलराज साहनी एक समर्पित और सृजनात्मक जीवन’ किताबों का संपादन भी उनके नाम है. उनकी चर्चित किताब ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’ मराठी और उर्दू ज़़बान में अनुवाद हो, प्रकाशित हो चुकी हैं. इस किताब के लिए उन्हें ‘मध्य प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ के ‘वागीश्वरी पुरस्कार’ से भी नवाज़ा गया.
