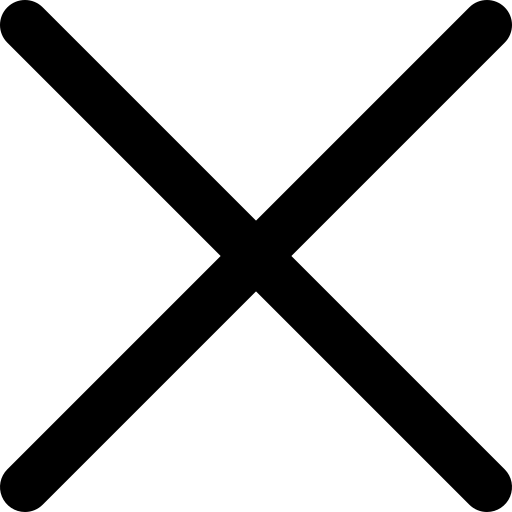अजित राय
मुंबईया सिनेमा में अपने अभिनय की खास अदा के लिए मशहूर यशपाल शर्मा की हरियाणवी फिल्म 'दादा लखमी' अपने सिनेमाई मुहावरे में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म है. 74वें कान में प्रदर्शन के साथ ही 'दादा लखमी' दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कान फिल्म समारोह (फिल्म बाजार) में दिखाई जानेवाली पहली हरियाणवी फिल्म बन गई है.
हरियाणवी सिनेमा के इतिहास में बहुत कम फिल्में ऐसी बनी है जिन्हें हम याद कर सकते हैं. जयंत प्रभाकर के निर्देशन में बनी 'चंद्रावल'(1984) को हरियाणवी की पहली सफल फिल्म माना जाता है जिसके लेखक और निर्माता थे देवीशंकर प्रभाकर.
हरियाणा की एक घूमंतू जनजाति गाड़िया लोहार की लड़की और एक जाट नौजवान की इस दुखांत प्रेम कथा को हरियाणा से बाहर दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि दूसरे राज्यों में भी काफी पसंद किया गया था. इसके बाद हरियाणवी में कई फिल्में बनी लेकिन कोई भी चर्चित नहीं रही. उसके सोलह साल बाद हरियाणवी सिनेमा की चर्चा तब शुरू हुई जब अश्विनी चौधरी की फिल्म 'लाडो' (2000) को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.
इसके चौदह साल बाद राजीव भाटिया की हरियाणवी फिल्म 'पगड़ी दि आनर' (2014) को भी दो-दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले. लेकिन यशपाल शर्मा की 'दादा लखमी' इन सारी फिल्मों से इसलिए अलग है कि यह सिनेमा का एक नया मुहावरा गढ़ती है और इसे बनाने में किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है.
राजेंद्र गुप्ता, यशपाल शर्मा, मेघना मलिक आदि ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. उत्तम सिंह का संगीत बेजोड़ है और फिल्म के आख्यान के साथ ऐसा घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं है कि इसे अलग से डाला गया है. एक-एक फ्रेम में हरियाणा के ग्रामीण जीवन और संस्कृति किसी यथार्थवादी पेंटिंग्स की तरह दिखाई देते है.
हरियाणा के सोनीपत जिले के जंतीकलां गांव में एक साधारण किसान के घर जन्मे पंडित लखमी चंद (1903-1945) परिवार की मर्जी के खिलाफ संगीत और कविता की दुनिया में गए और अपनी अद्वितीय प्रतिभा के कारण अमर हो गए. उस जमाने में संस्कृतिकर्म करने वालों को समाज में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था.
हिंदू समाज में तो उंची जातियों के लोगों के लिए तो यह काम प्रतिबंधित ही था. ऐसे में पंडित लखमीचंद को अपने ब्राह्मण समाज में कितना विरोध झेलना पड़ा होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है.
निरक्षर होने के बावजूद उन्होंने पारंपरिक लोकनाट्य विधा 'सांग' को नई ऊंचाई दी और दर्जनों 'सांगो' और रागिनियों की रचना की. आज उन्हें हरियाणा का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आइकन माना जाता है. उनके नाम पर कई पुरस्कार और संस्थाएं हैं जिनमें रोहतक का फिल्म विश्वविद्यालय भी एक है- लखमीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफार्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स.
फिल्म के इस पहले भाग में 1903-1924-25 तक के करीब बीस-बाईस साल के कालखंड को दिखाया गया है.
यशपाल शर्मा के निर्देशन में यह पहली फिल्म है जिसे बनाने में उन्होंने जुनून की हद तक अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया है. वे खुद हरियाणा के हिसार शहर से हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय होते हुए मुंबईया सिनेमा में गए हैं.
वे ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर आदि दिग्गज अभिनेताओं की परंपरा के कलाकार हैं
हालांकि सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बाद भी मुंबईया सिनेमा में उनकी अद्वितीय अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल होना अभी बाकी है जैसा कि राजन कोठारी की फिल्म 'दास कैपिटल' में हमने देखा है.
थियेटर से जुड़े रहने के कारण उन्होंने इस फिल्म में अपने अभिनेताओं से उम्दा काम करवाया है और जगह-जगह पर मेलोड्रामा की अति से बचे हैं. कहानी में करुणा स्वाभाविक रूप से हवा में नमी की तरह अंत तक बनी रहती है.
'चलो उस देश में जहां संगीत हो ' गाने का मुखड़ा बार बार बजता है और हमारे समय की हृदयविदारक संस्कृतिविहीनता के बारे में निर्देशक को अलग से कोई टिप्पणी नही करनी पड़ती.
फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि दादा लखमी चंद का अंतिम समय आ गया है. वे घर के आंगन में खटिया पर लेटे हैं. सारा गांव वहां इकट्ठा है. वे आंखें खोलते हैं और अंतिम यात्रा के लिए थोड़ी मदिरा की मांग करते हैं. वे गांववालों से कहते हैं कि मातम मत करो, जश्न मनाओ. वे अपनी प्रिय रागिनी 'लखमीचंद का ब्रह्मज्ञान' गाने लगते हैं जो कुछ कुछ कबीर के निर्गुण 'साधो यह मुर्दों का गांव' की तरह गूंजता है.
यहां से फिल्म फ्लैश बैक में लखमीचंद के बचपन में ले जाती है जहां उन्हें सांगी बनने के लिए कई स्तरों पर यातना, संघर्ष और सपनों से गुजरना पड़ता है. चौबोले सीखने के लिए एक नकली कवि के घर नौकर बनकर रहना पड़ता है तो अंधे संत मानसिंह का शिष्य बनना पड़ता है.
सांग मंडली में गाना और नाचना सीखने के लिए उन्हें झाड़ू लगाने से लेकर खाना बनाने तक का काम करना पड़ता है. जब वे सफल होने लगते हैं तो उनके प्रतिद्वंद्वी खाने में पारा मिलाकर दे देते हैं और वे बोलने और गाने की क्षमता खो देते हैं.
बड़ी मुश्किल से लंबे इलाज के बाद उनका गला ठीक होता है. वे अपनी सांग मंडली बनाते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते. यह वहीं समय है जब देश में आजादी का आंदोलन परवान चढ़ रहा है और जिसकी कमान महात्मा गांधी के हाथों में आ चुकी है.
फिल्म में कई मजेदार दृश्य हैं. देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है. पंडित जवाहरलाल नेहरू हरियाणा में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं. उसी रास्ते से पंडित लखमीचंद का काफिला गुजरात है. वे नेहरू के सुरक्षा गार्ड से गुजारिश करते हैं कि उन्हें पंडित जी से मिलने दे. वह इन्हें मना कर देता है. लखमीचंद अपने काफिले में आकर रागिनी गाने लगते हैं और सारी भीड़ पंडित नेहरू का भाषण छोड़कर उनका गाना सुनने लगती है.
दरअसल हरियाणा के इस सांस्कृतिक आइकन के बारे में बहुत कम प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है. लखमीचंद इतिहास से अधिक किंवदंतियों में जीवित हैं. ऐसे व्यक्ति पर फिल्म बनाना, वह भी दो खंडों में, जोखिम भरा हो सकता था.
यशपाल शर्मा ने अपने सिनेमाई बर्ताव में सावधानी, संजीदगी और संवेदनशीलता से काम लिया है. फिल्म में एक संवाद आता है, "तानसेन तो बहुत हुए कभी कभी कानसेन भी बन जाया करो."