
अब्दुल्लाह मंसूर
आज का स्कूल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है.छात्र सुबह से शाम तक अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल में बिताते हैं.यह जगह हमें किताबें, गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाती है, लेकिन क्या यह हमें सच में जीना भी सिखाती है? अगर हम ईमानदारी से सोचें तो पाएंगे कि स्कूल हमें अक्सर मशीन की तरह बना देता है.वहाँ हर दिन घंटी बजती है. बच्चे एक कतार में बैठते हैं.
सबको एक जैसा यूनिफॉर्म पहनना होता है. सबके लिए वही पाठ्यक्रम होता है.यह व्यवस्था हमें ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करती है जो समाज में फिट हो जाए, नौकरी कर सकेऔर औसत तरीके से ज़िंदगी जी सके.पर इसमें हमारी असली पहचान, हमारी मौलिकता दब जाती है.
स्कूल की यह व्यवस्था दरअसल औद्योगिक क्रांति के समय बनी थी.जब फैक्ट्रियाँ चल रही थीं, तब समाज को अनुशासित, समय पर काम करने वाले और आदेश मानने वाले लोग चाहिए थे.
इसलिए स्कूल का मॉडल फैक्ट्री जैसा बना दिया गया.बच्चों को एक ही जगह बैठा कर, टुकड़ों में बँटी पढ़ाई कराई जाने लगी.परीक्षा और ग्रेड पर ज़ोर दिया गया ताकि सबको एक ही पैमाने पर नापा जा सके.इस प्रक्रिया में यह भूल गया कि हर बच्चा अलग है. हर बच्चे की प्रतिभा अलग है.स्कूल बच्चों को खोजने का अवसर नहीं देता.उन्हें तयशुदा रास्ते पर ढकेल देता है.
सोचिए, छोटा बच्चा रोज़ सौ सवाल करता है.उसकी आँखों में हर चीज़ के प्रति जिज्ञासा चमकती है.लेकिन जैसे ही वह स्कूल व्यवस्था की चारदीवारी में आता है, यह जिज्ञासा धीरे-धीरे दबने लगती है.क्यों ?
क्योंकि वहाँ अनुशासन को इनाम मिलता है और सवालों को बगावत समझा जाता है.जिज्ञासा अनुशासन को तोड़ती है. यह बच्चे को चीज़ों को अलग नज़र से देखने और नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है.

मगर पाठ्यक्रम पहले से तय है. समय कम है.परीक्षा उसी पाठ्यक्रम पर आधारित है.शिक्षक पर दबाव है कि सिलेबस समय पर खत्म होऔर बच्चे पर दबाव है कि अच्छे अंक लाए.ऐसे माहौल में सवाल पूछना बोझ बन जाता है.
धीरे-धीरे बच्चा सीख जाता है.पूछने से फायदा नहीं है.चुप रहना और वही दोहराना बेहतर है जो किताब या शिक्षक कहते हैं.और जब यह आदत गहरी हो जाती है, तब वह बच्चा केवल यही सवाल करता है—"सर, यह परीक्षा में आएगा या नहीं ?"
उसकी सोच सीमित हो जाती है. सीखने की असली आग बुझ जाती है.यही सबसे खतरनाक स्थिति है.सवालों के बिना ज्ञान सिर्फ रटंत बन जाता है.इंसान की कल्पना और आलोचनात्मक क्षमता खत्म हो जाती है.
स्कूल व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि यह मौलिकता को दबा देती है.बच्चे अपनी असली प्रतिभा को भूल जाते हैं.उन्हें सिखाया जाता है कि "दूसरों की तरह बनो."
अगर तुम अलग सोचोगे तो असफल हो जाओगे.अगर तुम प्रयोग करोगे तो ग्रेड खराब होंगे.इसीलिए बच्चे असफल होने से डरते हैं.वे अपनी असली पहचान खोजने की जगह दूसरों को कॉपी करने लगते हैं.जीवन का अर्थ खोजने की जगह वे सिर्फ़ प्रमाण और वैलिडेशन चाहते हैं.

पूरी ज़िंदगी वे दूसरों से यह सुनना चाहते हैं कि "तुम ठीक हो, तुम सफल हो." लेकिन अंदर से वे खाली रह जाते हैं.यहाँ हमें एक गहरी बात समझनी चाहिए.
दार्शनिक नीत्शे ने कहा था.जब हम समाज के मूल्यों को अपनी आत्मा पर हावी होने देते हैं,हम अपने आप से कट जाते हैं.हम अपनी कहानी के लेखक नहीं रहते.दूसरों की कहानी में किरदार बन जाते हैं.यही स्कूल व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है.यह हमें खुद को खोजने नहीं देती.
ब्राज़ील के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पाउलो फ्रेरे ने कहा था.हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को बस रटाने और चुपचाप मान लेने की आदत डालती है.उन्होंने इसे "बैंकिंग मॉडल" कहा.जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं, वैसे ही शिक्षक बच्चों के दिमाग़ में जानकारी जमा कर देते हैं.
बच्चा बस उसे याद करता है.दोहराता है.इसमें बच्चे को सोचने, सवाल करने या अपने नज़रिए से देखने की जगह नहीं मिलती.नतीजा,बच्चे नियम मानने वाले और आज्ञाकारी तो बन जाते हैं, नए विचार लाने वाले या समाज को बदलने वाले नहीं बन पाते.ऐसी शिक्षा व्यवस्था से सत्ता और व्यवस्था मज़बूत होती है.लोग सवाल करना भूल जाते हैं.

फ्रेरे ने इसके बिल्कुल उलट "स्वातंत्र्यवादी शिक्षा" की बात की.इसमें शिक्षक और छात्र दोनों बराबर होते हैं.शिक्षक सिर्फ़ आदेश देने वाला नहीं होता.छात्र भी केवल सुनने वाला नहीं रहता.
दोनों मिलकर बातचीत करते हैं. सवाल उठाते हैं.सोचते हैं.इससे ज्ञान एकतरफ़ा नहीं बल्कि साझा हो जाता है.यही असली शिक्षा है, जो बच्चों को आज़ाद करती है, उन्हें अपनी सोच का मालिक बनाती है और उन्हें यह हिम्मत देती है कि वे अपनी ज़िंदगी और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें.
इसका मतलब यह नहीं है कि हमें स्कूल छोड़ देना चाहिए.हमें यह समझना होगा कि स्कूल व्यवस्था की कुछ सीमाएँ हैं.स्कूल हमें आधारभूत ज्ञान और अनुशासन देता है.
शिक्षा यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.असली शिक्षा तब होती है जब बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है. कला, संगीत, खेल और साहित्य से जीवन की गहराई समझता है.
समाज से जुड़कर संवेदनशील बनता है.अपनी गलतियों से आगे बढ़ना सीखता है.यही वजह है कि आज ज़रूरी है हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधार करें.
नई शिक्षा नीति (NEP 2020) इसी दिशा में एक कदम है, जिसमें केवल रटंत और परीक्षा आधारित पढ़ाई पर ज़ोर न देकर, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, व्यावहारिक ज्ञान और बच्चों की रुचियों को महत्व देने की बात की गई है.यह हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक लाना नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाना है.
जीवन का असली अर्थ भी यही है – खुद को खोजना.विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि अगर इंसान के पास जीने का कारण हो, तो वह किसी भी परिस्थिति में जी सकता है.
इसलिए हमें खुद से पूछना होगा – मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? अगर हम यह सवाल खोज पाएँ तो हमारी शिक्षा सफल हो जाएगी.
हमें यह भी समझना होगा कि मन और शरीर का रिश्ता गहरा है.स्कूल व्यवस्था दिमाग़ पर बहुत ध्यान देती है, लेकिन भावनाओं, अनुभवों और इच्छाओं को नज़रअंदाज़ कर देती है.जबकि इंसान केवल दिमाग़ से नहीं बनता, वह दिल और आत्मा से भी बनता है.
इसलिए हमें अपनी भावनाओं को सुनना होगा, अपने अनुभवों को अपनाना होगा.हमें यह अनुमति देनी होगी कि हम गलती कर सकते हैं, असफल हो सकते हैं.यही सीखने की प्रक्रिया है। स्कूल हमें यह झूठ सिखाता है कि एक बार मौका चला गया तो कभी नहीं मिलेगा.पर सच यह है कि सही काम करने के लिए कभी गलत समय नहीं होता.
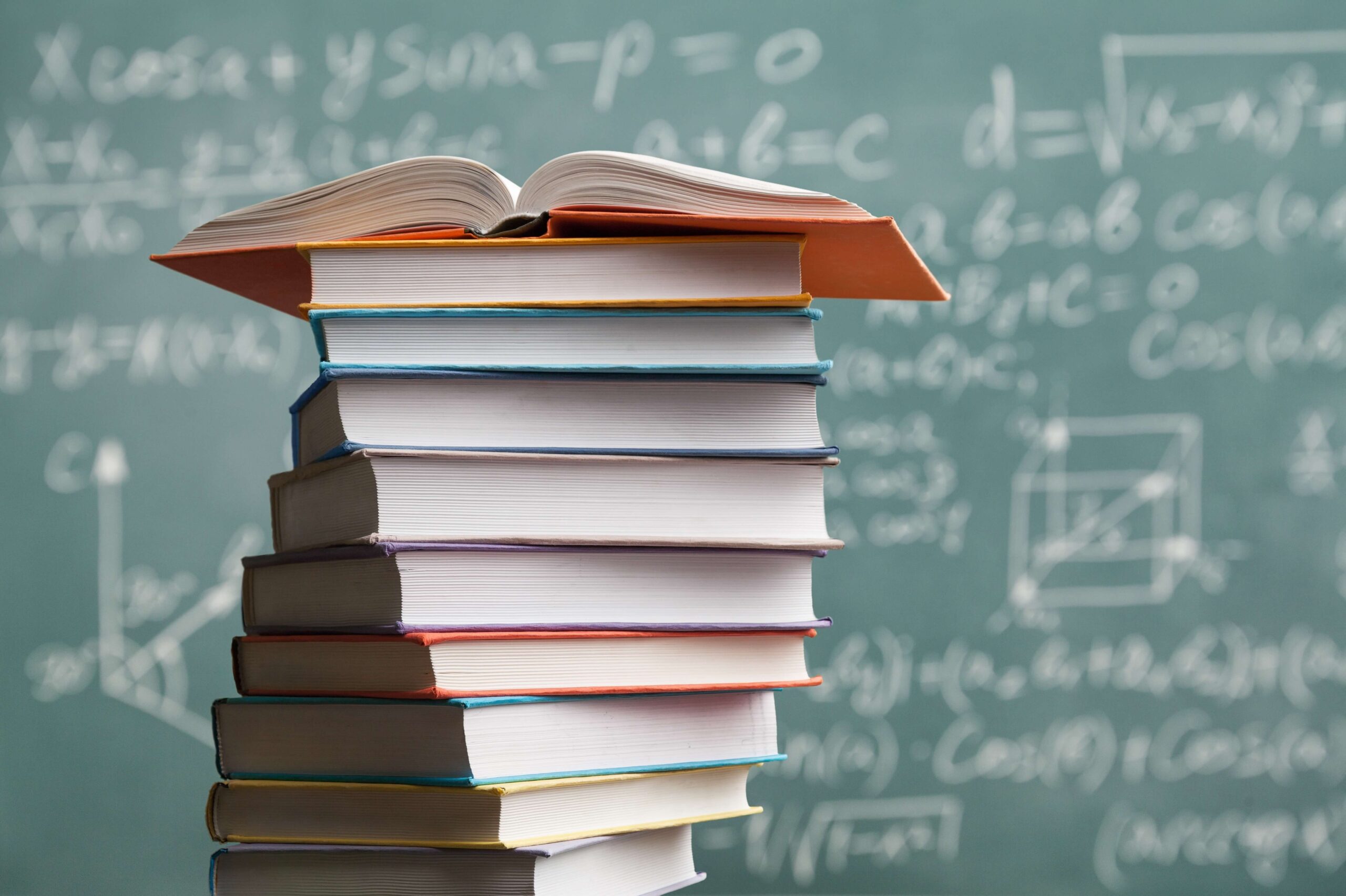
अगर हमें इस व्यवस्था को बदलना है तो हमें नए तरीके अपनाने होंगे.शिक्षा को परीक्षा और ग्रेड तक सीमित नहीं किया जा सकता.शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए.
शिक्षा का मतलब है – सोचने की ताकत, आलोचनात्मक दृष्टि और सृजनात्मकता.हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि सवाल पूछना उनकी ताकत है, न कि कमजोरी। हमें यह मानना होगा कि हर बच्चा अलग है और हर बच्चा अपनी तरह से सीखता है.
हमें यह याद रखना चाहिए कि स्कूल भले ही हमारी मौलिकता को दबा दे, लेकिन हमारी असली पहचान को हम खुद खोज सकते हैं.ग्रेड कम आ जाएँ तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेड हमारी पूरी ज़िंदगी का पैमाना नहीं हैं.
हो सकता है कि स्कूल आपको सिर्फ़ अंकों में मापे, लेकिन ज़िंदगी आपको आपके सवालों, आपके सपनों और आपकी सच्चाई से आँकती है.असली शिक्षा वही है जो हमें अपनी मौलिकता खोजने का साहस दे और हमें यह याद दिलाए कि हम अपनी कहानी के लेखक हैं, किसी और के किरदार नहीं.जब हम खुद को खोज लेते हैं, तब दुनिया भी हमें नए नज़रिये से देखने लगती है.
(लेखक पेशे से शिक्षक हैं)
