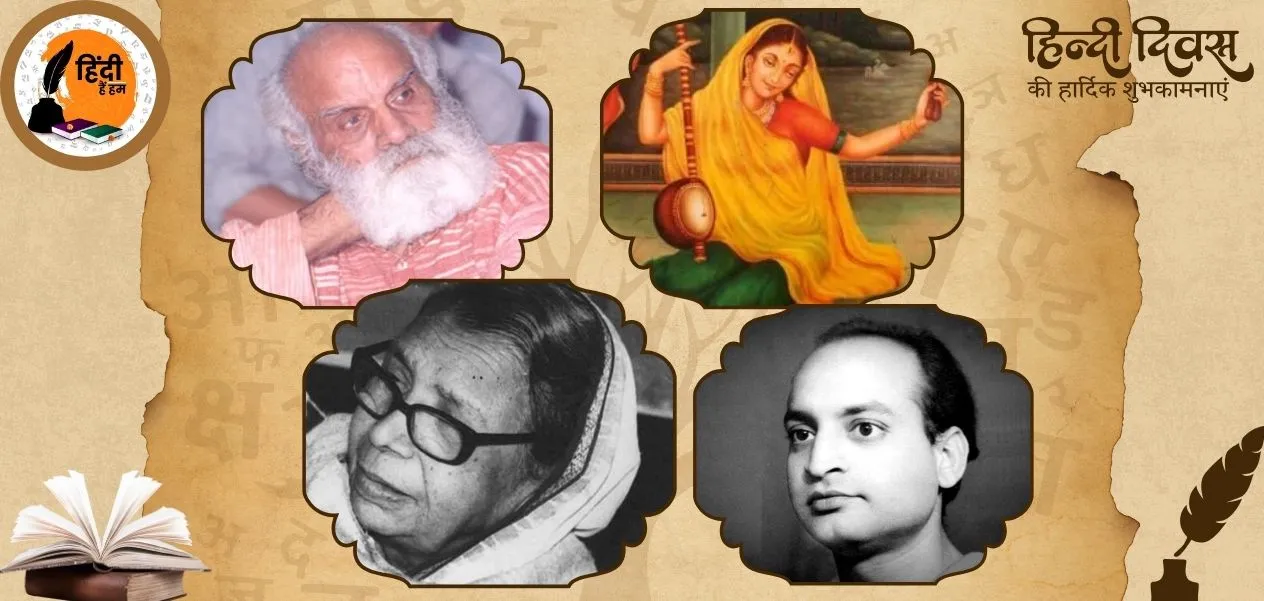
मनीषा सिंह
हम पाठक के तौर पर सोचते हैं कि भारतीय हिंदी साहित्य ने कामायनी से सीधा युगवाणी का सफर किस तरह पूरा किया होगा ? ऐसा क्या हुआ होगा कि छायावाद से प्रगतिवाद का पदार्पण हिंदी साहित्य मीमांसाकों का उत्कृष्ट प्रयास रहा . एक स्त्री होने के नाते यदि मैं स्वयं को 1936के समय में पढ़ते और लिखते हुए कल्पना करती हूं तो मुझे यह अत्यंत साहसी प्रतीत होता है . साथ ही मनुष्य के तौर पर नवाचार.
मैं इस बदलाव को रोचक तो पाती हूं ही अपितु सारगर्भित शब्दों में लिखूं तो छायावाद से प्रगतिवाद का सफर संप्रेषण की दृष्टि से भी एक चिरंजीवी मानवता का उद्घोष था. मैं इस काल में रांगेय राघव हों या त्रिलोचन या शिवमंगल सिंह सुमन सभी का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद साहित्य रसिकों के अवचेतन में एक सकारात्मक आशा का संचार तो करता ही है.

महादेवी वर्मा
परन्तु यदि इसे आधुनिक दृष्टिकोण और भारत में वर्तमान स्त्रीवादी चिंतन की दृष्टि से तौला जाए तो एक प्रश्न मेरे अवचेतन में आता है कि इस मार्क्सवादी चिंतन और क्रांतिकाल में स्त्री रचनाकार कहाँ छूट गईं ?
महादेवी वर्मा का दैन्य स्वर और सुभद्रकुमारी की मर्दानी लक्ष्मीबाई के अलावा क्या स्त्रियां ऐसा कुछ नहीं लिख रही थीं जो दर्ज नहीं हुआ? या कुछ रिक्त स्थान बाकी रह गए? यही सोचते हुए मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया तो पाया कि प्रगतिवाद को पूर्णतः पुरुषप्रधान काल मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी .
ऐसे में ' बहुजन हिताय ' का उद्घोष करने वाला यह काल स्त्री प्रश्न से कैसे चूक गया? जबकि यूरोप में स्त्रीवादी आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव से गुज़र रहा था . कम से कम थोड़ी बहुत बात तो यहाँ भी हो रही होगी?
ऐसे में बहुत अधिक स्त्री लेखिकाओं के नाम हाथ नहीं लगते हैं जो स्त्री मन को उकेर रही हों या यूरोप की भांति बहुआयामी चिंतन को स्वर दे रही हों . ऐसे में तारा बाई शिंदे का नाम लेना मुझे प्रासंगिक लगता है. जबकि उनका लेखन प्रगतिवाद से बहुत अधिक प्राचीन है .
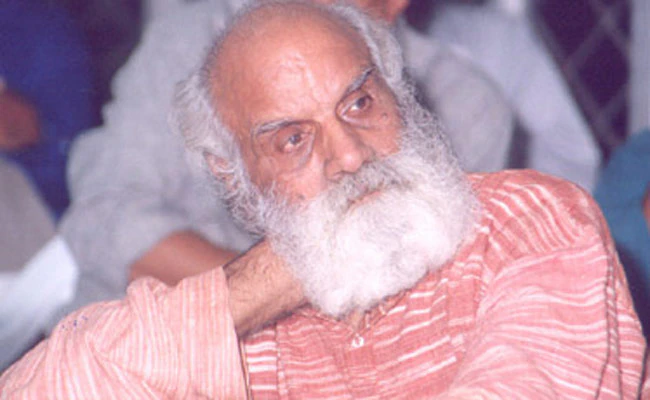
त्रिचन
ताराबाई शिंदे सीधे - सीधे शब्दों में अपनी रचना को ' स्त्री - पुरुष तुलना ' का नाम देती हैं. फुले दंपत्ति भी अठारहवीं शताब्दी से ही स्त्रीवादी चिंतन और नारी चेतना को स्वर देते रहे फिर भी यह कहना मुझे आज भी अजीब लग रहा है कि प्रगतिवादी लेखन में जिन स्त्री लेखिकाओं की दखल का इतिहास है उनमें स्त्री चेतना के स्वर का उपयोग भी दिखाई देकर कहीं न कहीं स्त्री की विवशता का ही वर्णन है.
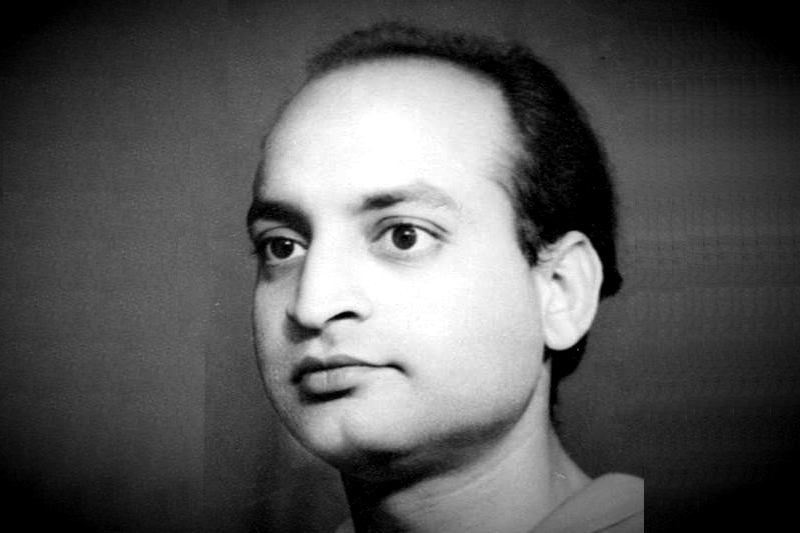 “क्या पूजन ,क्या अर्चन रे!” के स्थान पर “स्त्री का कमरा” जैसे चिंतन का अभाव क्यों प्रतीत होता है? हैरत की बात यह है कि प्रगतिवाद में यदि स्त्रीवादी चिंतन अथवा स्त्रियों के यथार्थ के चित्रण का श्रेय भी पुरुष रचनाकारों खासकर प्रेमचंद को दिया जाना प्रगतिवाद जैसे आशावादी काल में मेरे जैसी एक औसत पाठक को निराशा से भरता है क्योंकि मेरे ख्याल से स्त्री के बारे में स्त्री द्वारा लिखा जाना महत्वपूर्ण है..
“क्या पूजन ,क्या अर्चन रे!” के स्थान पर “स्त्री का कमरा” जैसे चिंतन का अभाव क्यों प्रतीत होता है? हैरत की बात यह है कि प्रगतिवाद में यदि स्त्रीवादी चिंतन अथवा स्त्रियों के यथार्थ के चित्रण का श्रेय भी पुरुष रचनाकारों खासकर प्रेमचंद को दिया जाना प्रगतिवाद जैसे आशावादी काल में मेरे जैसी एक औसत पाठक को निराशा से भरता है क्योंकि मेरे ख्याल से स्त्री के बारे में स्त्री द्वारा लिखा जाना महत्वपूर्ण है..
इसी निराशा को भरने के लिए मैने प्रगतिवाद को एक विद्यार्थी के रूप में आज तक भी जब - जब पढ़ा ,तब - तब मुझे लगा कि कुछ छूट गया है . क्योंकि पंद्रहवीं शताब्दी में मुझे ललद्यद हों या मीरा दोनों का चिंतन हो या अठारहवीं सदी में फुले दंपत्ति सभी का स्वर प्रगतिवादी स्त्री लेखिकाओं से अधिक धारदार और समय से काफी आगे का लगता है.

ऐसे में प्रगतिवादी रचनाओं में स्त्री लेखिकाओं की उपस्थिति इतनी शांत कैसे है ? यहाँ तक कि “दुखिनी बाला” कौन है यह आज भी एक रहस्य है.इतने तेजस्वी लेखन को भी प्रकाशन तक का सुअवसर 2008 में ही मिल सका है. ऐसे में मेरा विद्रोही मन कहता है कि निश्चित ही कई रिक्त स्थान बाकी रह गए हैं जो शायद प्रगतिवाद का और भी सुन्दर समायोजन कर सकते थे .
ये रिक्त स्थान हैं स्त्रीवादी लेखन को अनदेखा करना , जिसका कोई एक कारण नहीं कई कारण होंगे परन्तु उन्हें आज बहाना कहा जाए तब भी उद्दंडता नहीं कही जानी चाहिए . जानकी देवी बजाज की रचनाओं को भी अभी कुछ समय पहले ही प्रकाशन का अवसर मिला ऐसे में मार्क्सवादी स्त्रीवाद भी अधूरा ही रह गया.
यदि पूंजीवाद तरह - तरह से भारतीय परिपेक्ष्य में रोष का विषय रहा तो स्त्रियाँ कैसे पीछे छूट गई होंगी? मेरा मानना है कि आज के समय में भी हम जब हिंदी साहित्य में अंगुलियों पर गिने जा सकने वाली स्त्रियों का नाम लेते हैं ऐसे में यदि ये रिक्त स्थान न छूटते तो चिंतन की धरती की उर्वरता अलग ही आहर्ता रखती. शायद वह समय कुछ और रहा होगा परन्तु यह चूक न होती तो आज के स्त्रीवादी संघर्षों की भारतीय पृष्ठभूमि बहुत मजबूत कही जाती. “ बहुजन हिताय” का दर्शन संपूर्ण होता .
( मनीषा सिंह लेखिका और शिक्षिका हैं)
