
सुशांत झा
छायावाद (1918-1936) हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी युग था. यह युग द्विवेदी युग की नैतिक और उपदेशात्मक कविता के विरोध में उभरा, जिसने कविता को प्रकृति के सौंदर्य, मानवीय भावनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों की ओर मोड़ा. छायावाद का नाम 'छाया' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'छाया' या 'प्रतिबिंब'. यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस युग की कविता में प्रकृति और मानवीय भावनाओं का एक सूक्ष्म और प्रतीकात्मक प्रतिबिंब दिखाई देता है. इस युग के चार प्रमुख स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं.
प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित का कहना है कि छायावाद एक युग प्रवृत्ति भी है, काव्यधारा भी है और स्वयं में एक युग भी है. इसके सौ साल पूरे होने पर कई आयोजन हुए, शताब्दी समारोह हुए और इधर देखने में आया है कि यह अकेली युग प्रवृत्ति के तौर पर उभरी है जिसका शताब्दी समारोह मनाया गया. कई आलोचकों के मुताबिक इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है.
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हालाँकि उन्होंने इसे युग प्रवृत्ति मानने से इनकार करते हुए महज अभिव्यंजना की शैली माना. उन्होंने इसकी शुरुआत का इतिहास लिखते हुए इसे बंगाली काव्य की प्रेरणा से जोड़ा, साथ ही इसके ऊपर उन्होंने अंग्रेजी के स्वच्छतावाद का प्रभाव भी दर्शाया. कालांतर में ये मान्यताएं निरस्त होती गईं.
क्योंकि बंग्ला साहित्य को बहुत निकट से देखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि बंगाल में ऐसी कोई धारा नहीं चली, साथ ही ईसाइयों का रहस्यवाद भी इससे अलग है.कई लोगों ने इसे दार्शनिक दृष्टि से देखा तो कई लोगों ने इसे सामाजिक संचेतना का एक माध्यम माना, लेकिन अनेक विवादों के बावजूद इसका महत्व हिंदी साहित्य में अक्षुण्ण है.
ऐसा माना जाता है कि 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्रीशारदा नामका पत्रिका में मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद नामकी एक लेखमाला प्रकाशित की और उसी से छायावाद शब्द रूढ़ हो गया. हालाँकि कुछ विद्वानों का मत है कि छाया शब्द जयशंकर प्रसाद का एक रूढ़ शब्द है और वे एक अरसे से इसका प्रयोग करते आ रहे थे.
मसलन 1912 में उन्होंने ‘छाया’ नामसे एक कहानी भी लिखी थी. आगे चलकर उन्होंने कविता में छाया की व्याख्या की और साथ ही उन्होंने अपने निबंध संग्रह मे उन्होंने यथार्थवाद और छायावाद नामका एक निबंध भी लिखा जिसमें उन्होंने छाया की परिभाषा दी, उसके स्रोत बताए और उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला.
वैसे भी प्राचीन आचार्यों का कहना था कि कविता में वक्रोक्ति, लक्षणा और व्यंजना या प्रतीक व बिंब होने चाहिए जिसका प्रसाद ने समर्थन किया—क्योंकि सिर्फ कोई बतकही या साफगोई ही कविता नहीं हो सकती. इसका मुख्य कारण ये था कि द्विवेदी युग की कविता जरूरत से ज्यादा वर्णनात्मक हो गई थी, उसमें पौराणिकता और उपदेशात्मकता भर गई थी जिसके प्रत्युत्तर में छायावाद आया था.
छायावाद की कुछ खास विशेषताएँ हैं:
1. प्रकृति-सौंदर्य
छायावादी कवियों ने प्रकृति को केवल बाहरी रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक जीवित और चेतन सत्ता के रूप में अनुभव किया. वे प्रकृति में अपने दुखों, सुखों, और भावनाओं का प्रतिबिंब देखते थे. प्रकृति उनके लिए केवल एक पृष्ठभूमि नहीं थी, बल्कि एक सहचरी थी, जिससे वे संवाद स्थापित करते थे.
सुमित्रानंदन पंत को 'प्रकृति का सुकुमार कवि' कहा जाता है. उनकी कविताओं में प्रकृति का अत्यंत सूक्ष्म और कोमल चित्रण मिलता है. 'पल्लव' और 'गुंजन' जैसी रचनाओं में उन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों, जैसे सुबह की किरणें, शाम की लालिमा, और फूलों की कोमलता का वर्णन किया है.
जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है. वे प्रकृति को एक संवेदनशील पात्र के रूप में चित्रित करते हैं.महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रकृति एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के रूप में प्रकट होती है, जहाँ वे अपने रहस्यमय प्रियतम से मिलती हैं.
2. रहस्यवाद
छायावाद की एक और प्रमुख विशेषता रहस्यवाद है. रहस्यवाद का अर्थ है अज्ञात और अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम और जिज्ञासा. छायावादी कवि अपनी कविताओं में एक ऐसे प्रियतम की खोज करते हैं, जो इस भौतिक दुनिया से परे है. यह रहस्यवाद लौकिक प्रेम से शुरू होकर अलौकिक प्रेम तक पहुँचता है.
महादेवी वर्मा को 'आधुनिक मीरा' कहा जाता है. उनकी कविताओं में रहस्यवाद की गहरी अनुभूति मिलती है. वे अपने गीतों में एक ऐसे प्रियतम की प्रतीक्षा करती हैं, जो कभी नहीं आता, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है. 'नीर भरी दुख की बदली' और 'मैं नीर भरी दुख की बदली' जैसी रचनाओं में यह रहस्यवाद स्पष्ट दिखाई देता है.
जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' में भी रहस्यवाद की झलक मिलती है, जहाँ वे मनु और श्रद्धा के माध्यम से सृष्टि के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं.
3. व्यक्तिवाद
द्विवेदी युग की कविता जहाँ समाज और नैतिकता पर केंद्रित थी, वहीं छायावादी कविता व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों पर केंद्रित थी. कवियों ने अपने व्यक्तिगत सुख-दुख, आशा-निराशा, और प्रेम-विरह को कविता का विषय बनाया. यह व्यक्तिवाद कविता को एक नया आयाम देता है, जहाँ कवि अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है.
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कविताओं में व्यक्तिवाद का एक सशक्त रूप दिखाई देता है. उनकी कविता 'राम की शक्तिपूजा' में राम का चरित्र व्यक्तिगत संघर्षों और पीड़ाओं से भरा है. 'सरोज स्मृति' में वे अपनी पुत्री की मृत्यु पर अपनी व्यक्तिगत वेदना को व्यक्त करते हैं.
4. प्रेम-भावना
छायावादी कविता में प्रेम-भावना का एक नया रूप देखने को मिलता है. यह प्रेम स्थूल और भौतिक नहीं, बल्कि सूक्ष्म, आध्यात्मिक और उदात्त है. यह प्रेम अक्सर विरह और निराशा से भरा होता है, जो इसे और भी गहरा और मार्मिक बनाता है.
जयशंकर प्रसाद की 'आँसू' विरह काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें कवि अपने प्रिय के वियोग में अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं.महादेवी वर्मा के गीतों में प्रेम एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ वे अपने प्रियतम से मिलने की आतुरता में हैं.
सुमित्रानंदन पंत की कविता में प्रेम प्रकृति के सौंदर्य से जुड़ा है, जहाँ प्रकृति प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है.
छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ

1. जयशंकर प्रसाद (1889-1937)
प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है. उनकी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और रहस्यवाद का अद्भुत संगम मिलता है. उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं-- 'कामायनी', 'आँसू', 'लहर' 'झरना' इत्यादि.
कामायनी प्रसाद का महाकाव्य है, जो मनु और श्रद्धा की कहानी के माध्यम से मानवता के विकास को दर्शाता है. इसमें दर्शन, मनोविज्ञान, और प्रकृति का सुंदर समन्वय है.
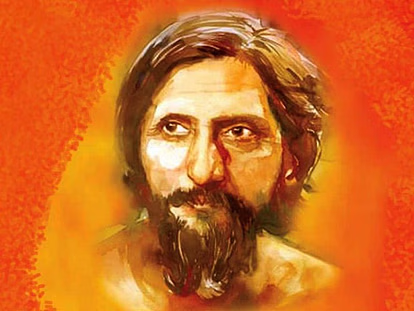
2. सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (1896-1961)
निराला को छायावाद का विद्रोही कवि कहा जाता है. उन्होंने छंदों के बंधन को तोड़ा और मुक्त छंद में कविताएँ लिखीं. उनकी कविता में ओज, विद्रोह और गहनता का समावेश है. उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं-'परिमल', 'गीतिका', 'अनामिका', 'सरोज स्मृति', 'राम की शक्तिपूजा' आदि.
राम की शक्तिपूजा उनकी सबसे प्रसिद्ध लंबी कविता है, जिसमें राम के मानवीय संघर्ष और शक्ति प्राप्त करने की कहानी का वर्णन है.

3. सुमित्रानंदन पंत (1900-1977)
पंत को 'प्रकृति का सुकुमार कवि' कहा जाता है. उनकी कविताओं में प्रकृति का अत्यंत कोमल और मानवीय चित्रण मिलता है. उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं-- 'वीणा', 'पल्लव', 'गुंजन', 'युगांत' आदि.
पल्लव संग्रह में प्रकृति के विभिन्न रूपों का सूक्ष्म और कोमल चित्रण है, जो इसे छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक बनाता है.

4. महादेवी वर्मा (1907-1987)
महादेवी वर्मा को 'आधुनिक मीरा' और 'वेदना की कवयित्री' कहा जाता है. उनके गीतों में रहस्यवाद, प्रेम और विरह की गहरी अनुभूति मिलती है. उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं-- 'नीहार', 'रश्मि', 'नीरजा', 'सांध्यगीत', 'यामा' आदि.यामा उनकी कविताओं का संग्रह है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला.
सुमित्रानंदन पंत ने इसके लिए ‘छाया दर्शन’, महादेवी वर्मा ने इसके लिए ‘छायावृत्ति’ और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसके लिए वेदों की नीलिमा यानी आकाश की गहनता तक का इस्तेमाल किया. यानी जिस तरह से कला में एक गोपन वृत्ति होती है, उसी तरह से काव्य में भी एक छाया-वृत्ति हो और उसे हूबहू वैसे ही न कह दिया जाए जैसे कि वह उपस्थित है.
छायावाद हिंदी साहित्य का एक ऐसा युग था, जिसने कविता को एक नई दिशा दी. इसने कविता को व्यक्तिपरक, भावुक और सौंदर्यपरक बनाया. इसने प्रकृति, प्रेम और रहस्यवाद को कविता का मुख्य विषय बनाया. छायावाद के चार स्तंभ कवियों ने हिंदी कविता को एक नया आयाम दिया और उसे विश्व साहित्य के समकक्ष खड़ा किया. यद्यपि छायावाद का समय काल 1918से 1936तक माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी हिंदी साहित्य में दिखाई देता है.
(लेखक पत्रकार, टिप्पणीकार और अनुवादक रहे हैं. फिलहाल मंजुल पब्लिशिंह हाउस में प्रबंध संपादक हैं.)
