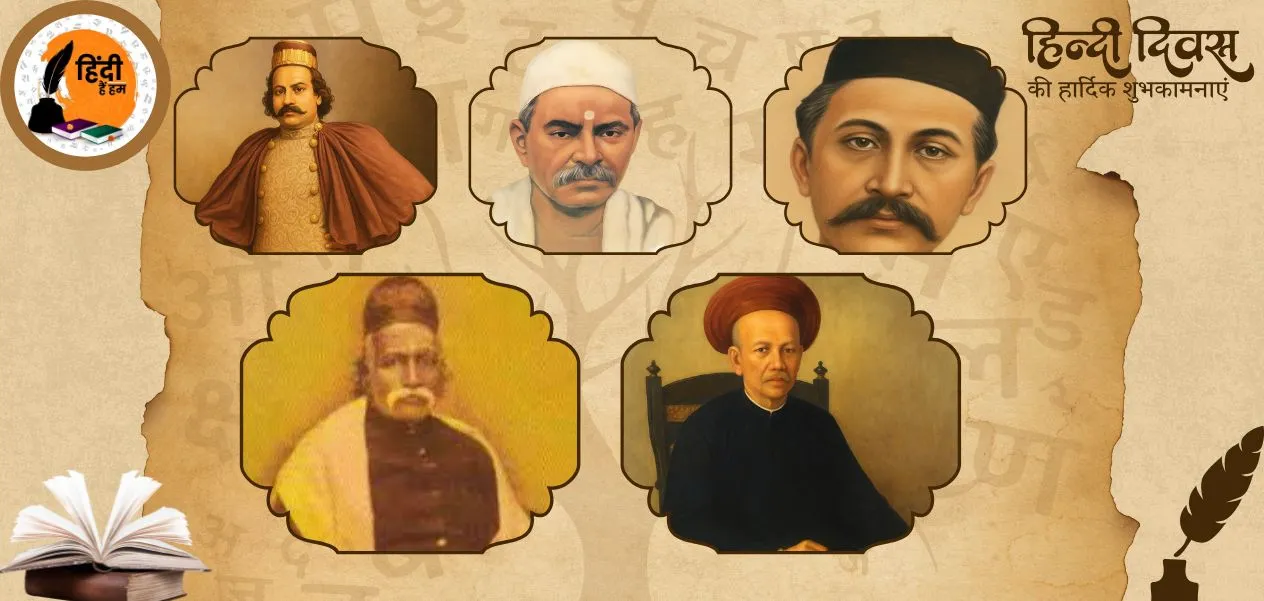
डॉ. फ़िरदौस ख़ान
हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु युग को सामान्यतः सन् 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है.इस युग के अग्रदूत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को आधुनिक हिन्दी साहित्य का जनक कहा जाता है, और उन्हीं के सम्मान में इस युग को ‘भारतेन्दु युग’ की संज्ञा दी गई.यह कालखण्ड आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक चरण है, जिसे हिन्दी का पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है.इस युग में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और जन-जागरण की भावना ने साहित्य को एक नई दिशा दी.साहित्य के माध्यम से समाज को जागरूक करने और नवीन विचारधारा को प्रसारित करने का कार्य इसी युग में प्रभावी रूप से आरम्भ हुआ.
निःसंदेह, यह कालखंड भारतीय समाज के पुनर्जागरण का युग था, जिसमें व्याप्त जातिवाद, ऊँच-नीच का भेदभाव, लैंगिक विषमता, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा और अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सशक्त आवाज़ उठाई गई.इन विघातक प्रवृत्तियों के उन्मूलन हेतु निरंतर संघर्ष किया गया और सामाजिक समरसता, समानता व राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया.
इस समय भारत ब्रिटिश शासन की कठोर और दमनकारी नीतियों के अधीन था.अंग्रेजों के अत्याचारों से जनता का जीवन दयनीय हो गया था.ऐसे संकटपूर्ण वातावरण में साहित्यकारों ने अपनी लेखनी को जनजागरण का माध्यम बनाया और स्वतंत्रता की चिंगारी को जनमानस में प्रज्वलित किया.इस युग का साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, अपितु वह सामाजिक सुधार, देशभक्ति और राष्ट्र चेतना का प्रभावशाली स्वर बन गया.
इस काल में असंख्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिनका उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना, स्वतंत्रता के प्रति उत्साह जगाना और ब्रिटिश शासन की जनविरोधी नीतियों का निर्भीक विरोध करना था.साहित्य के साथ-साथ पत्रकारिता ने भी इस जागरण अभियान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
यही नहीं, इस युग में नाट्यकला को भी नया जीवन मिला.अनेक मौलिक तथा अनूदित नाटकों की रचना के माध्यम से राष्ट्रीय रंगमंच का विकास हुआ.इस मंच ने भी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनजागरण का कार्य किया और जनता को सुधार की दिशा में प्रेरित किया.वस्तुतः यह युग साहित्य, पत्रकारिता और नाट्यकला के संगम से भारतीय समाज के नवजागरण का साक्षी बना.
इस युग में हिन्दी की उन्नति पर भी विशेष बल दिया गया.जनसम्पर्क की भाषा के रूप में इसका प्रचार-प्रसार किया गया.इस युग में साहित्य लेखन की विभिन्न विधाओं के साथ-साथ हास्य-व्यंग्य को भी प्रोत्साहन मिला.इसके द्वारा तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य किए गये, तीखे कटाक्ष किए गये.
भारतेन्दु युग के साहित्यकार नायिका के बाहरी सौन्दर्य पर काव्य नहीं रचते थे, बल्कि उसके मन की व्यथा और उसकी वेदना को अनुभव करते हुए इस पर चिन्ता व्यक्त करते थे। उन्होंने जनमानस के लिए साहित्य रचा.
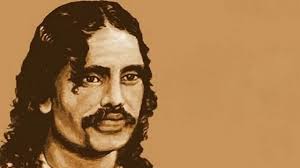
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.उनका मूल नाम ‘हरिश्चन्द्र’ था और ‘भारतेन्दु' उनकी उपाधि थी.उन्होंने रीतिकाल की सामन्ती संस्कृति को त्याग कर एक नई परम्परा प्रारम्भ की.
उल्लेखनीय है कि रीतिकाल में अधिकांश काव्य राजाओं के दरबारों में आश्रय पाकर लिखा गया.इसलिए काव्य की रचना आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार ही होती थी.काव्य का उद्देश्य राजाओं का मनोरंजन करना होता था.इसके लिए मुक्तक काव्य सर्वोत्तम माना जाता था.
साहित्य में नवीनता के कारण भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध हुए.उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध स्वर मुखर किया.उनके साहित्य में तत्कालीन परिवेश का सजीव चित्रण मिलता है.
वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे.वे एक कवि, गद्यकार, नाटककार, निबंधकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, सम्पादक और कुशल वक्ता भी थे.उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया.उन्होंने 'कविवचनसुधा, हरिश्चन्द्र मैगजीन और बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं भी निकालीं.
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को काव्य-प्रतिभा अपने पिता से विरासत में में मिली थी.उनके पिता गोपालचन्द्र कवि थे और 'गिरधरदास' उपनाम से काव्य रचते थे.कहा जाता है कि केवल पांच वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने एक दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया था-
लै ब्योढ़ा ठाढ़े भए श्री अनिरुद्ध सुजान।
बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान।।
अपने नन्हे बालक के मुंह से दोहा सुनकर उनके पिता भाव-विभोर हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को सुकवि होने का आशीर्वाद दिया.पिता के आशीष का ही फल था कि उन्होंने बहुत ही कम आयु में साहित्य जगत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया.
उनकी मुख्य रचनाओं में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चन्द्र, श्री चंद्रावली, विषस्य विषमौषधम्, भारत दुर्दशा, नीलदेवी और अंधेर नगरी आदि सम्मिलित हैं.भारतेन्दु हरिश्चंन्द्र खड़ीबोली गद्य के प्रर्तक हैं.उनके युग में कविता की भाषा मुख्यतः ब्रज थी.उन्होंने हिन्दी के साथ-साथ मातृभाषा पर विशेष बल दिया-
निज भाषा उन्नाति अहै सब उन्नयति को मूल
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल
भारतेन्दु युग के विषय में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है- “भारतेन्दु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था, उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मन्दाकिनी में स्ना न कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोकजीवन के आमने-सामने खड़ा कर दिया.”
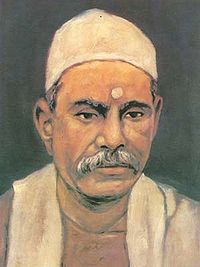
बालकृष्ण भट्ट
बालकृष्ण भट्ट भारतेन्दु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक हैं.उन्हें गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है.वे उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और पत्रकार थे.वे पहले ऐसे निबंधकार थे, जिन्होंने आत्मपरक शैली का प्रयोग कर हिन्दी को एक नई शैली प्रदान की.
उनकी प्रमुख रचनाओं में साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली (निबंध संग्रह), नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान (उपन्यास), दमयंती स्वयंवर, बाल-विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल (नाटक) और वेणीसंहार, मृच्छकटिक, पद्मावती (अनुवाद) सम्मिलित हैं.
उन्होंने लगभग बत्तीस साल तक मासिक पत्रिका 'हिन्दी प्रदीप' का सम्पादन किया.उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से जनमानस में देशप्रेम की भावना जागृत की और हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
उन्होंने जहां 'भारतेन्दु युग' को आधार प्रदान किया, वहीं वे 'द्विवेदी युग' के लेखकों के प्रेरणा स्त्रोत भी रहे.उनकी भाषा शैली उत्कृष्ट थी.उन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध हिन्दी का प्रयोग किया.वे शब्दों का चयन करने में अत्यंत कुशल थे.उन्होंने अपनी रचनाओं में यथासंभव लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी किया.
उन्होंने संस्कृत के शब्दों के साथ-साथ अरबी, फ़ारसी, उर्दू और स्थानीय भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया.विभिन्न भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली बन गई है.उन्होंने वर्णनात्मक शैली में निबंध लिखे और उपन्यास में भी इसी शैली का प्रयोग किया.
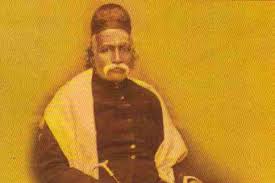
बदरीनारायण चौधरी उपाध्याय "प्रेमघन"
बदरीनारायण चौधरी उपाध्याय ‘प्रेमघन’ भी भारतेन्दु युग के आधार स्तम्भ माने जाते हैं.वे कवि, गद्य लेखक और नाटककार थे.वे खड़ी बोली गद्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं.उन्होंने कविता, निबंध, नाटक, आलोचना और प्रहसन लिखकर साहित्य जगत में अपनी एक पहचान स्थापित की.
उनकी गद्य रचनाओं में हास-परिहास का पुट मिलता है.उन्होंने अपनी रचनाओं में हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत, फ़ारसी, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का भरपूर प्रयोग किया.हिन्दी आलोचना और अन्य गद्य विधाओं के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है.उन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना की.उन्होंने लोकगीत कजली, होली और चैता आदि लिखे, जो ख़ूब लोकप्रिय हुए.
उन्होंने पत्रिका ‘आनन्द कादम्बनी’ का भी सम्पादन किया.उन्होंने बाद में समाचार-पत्र ‘नागरी नीरद’ का भी प्रकाशन किया.उन्होंने इन पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के विरुद्ध स्वर मुखर किया, विशेषकर किसानों की व्यथा के बारे में लिखा। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी लिखा.
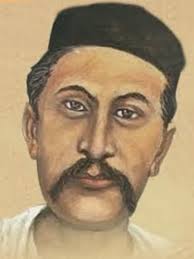
प्रतापनारायण मिश्र
प्रतापनारायण मिश्र भी भारतेन्दु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं.वे कवि, उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार, निबंधकार और पत्रकार थे.उन्हें हिन्दी खड़ी बोली का उन्नायक कहा जाता है.उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली के रूप में प्रचलित जनभाषा का प्रयोग किया.
उनकी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र में अपार श्रद्धा थी.वह स्वयं को उनका शिष्य कहते थे.उनकी भाषा शैली और अन्य विशेषताओं के कारण उन्हें 'प्रतिभारतेन्दु' अथवा 'द्वितीयचन्द्र' कहा जाता है.
उन्होंने मासिक पत्रिका ‘ब्राह्मण’ का सम्पादन किया.इसमें उन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम व अन्य सम-सामयिक विषयों पर लेख लिखे.उनकी प्रमुख रचनाओं में कानपुर माहात्म्य, तृप्यन्ताम्, तारापति पचीसी, प्रार्थना शतक, प्रेम पुष्पावली, फाल्गुन माहात्म्य, मन की लहर, युवराज कुमार स्वागतन्ते, लोकोक्ति शतक, शोकाश्रु, श्रृंगार विलास, श्री प्रेम पुराण और होली है (काव्य) और कलि कौतुक, भारत दुर्दशा (रूपक), हठी हमीर, संगीत शाकुन्तल, कलि प्रवेश (गीति रूपक) आदि सम्मिलित हैं.
राधाकृष्ण दास
राधाकृष्ण दास भी भारतेन्दु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक हैं.वे कवि, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और पत्रकार थे.वे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के फुफेरे भाई थे.उनकी मुख्य रचनाओं में धर्मालाप, दुःखिनी बाला, पद्मावती, नागरीदास का जीवन चरित, हिन्दी भाषा के पत्रों का सामयिक इतिहास, राजस्थान केसरी, महाराणा प्रताप सिंह नाटक, भारतेन्दु जी की जीवनी, रहिमन विलास आदि सम्मिलित हैं.वे प्रसिद्ध पत्रिका ‘सरस्वती’ के सम्पादक मंडल में रहे.वे नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे.उन्होंने जीवन पर्यन्त हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया.उन्होंने समाज सुधार और देशप्रेम पर विशेष बल दिया.

लाला श्रीनिवासदास
भारतेन्दु युग के साहित्यकारों में लाला श्रीनिवासदास को भी एक विशेष स्थान प्राप्त है.वे नाटककार और उपन्यासकार थे.उन्होंने हिन्दी का पहला उपन्यास लिखा था.इसलिए उन्हें हिन्दी का प्रथम उपान्यासकार माना जाता है.
नाट्य-लेखन में वे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समकक्ष माने जाते हैं.उनकी प्रमुख नाटकों में प्रह्लाद चरित्र, तप्ता-संवरण, रणधीर और प्रेममोहनी, संयोगता-स्वयंवर सम्मिलित हैं.उन्होंने ‘परीक्षागुरु’ नामक एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा.
अम्बिका दत्त व्यास
अम्बिका दत्त व्यास भी भारतेन्दु युग के प्रमुख कवि और नाटककार थे.काशी कविता वर्धिनी सभा ने उन्हें 'सुकवि' की उपाधि से सम्मानित किया था.उन्होंने पत्रिका ‘वैष्णव’ निकाली, जिसे बाद में 'पियूष-प्रवाह' नाम से साहित्यिक पत्रिका में रूपांतरित कर दिया गया.
उन्होंने ‘फ़ंतासी’ और ‘शिवराज विजय’ नामक उपन्यास लिखे.उन्होंने खड़ी बोली में तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार की कविताएं लिखीं.‘पावन पचासा’ उनकी एक प्रमुख काव्यकृति है.उन्होंने अवतार मीमांसा नामक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ की भी रचना की.यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतेन्दु युग के साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से जनमानस के लिए संघर्ष किया और उनमें राष्ट्रीय चेतना का संचार किया.
(लेखिका शायरा, कहानीकार और पत्रकार हैं)
