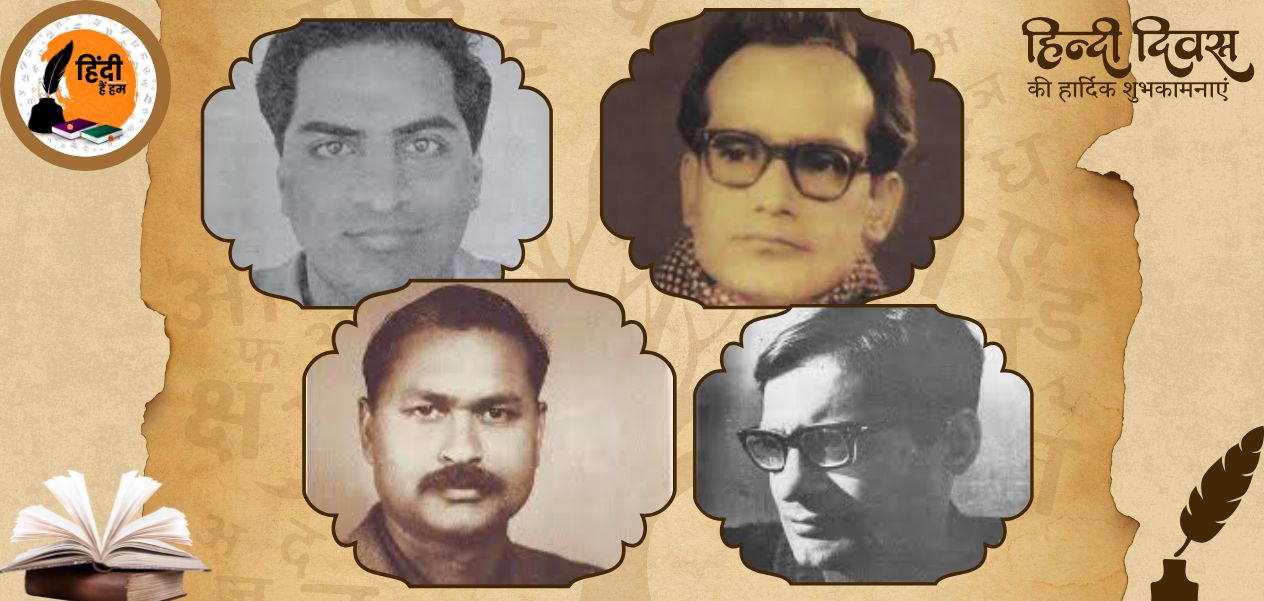
 डॉ. फ़िरदौस ख़ान
डॉ. फ़िरदौस ख़ान
हिन्दी साहित्य जगत में 1960से 1970तक चले काव्य आन्दोलन को ‘अकविता आन्दोलन’ कहा जाता है. हिन्दी साहित्य में डॉ. जगदीश चतुर्वेदी को इसका प्रवर्तक माना जाता है. इस आन्दोलन की विशेषता यह थी कि इसने कविता के पारम्परिक सिंद्धांतों का विरोध किया और कविता के लिए एक नई परिभाषा गढ़ी. यह भी कह सकते हैं कि इसने कविता को हर पारम्परिक बंधन से मुक्त कर दिया.
वास्तव में यह आन्दोलन पश्चिम के ‘एंटी पोएट्री’ (अकविता) आन्दोलन से प्रभावित था. यह कहना क़तई ग़लत नहीं होगा कि यह ‘एंटी पोएट्री’ का ही हिन्दी संस्करण था. चिली के सुप्रसिद्ध कवि निकानोर पार्रा ने इस आन्दोलन का प्रारम्भ किया था, इसलिए उन्हें इसका जनक माना जाता है. वे बीसवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध लैटिन अमेरिकी कवियों में से एक थे. उन्होंने कविता के पारम्परिक सिद्धांतों छन्द, लय और परिष्कृत भाषा आदि का विरोध कर जनमानस की बोलचाल की भाषा में कविताएं लिखीं. उन्होंने 1954में इन कविताओं का प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित किया. इसके बाद ऐसी कविताओं के संग्रह प्रकाशित होने लगे. काव्य क्षेत्र में यह एक ऐसा आन्दोलन था, जिसे जनमानस का भरपूर समर्थन मिला.
साधारण लोगों को इस आन्दोलन से बहुत लाभ हुआ. जो लोग कविता के माध्यम से अपने मनोभावों और अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन वे काव्य के सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे, अब वे भी कविता कहने लगे थे. कविता की पहुंच जनमानस तक हो गई थी. कविता की भाषा इतनी सरल, सहज और सपाट थी कि हर कोई कविता का अर्थ और मर्म समझ जाता था. इस तरह निकानोर पार्रा जनमानस के कवि बनकर लोकप्रिय हुए.
ऐसा नहीं है कि अकविता आन्दोलन केवल कविता के स्थापित पारम्परिक सिद्धांतों का विरोध करता था, बल्कि यह व्यवस्था के प्रति हताशा, निराशा, आक्रमकता और विद्रोह को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करता था. यह काव्य के अन्य आन्दोलनों की तरह नई कविता से भी बिल्कुल अलग था.
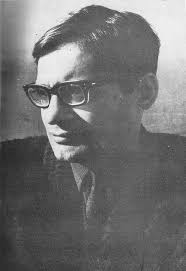 डॉ. जगदीश चतुर्वेदी
डॉ. जगदीश चतुर्वेदी
अकविता के जनक डॉ. जगदीश चतुर्वेदी प्रमुख कवि, कथाकार, नाटककार और सम्पादक थे. तत्कालीन व्यवस्था के प्रति उनके मन में क्षोभ और आक्रोश था. उन्होंने असमानता और भ्रष्टाचार के प्रति लेखन के माध्यम से स्वर मुखर किया. उनकी कविता एक साधारण व्यक्ति की कविता थी. उनकी कविताओं में जनमानस की मनोव्यथा की अभिव्यक्ति थी.
उनकी प्रमुख कृतियों में सूर्यपुत्र, पूर्वराग, इतिहासहंता, नये मसीहा का जन्म, कहानी संग्रह अंधेरे का आदमी, अंतराल के दो छोर (कविता संग्रह) और कपास के फूल, पीली दोपहर (नाटक) आदि शामिल हैं. उन्होंने पत्रिका ’भाषा’ और ’वार्षिकी’ का सम्पादन भी किया. उन्हें उत्कृष्ट लेखन के लिए सूर पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का पुरस्कार और प्रियदर्शिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
उनकी कविताओं की भाषा सरल, सहज और मनभावन है. उनकी एक कविता देखें-
मैंने गुलाब को छुआ
और उसकी पंखुड़ियाँ खिल उठीं
मैंने गुलाब को अधरों से लगाया
और उसकी कोंपलों में ऊष्मा उतर आई.
गुलाब की आँखों में वसन्त था
और मेरी आँखों में उन्माद
मैंने उसे अपने पास आने का आह्वान दिया
और उसने
अपने कोमल स्पर्श से मेरी धमनियों में
स्नेह की वर्षा उड़ेल दी.
अब गुलाब मेरे रोम-रोम में है
मेरे होठों में है
मेरी बांहों में है
और उसकी रक्तिम आभा
आकाश में फैल गई है
और
बिखेर गई है मादक सुगन्ध
अवयवों में
और उगते सूरज की मुस्कुराहट में.
 श्याम परमार
श्याम परमार
श्याम परमार ‘अकविता' आंदोलन के सुप्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, आलोचक और सम्पादक थे. उनकी कविताओं में लोक बोलता है अर्थात उनकी कविताएं स्वयं में लोक-जीवन के संघर्ष, उसकी जटिलताओं और अनुभवों को समेटे हुए हैं. उनकी एक कविता देखें-
(कमबख़्त इस मौसम को क्या कहूँ)
एक चमकती झील
पूरे शहर पर आ गिरी
(मज़ा यह कि) इमारतों की छतें
सुर्ख़ हो गईं
सड़कों के बीचों-बीच
टिन की नई चादरें
बिछा दीं इसने
(और देखता क्या हूँ)
काले चश्मों ने तमाम चेहरों को
ढँक लिया है.
उनकी प्रमुख कृतियों में अकविता और कला-संदर्भ (आलोचना), मोर झाल (उपन्यास) और भारतीय लोक-साहित्य, लोक-धर्मी नाट्य-परम्परा, हिन्दी-साहित्य का बृहत इतिहास व लोक-साहित्य की अनेक पुस्तकें शामिल हैं. उन्होंने हिन्दी-साहित्य कोश में भी सहयोगी की भूमिका निभाई. उन्होंने 1965में पत्रिका 'अकविता' का सम्पादन भी किया.
 राजकमल चौधरी
राजकमल चौधरी
राजकमल चौधरी हिन्दी और मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे. हिन्दी के साथ-साथ उन्होंने मैथिली भाषा में भी बहुत लिखा. वास्तव में उन्होंने लेखन का प्रारम्भ अपनी मातृभाषा मैथिली से किया था, परन्तु बाद में वे हिन्दी में भी लिखने लगे. हिन्दी साहित्य जगत में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई.
उनकी प्रमुख कृतियों में कंकावती, इस अकालबेला में, विचित्रा (कविता संग्रह), सामुद्रिक और अन्य कहानियां, मछलीजाल, प्रतिनिधि कहानियां (कहानी संग्रह) और मछली मरी हुई, देहगाथा, नदी बहती थी,शहर था शहर नहीं था, अग्निस्नान, बीस रानियों के बाइस्कोप, एक अनार एक बीमार, ताश के पत्तों का शहर (उपन्यास शामिल हैं.
उनकी कविताएं अकविता शैली की हैं. उन्होंने कविता के पारम्परिक सिद्धांतों को त्याग कर अपनी इच्छानुसार काव्य की रचना की. उन्होंने स्वयं को न तो किसी लय से बांधा और न काव्य के किसी अन्य नियम का पालन किया. उनकी कविताएं तो हवा के उस झोंके की तरह थीं, जो तन को छूकर चला जाता है. उनकी कविताओं में उनकी अंतरात्मा का स्वर था, उनके मनोभाव थे, उनकी निजी अनुभूति थी. उनकी कविता की यही विशेषताएं उन्हें उनके समकालीन कवियों से अलग करती हैं, उन्हें विशिष्टता प्रदान करती हैं. प्रारम्भ में उन्होंने लयबद्ध कविताएं लिखी थीं, लेकिन बाद में वे अकविता शैली की कविताएं लिखने लगे. उनकी कविता का एक अंश देखें-
पहली कविता की आख़िरी शाम
नीले दरख़्तों के साए में तुम्हारे
बेचैन हाथ
पीले पड़ते हुए.
क्राटन के लम्बे पत्तों की तरह हिलते हैं
यों दरख़्त भव्य काले हैं
घनी और जड़ चाँदी की हल्की पर्त
चाँदनी में गूँज और गंध-वसंत की वापिसी की
लगातार आहटें
और, नीले सायों का बेतरतीब
जाल
ओस भीगी धरती पर (रौंदी हुई फिर भी हरी घास)
बुनती हैं झुकी डालें
—बेचैन हाथों की ज़र्द उँगलियाँ
अचानक चुप हो जाती हैं
अनदिखे सितार का एक भी तार नहीं सिहरता
शतरंज के खेल में खोई हुई किश्ती
ढूँढ़ता हुआ हर शाम यहाँ इस चंपक-वन
तक मैं बेकार चला आता था जबकि आज
की शाम (या ऐसी हर शाम)
अनकहे-अधबने शब्दों की शाम है...
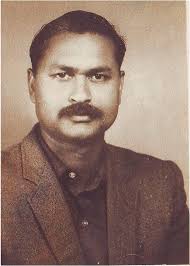 सुदामा पांडेय 'धूमिल'
सुदामा पांडेय 'धूमिल'
सुदामा पाण्डेय ‘धूमिल’ अकविता आन्दोलन के प्रमुख कवि, कहानीकार और निबंधकार थे. उन्होंने पारम्परिक कवि की तरह स्वप्न लोक में विचरते हुए काव्य नहीं रचा, बल्कि यथार्थ के धरातल पर रहते हुए कविताएं लिखीं. उनकी कविताओं में एक साधारण व्यक्ति की मनोव्यथा, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना और उसका आक्रोश झलकता है. उनके काव्य की भाषा अत्यंत सरल और सहज है. उनकी एक कविता देखें-
एक आदमी
रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है
वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूँ—
‘यह तीसरा आदमी कौन है?’
मेरे देश की संसद मौन है.
उनका काव्य संग्रह ‘संसद से सड़क तक’ बहुत चर्चित हुआ था. यह उनका एकमात्र काव्य संग्रह था, जो उनके जीवनकाल में प्रकाशित हुआ. केवल 39वर्ष की अल्प आयु में उनका निधन हो गया था. उनकी मृत्यु के बाद उनके दो काव्य संग्रह ‘कल सुनना मुझे’ और ‘सुदामा पांडे का प्रजातंत्र’ प्रकाशित हुए. मरणोपरांत ‘कल सुनना मुझे’ काव्य संग्रह के लिए उन्हें वर्ष 1979के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उनकी कहानियां और असंख्य निबंध विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं.
(लेखिका शायरा, कहानीकार व पत्रकार हैं)
