
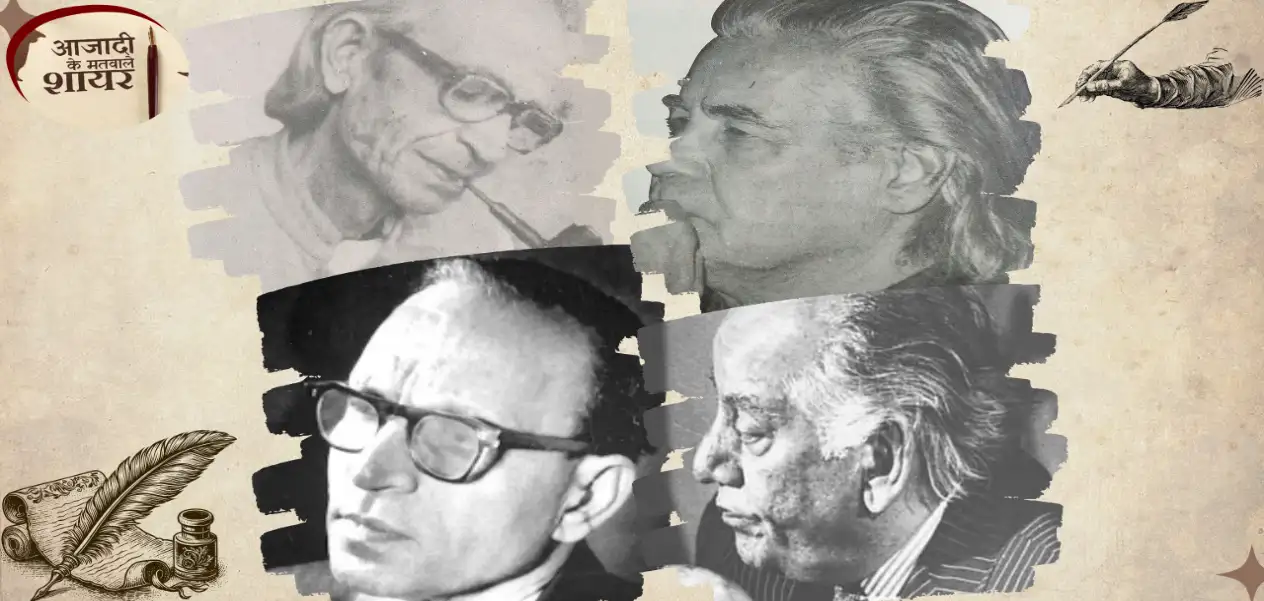
ज़ाहिद ख़ान
तरक़्क़ी—पसंद तहरीक से निकले तमाम तरक़्क़ी—पसंद शायरों का ख़्वाब हिंदुस्तान की आज़ादी थी. साल 1942 से 1947 तक का दौर, तरक़्क़ी—पसंद तहरीक का सुनहरा दौर था. यह तहरीक आहिस्ता-आहिस्ता मुल्क की सारी ज़बानों में फैलती चली गई. हर भाषा में एक नये सांस्कृतिक आंदोलन ने जन्म लिया. इन आंदोलनों का आख़िरी मक़सद मुल्क की आज़ादी थी. आन्दोलन ने जहॉं धार्मिक अंधविश्वास, जातिवाद व हर तरह की धर्मांधता और सामंतशाही का विरोध किया, तो वहीं साम्राज्यवादी दुश्मनों से भी जमकर टक्कर ली. फै़ज़ अहमद फ़ैज़, मख़दूम मोहिउद्दीन, अली सरदार जाफ़री और वामिक़ जौनपुरी जैसे मशहूर—ओ—मारूफ़ शायर तरक़्क़ी—पसंद तहरीक के हमनवॉं, हमसफ़र थे.
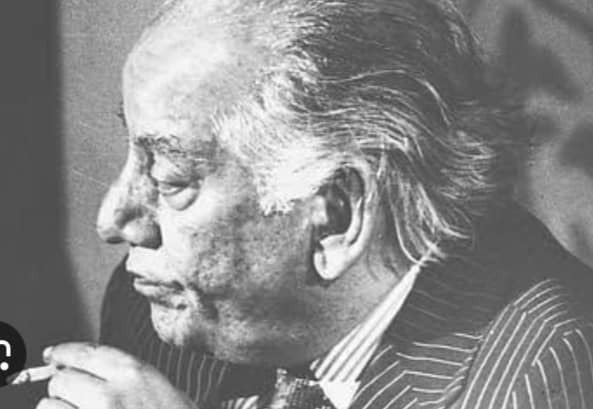 फै़ज़ अहमद फै़ज़
फै़ज़ अहमद फै़ज़
फै़ज़ अहमद फै़ज़ ने अपने कलाम से बार-बार मुल्कवासियों को एक फ़ैसलाकुन जंग के लिए ललकारा. ‘शीशों का मसीहा कोई नहीं’ शीर्षक नज़्म में वे कहते हैं,‘‘सब सागर शीशे लालो-गुहर, इस बाजी में बद जाते हैं/उठो, सब खाली हाथों को इस रन से बुलावे आते हैं.’’ फ़ैज़ की ऐसी ही एक दीगर ग़ज़ल का शे’र है,‘‘लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं/इक जरा सब्र कि फ़रियाद के दिन थोड़े हैं.’’
लाखों लोगों की क़ुर्बानियों के बाद आख़िरकार, वह दिन भी आया जब मुल्क आज़ाद हुआ. पर यह आज़ादी हमें बंटवारे के तौर पर मिली. मुल्क दो हिस्सों में बंट गया. भारत और पाकिस्तान ! बंटवारे से पहले हुई साम्प्रदायिक हिंसा ने पूरे मुल्क को झुलसा के रख दिया. रक्तरंजित और जलते हुए शहरों को देखकर फै़ज़ ने ‘सुबह-ए-आज़ादी’ टाइटल से एक नज़्म लिखी. इस नज़्म में बंटवारे का दर्द जिस तरह से नुमायां हुआ है, वैसा उर्दू अदब में दूसरी जगह मिलना बामुश्किल है, "ये दाग-दाग उजाला, ये शबग़जीदा सहर/वो इंतिज़ार था जिसका,ये वो सहर तो नहीं.
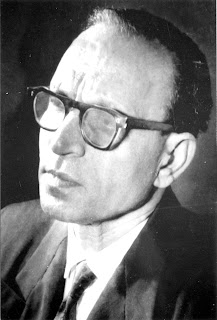 मख़दूम मोहिउद्दीन
मख़दूम मोहिउद्दीन
मेहनत—कशों के चहेते, इंक़लाबी शायर मख़दूम मोहिउद्दीन का शुमार मुल्क में उन शख़्सियतों में होता है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अवाम की लड़ाई लड़ने में गुज़ार दी. सुर्ख़ परचम के तले उन्होंने आज़ादी की तहरीक में हिस्सेदारी की. आज़ादी की तहरीक के दौरान उन्होंने न सिर्फ़ साम्राज्यवादी अंग्रेज़ी हुकूमत से टक्कर ली, बल्कि अवाम को सामंतशाही के खिलाफ़ भी बेदार किया.
मख़दूम की क़ौमी नज़्मों का कोई सानी नहीं था. जलसों में कोरस की शक्ल में जब उनकी नज़्में गाई जातीं, तो एक समां बंध जाता. हज़ारों लोग आंदोलित हो उठते. ‘‘वो हिन्दी नौजवां यानी अलम्बरदार-ए-आज़ादी/वतन का पासबां वो तेग-ए-जौहर दार-ए-आज़ादी.’’ (‘आज़ादी-ए-वतन’) और ‘‘ये जंग है, जंग-ए-आज़ादी के लिए’’ इन नज़्मों ने तो उन्हें हिन्दुस्तानी अवाम का महबूब और मक़बूल शायर बना दिया. मुल्क की आज़ादी की तहरीक के दौरान अंगेज़ी हुकूमत का विरोध करने के जुर्म में मख़दूम कई मर्तबा जेल भी गए, पर उनके तेवर नहीं बदले.
मख़दूम मोहिउद्दीन ने न सिर्फ़ आज़ादी की तहरीक में हिस्सेदारी की, बल्कि अवामी थियेटर में मख़दूम के गीत जोश-ओ-खरोश से गाए जाते थे. किसान और मज़दूरों के बीच जब इंक़लाबी मुशायरे होते, तो मख़दूम उसमे पेश-पेश होते. उनकी क़लम से साम्राज्यवाद विरोधी नज़्म ‘आज़ादी-ए-वतन’ व सामंतवाद विरोधी ‘हवेली’, ‘मौत के गीत’ जैसी कई इंक़लाबी नज़्में निकलीं. आलमी जंग का जब आग़ाज़ हुआ, तो मुल्क की अवामी तहरीकों पर भी हमला हुआ. इन हमलों से तहरीक कमज़ोर होने की बजाए और भी ज़्यादा मज़बूत होकर उभरी. साम्राजी तबाहकारी, हिंसा और अत्याचार के माहौल की फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और मख़दूम ने अपनी नज़्मों में बड़े पुर—असर अंदाज़ में अक्कासी की. साम्राजी जंग के दौर में मुश्किल से आधा दर्जन ऐसी नज़्में कही गई होंगी, जिनसे जंग की असल हक़ीक़त वाज़ेह होती हैं और उनमें भी आधी से ज़्यादा मख़दूम की हैं. मसलन ‘जुल्फ़-ए-चलीपा’, ‘सिपाही’, ‘जंग’, 'मशरिक़' और ‘अंधेरा’. ‘सिपाही’ नज़्म में वे जंग पर तनक़ीद करते हुए लिखते हैं, "कितने सहमे हुए हैं नज़ारे/
कैसे डर-डर के चलते हैं तारे/
क्या जवानी का ख़ूं हो रहा है/
सूखे हैं आंचलों के किनारे/
जाने वाले सिपाही से पूछो/
वो कहां जा रहा है ?’’
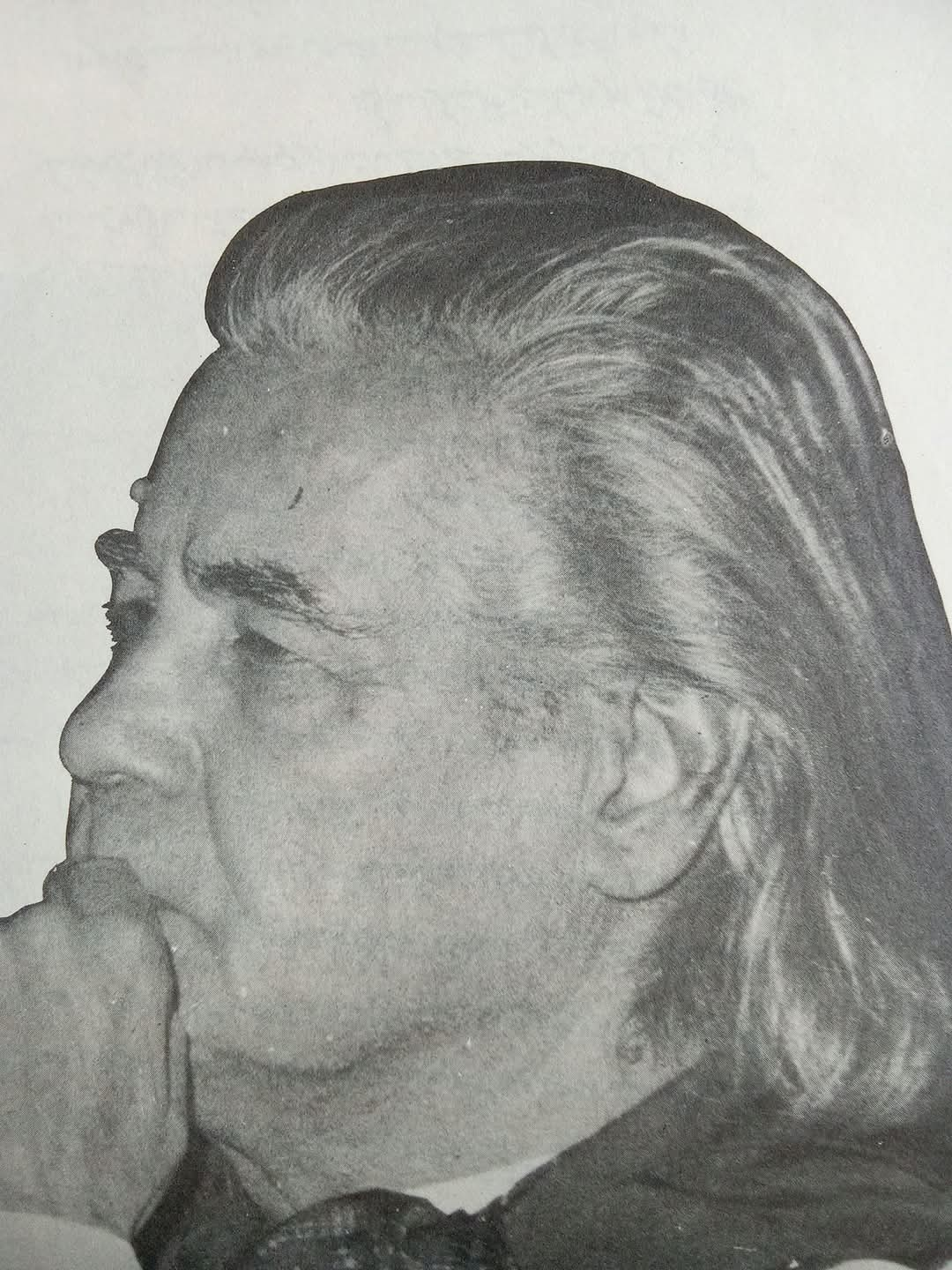 अली सरदार जाफ़री
अली सरदार जाफ़री
अली सरदार जाफ़री एक जोशीले अदीब, इंक़लाबी शायर थे. मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उन्होंने सरगर्म हिस्सेदारी की. सरदार जाफ़री अपने बाग़ियाना तेवर और इंक़लाबी सोच के चलते अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में जल्द ही मक़बूल हो गए. पढ़ाई से ज्यादा उनका दिल आज़ादी के आंदोलन में लगता. वे ऐसे मौके़ तलाश करते रहते, जिसमें बरतानिया हुकूमत और उसकी पॉलिसियों की मुख़ालफ़त कर सकें. एक मर्तबा जब यूनीवर्सिटी में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेम्बर आए, तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ हड़ताल कर दी. बहरहाल, इस हड़ताल करने के इल्ज़ाम में अली सरदार जाफ़री को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया. अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ़ आंदोलन और साम्राज्य विरोधी नज़्मों की वजह से अली सरदार जाफ़री को भी कई मर्तबा जेल जाना पड़ा. उनकी कई बेहतरीन नज़्में जेल की सलाख़ों के पीछे ही लिखीं गई हैं.
‘बग़ावत’, ‘अहद-ए-हाज़िर’, ‘सामराजी लड़ाई’, ‘इंक़लाब-ए-रूस’, ‘मल्लाहों की बग़ावत’, ‘फ़रेब’, ‘सैलाब-ए-चीन’, ‘जश्न-ए-बग़ावत’ आदि नज़्मों में उन्होंने अपने समय के बड़े सवालों को उठाया है. सच बात तो यह है कि उन्होंने अपने आसपास के मसाइल से कभी मुंह नहीं चुराया, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की. बंगाल का जब भयंकर अकाल पड़ा, तो अली सरदार जाफ़री की क़लम ने लिखा,‘‘चंद टुकड़ों के लिए झांसी की रानी बिक गई/आबरू मरियम की सीता की जवानी बिक गई/गांव वीरां हो गए हर झोंपड़ा सुनसान है/खित्ता-ए-बंगाल है या एक कब्रिस्तान है.’’
मुल्क की आज़ादी बंटवारा लेकर आई. साम्राज्यवादी साजिशों के चलते मुल्क भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गया. तमाम तरक़्क़ी-पसंद शायरों के साथ अली सरदार जाफ़री भी इस बंटवारे के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने अपने तईं इसकी मुखालफत भी की. नज़्म ‘आंसुओं के चराग’ में वे अपने जज़्बात को कुछ इस तरह से पेश करते हैं, "ये कौन जालिम है जिसने क़ानून के दहकते हुए क़लम से/वतन के सीने पै ख़ून-ए -नाहक़ की एक गहरी लकीर खींची."
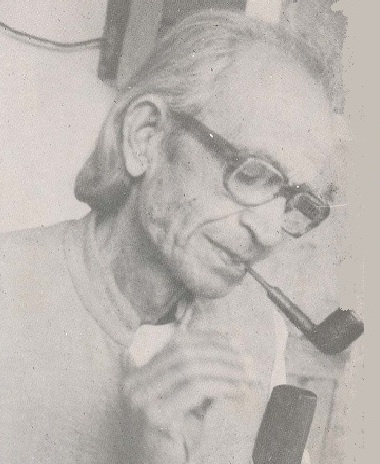 वामिक़ जौनपुरी
वामिक़ जौनपुरी
‘‘भूका है बंगाल रे साथी, भूका है बंगाल’’ वह नज़्म है, जिससे शायर वामिक़ जौनपुरी की शोहरत पूरे मुल्क में फैली. इस नज़्म का पसमंज़र साल 1943 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल है. इस अकाल में उस वक़्त एक आंकड़े के मुताबिक करीब तीस लाख लोग भूख से मारे गए थे. वह तब, जब मुल्क में अनाज की कोई कमी नहीं थी. गोदाम भरे पड़े हुए थे. बावजूद इसके लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था. एक तरफ लोग भूख से तड़प-तड़पकर मर रहे थे, दूसरी ओर अंग्रेज़ सरकार के कान पर जूं तक नही रेंग रही थी. बंगाल के ऐसे अमानवीय और संवेदनहीन हालात की तर्जुमानी ‘भूका है बंगाल’ नज़्म में है.
‘‘पूरब देस में डुग्गी बाजी फैला दुख का जाल/दुख की अगनी कौन बुझाये सूख गए सब ताल/जिन हाथों ने मोती रोले आज वही कंगाल रे साथी/आज वही कंगाल/भूका है बंगाल रे साथी भूका है बंगाल.’’ इप्टा के ‘बंगाल स्क्वॉड’ और सेंट्रल स्क्वॉड ने ‘भूका है बंगाल’ नज़्म की धुन बनाई और चंद महीनों के अंदर यह तराना मुल्क के कोने-कोने में फैल गया.
इस नज़्म ने लाखों लोगों के अंदर वतन-परस्ती, एकता और भाईचारे के जज़्बात जगाए. इप्टा के कलाकारों ने नज़्म को गा-गाकर बंगाल रिलीफ़ फंड के लिए हज़ारों रुपए और अनाज बंगाल के लिए इकट्ठा किया. जिससे लाखों हम—वतनों की जान बची.
 लेखक के बारे में : भारतीय साहित्य में चले प्रगतिशील आंदोलन पर लेखक, पत्रकार ज़ाहिद ख़ान का विस्तृत कार्य है. उनकी कुछ अहम किताबों की फ़ेहरिस्त इस तरह है-‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’, ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र’, ‘तहरीक-ए-आज़ादी और तरक़्क़ीपसंद शायर’ और ‘आधी आबादी अधूरा सफ़र’. ज़ाहिद ख़ान ने कृश्न चंदर के ऐतिहासिक रिपोर्ताज ‘पौदे’, अली सरदार जाफ़री का ड्रामा ‘यह किसका ख़ून है’ और हमीद अख़्तर की किताब ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ का उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण किया है. ‘
लेखक के बारे में : भारतीय साहित्य में चले प्रगतिशील आंदोलन पर लेखक, पत्रकार ज़ाहिद ख़ान का विस्तृत कार्य है. उनकी कुछ अहम किताबों की फ़ेहरिस्त इस तरह है-‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’, ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र’, ‘तहरीक-ए-आज़ादी और तरक़्क़ीपसंद शायर’ और ‘आधी आबादी अधूरा सफ़र’. ज़ाहिद ख़ान ने कृश्न चंदर के ऐतिहासिक रिपोर्ताज ‘पौदे’, अली सरदार जाफ़री का ड्रामा ‘यह किसका ख़ून है’ और हमीद अख़्तर की किताब ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ का उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण किया है. ‘
शैलेन्द्र हर ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर में’ और ‘बलराज साहनी एक समर्पित और सृजनात्मक जीवन’ किताबों का संपादन भी उनके नाम है. उनकी चर्चित किताब ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’ मराठी और उर्दू ज़़बान में अनुवाद हो, प्रकाशित हो चुकी हैं. इस किताब के लिए उन्हें ‘मध्य प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ के ‘वागीश्वरी पुरस्कार’ से भी नवाज़ा गया.
