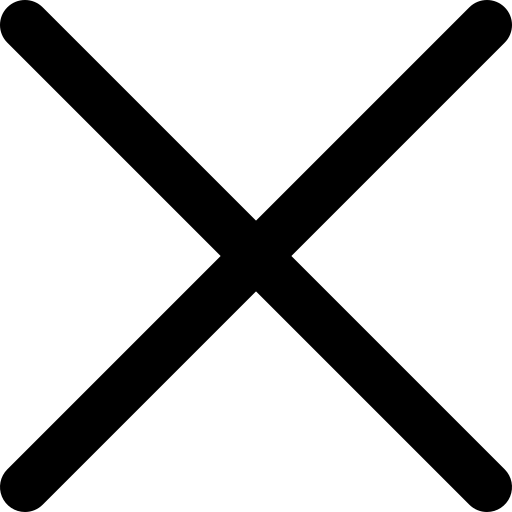फ़िरदौस ख़ान
दस्तकारी यानी हस्तकला एक ऐसा हुनर है, जिससे किसी भी मामूली चीज़ को बेहद ख़ूबसूरत बनाया जा सकता है. दस्तकारी से सजावट की चीज़ें भी बनाई जाती हैं और काम में आने वाला सामान भी बनाया जाता है. दस्तकारी का हुनर सदियों से चला आ रहा है. चूंकि दस्तकारी रोज़गार से जुड़ी हुई है, इसलिए दस्तकार पीढ़ी-दर- पीढ़ी ये हुनर अपने बच्चों को सिखाते रहे हैं. राजाओं-महाराजाओं और बादशाहों ने इस हुनर को ख़ूब बढ़ावा दिया. इसीलिए पुराने ज़माने में बेरोज़गारी का नामो-निशान तक नहीं था. जितने हाथ थे, उतने ही काम भी थे. पुश्तैनी काम होने की वजह से रोज़गार की कोई समस्या ही नहीं थी.
फिर वक़्त बदला और मशीनें आ गईं. इनकी वजह से दस्तकारी के काम को बहुत ही नुक़सान पहुंचा. लोग मशीनों से बनी चीज़ें ख़रीदने लगे. रफ़्ता-रफ़्ता दस्तकारी की बातें किताबों में सिमटने लगीं. लेकिन इस सबके दरम्यान छोटे क़स्बों और गांव-देहात में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने हुनर को थामे रखा. उन्हें अपने हुनर से इतनी मुहब्बत थी कि वे इसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे, भले ही उन्हें इससे कोई ख़ास आमदनी नहीं होती थी. दस्तकारों का कहना है कि यही हुनर तो उनकी पहचान है. भला क्या कोई अपनी पहचान को खोकर ख़ुश रह सकता है ? इसी लगाव ने उन्हें अपने पुश्तैनी काम से जोड़े रखा. उन्होंने अपने बच्चों को भी ये हुनर सिखाया. वे अपनी अगली पीढ़ी को काम की बारीकियां सिखाते हैं. वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा हुनरमंद हों और ख़ूब नाम कमायें.
.jpeg)
बहुत से दस्तकारों के बेटे तो आमदनी न होने की वजह से अपना पुश्तैनी काम-धंधा छोड़कर कोई दूसरा काम करने लगे या फिर वे काम की तलाश में दूर-दराज़ के इलाक़ों में चले गए. लेकिन कुछ युवाओं ने अपने इस हुनर को ज़िन्दा रखा. ऐसे ही एक युवा हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज के मोहम्मद मुरसलीन. वे चमड़े की दस्तकारी में माहिर हैं. वे कहते हैं कि जो लोग अपना पुश्तैनी काम छोड़ देते हैं, इतिहास से उनका नाम भी मिट जाता है. उनके शानदार हुनर के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाज़ा जा चुका है. गुज़श्ता साल जनवरी में उन्हें उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ये दक्षता पुरस्कार उन्हें चमड़े के ख़ूबसूरत फूलदान बनाने के लिए दिया गया. इस पुरस्कार में उन्हें प्रशस्ति पत्र, एक ताम्र पत्र, शॉल और 20 हज़ार रुपये का चेक दिया गया.
ग़ौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा राज्य में हस्तकला को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार दिए जाते हैं. इसके तहत दो तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं. पहला राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार और दूसरा दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार. इन पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं. जिन शिल्पियों के पास प्रादेशिक पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा जारी हस्तशिल्प पहचान पत्र है, वे अपनी सहभागिता के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्र एवं कलाकृतियां, शिल्पी पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ कार्यालय में जमा करा देते हैं. कार्यालय द्वारा पुरस्कार के लिए शिल्पियों का चयन किया जाता है.
दरअसल इन पुरस्कारों के ज़रिये दस्तकारों को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे अपने पुश्तैनी काम से विमुख न हों और स्वरोज़गार अर्जित करें. लगातार घटती नौकरियों और बढ़ती बेरोज़गारी के मद्देनज़र देशभर में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया जा रहा है. स्वरोज़गार के कई फ़ायदे हैं. इसमें व्यक्ति ख़ुद मालिक होता है. जहां वह अपने लिए रोज़गार जुटाता है, वहीं दूसरों को भी रोज़गार देने वाला बन जाता है.
मुहम्मद मुरसलीन बताते हैं कि दस्तकारी का उनका पुश्तैनी काम है. उनके परिवार में ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है. पहले ज़माने में धातु और प्लास्टिक के बर्तन नहीं हुआ करते थे. उस वक़्त लोग सामान रखने के लिए मिट्टी और चमड़े से बनी चीज़ों का इतेमाल किया करते थे. ख़ासकर तेल रखने के लिए चमड़े से बने बड़े-बड़े कूपों का इस्तेमाल किया जाता था. वे बताते हैं कि फ़िल्म ‘अली बाबा चालीस चोर’ में तेल रखने के लिए जिन बड़े-बड़े कूपों का इस्तेमाल किया गया है, वे चमड़े के ही बने हुए थे. वे कहते हैं कि पहले के वक़्त में यातायात के आज जैसे साधन नहीं थे. उस वक़्त लोग ऊंट, घोड़े और बैलगाड़ी के ज़रिये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. ऐसे में मिट्टी के बर्तन रास्ते के लिए मुनासिब नहीं थे. उनके टूटने का डर रहता था. इसलिए सफ़र के दौरान चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था.

चमड़े से चीज़ें बनाने का काम आसान नहीं है. इसमें बहुत ही महारत की ज़रूरत होती है. इसके साथ-साथ इसमें मेहनत- मशक़्क़त भी बहुत करनी पड़ती है. सारा काम हाथ से होता है. उनके दादा अब्दुल करीम भी बहुत अच्छे और माने हुए दस्तकार थे. उनका बहुत नाम था. उनकी बनाई हुई चीज़ें दूर-दूर तलक जाती थीं. उन्होंने अपने बेटे मुस्तक़ीम को भी ये नायाब हुनर सिखाया. उनके वालिद मुस्तक़ीम भी दस्तकारी में बहुत ही माहिर हैं. उन्होंने भी बहुत नाम कमाया, लेकिन वे भी माल व दौलत नहीं कमा पाये. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस काम में जितनी लागत लगती है और जितनी मेहनत होती है, उस हिसाब से आमदनी नहीं होती.
मुहम्मद मुरसलीन देशभर में आयोजित होने वाली हस्तकला प्रदर्शनियों में शिरकत करते हैं. वे देश की राजधानी दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और मथुरा आदि शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं. उनका सामान विदेशों तक में जाता है. वे बताते हैं कि कारोबारी उनसे फूलदान ख़रीदकर उस पर नक़्क़ाशी करवाकर उन्हें विदेशों में महंगे दामों पर बेचते हैं. विदेशों में हिन्दुस्तानी कलाकृतियों की भारी मांग है.
इन प्रदर्शनियों में दस्तकार अपनी बनाई हुई कलाकृतियों और सामान का प्रदर्शन करते हैं. इन्हें देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और उनका सामान ख़रीदते हैं. इनमें ऐसे कारोबारी भी शामिल होते हैं, जो इन कलाकृतियों को ख़रीदकर विदेशों में बेचते हैं. चीज़ें पसंद आने पर वे दस्तकारों को अपनी पसंद की चीज़ें बनाने का ऑर्डर भी देते हैं.
दस्तकारों का कहना है कि इस काम में बिचौलियों को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है. ज़्यादातर दस्तकार पढ़े-लिखे नहीं हैं. उन्हें कलाकृतियां बनानी तो आती हैं, लेकिन वे उन्हें बेचने का हुनर नहीं जानते. ऐसे में वे अपना सामान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर हैं. दस्तकारों की सरकार से मांग है कि वे चमड़े की दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए ख़ास क़दम उठाए और दस्तकारों को बाज़ार भी मुहैया कराए, ताकि उन्हें उनकी मेहनत की वाजिब क़ीमत मिल सके.
(लेखिका शायरा, कहानीकार व पत्रकार हैं)
.webp)
.jpeg)