भारत के पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं अब कोई असामान्य घटनाएं नहीं रहीं, बल्कि एक भयावह और अनुमानित वार्षिक त्रासदी का रूप ले चुकी हैं. पिछले हफ्ते, जब मैं अपनी मासिक यात्रा पर भारत के पहाड़ों की ओर गया,जहां मैं अक्सर शांति और सुकून की तलाश करता हूं,तो मुझे आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा. मेरे ये शांत, सौम्य पहाड़ अब मानो मुझ पर थूक रहे थे. उन्होंने अपने भीतर जो विनाश, उपेक्षा और लापरवाही सहन की है, अब वह आक्रोश के रूप में फूट रहा है. इंसानी लालच ने इन वनों, नदियों और पर्वतों को एक खतरनाक रंगमंच में बदल दिया है, जहां अब प्रकृति पलटवार कर रही है.
पर्वतों का यह आक्रोश बादल फटने, अचानक बाढ़, ग्लेशियरों के फटने और भूस्खलनों के रूप में सामने आ रहा है. ये घटनाएं अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आम होती जा रही हैं.
घर उजड़ रहे हैं, सड़कें बह रही हैं, ज़िंदगियाँ खत्म हो रही हैं और सपने मलबे में दफन हो रहे हैं. यह सब महज़ जलवायु परिवर्तन का परिणाम नहीं है, बल्कि विकास के नाम पर की गई लापरवाह मानवीय गतिविधियों, प्रशासनिक लापरवाही और पर्यावरणीय संतुलन की उपेक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण है.
हिमाचल प्रदेश इस त्रासदी का एक जीवंत उदाहरण है. हाल ही में, चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग के हिस्से बह गए या मलबे में दब गए. 360 से अधिक सड़कों का संपर्क टूट गया और मंडी और कुल्लू जिलों में 1,988 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
20 जून से 10 जुलाई के बीच, नदियों के किनारे हुए अवैध निर्माणों ने हिमाचल को लगभग 750 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया. स्थानीय समुदाय अलग-थलग पड़ गए और राज्य की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई.
उत्तराखंड में भी हालात गंभीर हैं. धराली कस्बा, जो अपने सेबों के लिए जाना जाता है, एक ही मिनट में बर्बाद हो गया. लगातार आने वाली बाढ़ों ने गांवों और कस्बों को बहा दिया. कई इलाके मलबे में दब गए, हजारों लोग अपनी ज़िंदगी खो बैठे और कृषि भूमि पूरी तरह नष्ट हो गई.
गंगोत्री जैसे तीर्थस्थलों तक पर प्रकृति का कहर टूटा है. बाढ़ ने 300 दुकानों को तबाह कर दिया और 100 करोड़ रुपये की आय को नष्ट कर दिया.जम्मू-कश्मीर का हाल भी कुछ अलग नहीं है. किश्तवाड़ ज़िले के चोसिटी गांव में मचैल माता यात्रा के दौरान बादल फटने से आई बाढ़ में 63 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 300 घायल हुए.
200 से ज्यादा लोग लापता हो गए. कुछ ही दिनों में कठुआ में हुए भूस्खलन में 21 लोगों की मौत हुई. जोशीमठ और थाथरी में ज़मीन धंसने के चलते लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं.
पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर सिक्किम, पहले से ही खतरे के निशान पर है। 2023 की भयावह बाढ़ के बाद भी खतरा कम नहीं हुआ. दक्षिण ल्होनक झील बार-बार फट रही है, जिससे भारी भूस्खलन और तबाही हो रही है. पूरे इलाके में भूस्खलन की घटनाओं में छह गुना वृद्धि हुई है और 17,000 से अधिक खतरे वाले स्थान चिन्हित किए गए हैं.
इन घटनाओं की भयावहता को समझना तब आसान हो जाता है जब आप वहां बचे लोगों की कहानियां सुनते हैं. हर जगह एक ही दर्दनाक बयान सुनने को मिलता है: "अचानक आसमान से पानी की दीवारें गिरीं और सब कुछ बहा ले गईं…" ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं. यह मानव निर्मित आपदाएं हैं, जिनकी जड़ें हैं लापरवाही, लालच और अदूरदर्शिता में.

दरअसल, सरकारें हिमालयी राज्यों में सड़क निर्माण और पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर जिस तरह का ‘विकास’ कर रही हैं, उसने इस नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की जड़ों को हिला दिया है. छह से आठ लेन वाले राजमार्ग बनाने के लिए पहाड़ों की ढलानों को विस्फोट से उड़ाया जा रहा है, जंगलों को बेरहमी से काटा जा रहा है और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है.
इस तरह की गतिविधियां न केवल भूस्खलन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि बाढ़ के समय पानी को सही रास्ता नहीं मिलने से पूरे गांव मलबे में तब्दील हो जाते हैं.
होटल और रिसॉर्ट्स भी इसी अव्यवस्था का हिस्सा हैं. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नदियों के किनारे और अस्थिर ढलानों पर निर्माण कार्य किए गए हैं, जिनमें पर्यावरणीय मंजूरी और ज़ोनिंग कानूनों की खुली अवहेलना की गई है. ये निर्माण मामूली बारिश में भी ढह जाते हैं, और जब बादल फटते हैं, तो इनमें रहने वाले लोगों की जान पर बन आती है.
स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. ज़्यादातर मामलों में इन अवैध निर्माणों को अनदेखा किया जाता है, यहां तक कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है. पर्यावरणविद और वैज्ञानिक वर्षों से चेतावनी देते आ रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों और राजनेताओं की मिलीभगत ने उनकी आवाज़ों को दबा दिया है.
हिमालय क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाएं भी एक बड़ा संकट बन चुकी हैं. नाज़ुक पहाड़ों के भीतर सुरंगें खोदकर बनाई गई इन परियोजनाओं ने पहाड़ों की स्थिरता को नुकसान पहुंचाया है. इन परियोजनाओं से निकला मलबा नदियों और घाटियों में फेंका जा रहा है, जिससे प्राकृतिक जल प्रवाह अवरुद्ध होता है और बाढ़ की तीव्रता बढ़ जाती है.
इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन की मार लगातार तेज़ होती जा रही है. हिमालय दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में दोगुनी गति से गर्म हो रहा है, जिससे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं. इससे झीलों के फटने और अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं.
पहले जहां मानसून धीरे-धीरे आता था और महीनों तक स्थिर रहता था, अब एक घंटे में महीने भर की बारिश हो जाती है, जिससे मिट्टी ढलानों से बह जाती है और भूस्खलन होते हैं.प्राकृतिक आपदाओं की यह बढ़ती श्रृंखला सिर्फ पर्यावरण का मामला नहीं है,यह एक मानवीय त्रासदी है.
जिन लोगों ने अपने घर, परिवार, जानवर और ज़िंदगी खो दी है, उनके लिए यह हमेशा का दर्द बन गया है. किसानों की ज़मीनें बर्बाद हो चुकी हैं, मवेशी मारे गए हैं, और कई परिवार बेसहारा हो गए हैं. बाढ़ में खोए बच्चों की तलाश में माता-पिता अब भी दर-दर भटक रहे हैं. सैलानी, जो पहाड़ों की खूबसूरती देखने आए थे, अब ताबूतों में लौट रहे हैं.
यह विकास नहीं है,यह विनाश है। जिन सड़कों, होटलों और जल परियोजनाओं को 'प्रगति' का प्रतीक माना गया, वे अब राष्ट्रीय त्रासदी के स्मारक बनते जा रहे हैं. जब-जब आसमान फटता है, शोषित पारिस्थितिक तंत्र मानो चीख-चीख कर चेतावनी देता है: अब और नहीं.
अब सवाल यह है: ये पागलपन कब रुकेगा? क्या सरकारें अब भी तात्कालिक आर्थिक फायदे को दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन पर तरजीह देती रहेंगी? क्या पर्यावरणीय नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा या फिर भ्रष्टाचार के खेल में वे भी मिट्टी में दब जाएंगे? क्या स्थानीय लोग अपनी पुश्तैनी ज़मीनों को यूं ही बहते देखने को मजबूर रहेंगे?

भारत को अब यह समझना होगा कि हिमालय कोई निर्माण क्षेत्र नहीं है,यह जीवनदायी पारिस्थितिक तंत्र है, जो न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवनरेखा भी है. यह समय है जब हम विकास की परिभाषा पर पुनर्विचार करें.
ALSO READ धर्म नहीं, मानवता: किश्तवाड़ की आपदा में एकजुट हुआ पूरा समाज
जब तक हम अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगे, तब तक आसमान से मौत की बारिश होती रहेगी.हमें प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि एक साझेदार के रूप में देखना होगा. वरना, वो दिन दूर नहीं जब ये पहाड़ हमें हमेशा के लिए अपने भीतर समा लेंगे.












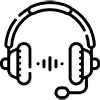

 राजीव नारायण
राजीव नारायण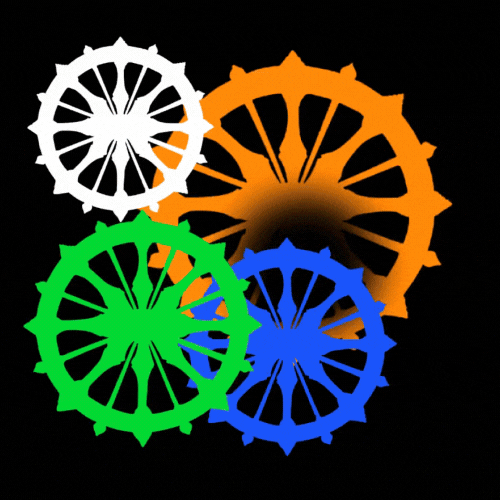

.jpg)

.jpg)

.jpg)








