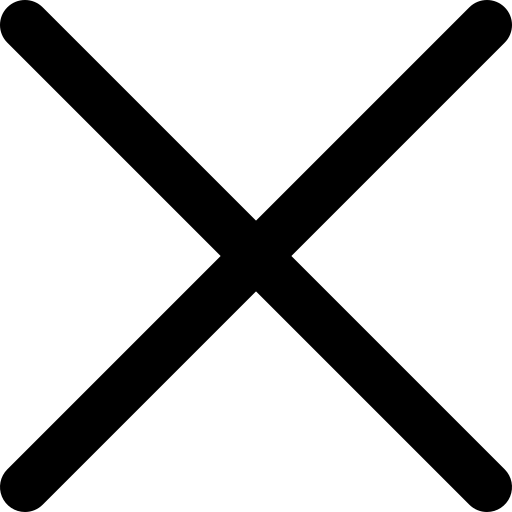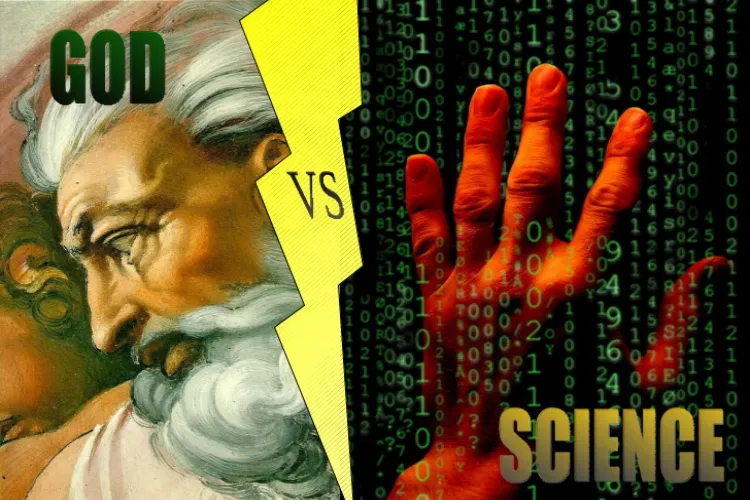
अमीर सुहैल वानी
लोग हमारी पोषित और लंबे समय से चली आ रही धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं पर बढ़ते विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर बहस कर रहे हैं. आम धारणा यह है कि वैज्ञानिक शिक्षा की प्रगति के साथ, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं ने अपना मूल्य खो दिया है और लोगों को अपना विश्वास छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है. लेकिन आस्था, मानव सभ्यता के मूल सिद्धांतों में से एक है और धार्मिक विश्वासों के अभाव में, नैतिक ताने-बाने के क्षरण का खतरा पैदा हो जाता है और पूरी संस्कृति अभद्रता, अपराध, बर्बरता और अमानवीयकरण की चपेट में आ जाती है.
इस प्रकार हमारे विश्वासों और आस्था प्रणालियों पर उभरती वैज्ञानिक मानसिकता के प्रभाव की जांच करना और यह देखना अपरिहार्य हो जाता है कि हम ऐतिहासिक आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति अपनी आस्था और समर्पण से समझौता किए बिना इन नवीनतम वैज्ञानिक विकासों से कैसे लाभ उठा सकते हैं.
समस्या को उसके वर्तमान संदर्भ में समझने के लिए, हमें इस ‘धर्म-विज्ञान विवाद’ के ऐतिहासिक विकास की कुछ समझ की आवश्यकता है और इसके ऐतिहासिक विकास के संबंध में इसकी वर्तमान अभिव्यक्तियों को समझने का प्रयास करें.
यूरोपीय ज्ञानोदय के उदय और पुनर्जागरण के युग के आगमन के साथ, यूरोप में विश्वास की पुरानी प्रणालियों को गहराई से हिला दिया गया और विचार और कार्य की नई आदतों को पश्चिम में मजबूती मिली.
दर्शनशास्त्र में यांत्रिक विज्ञान और अनुभववाद के उदय के साथ, विचार की पुरानी प्रणालियों की सख्ती से आलोचना की गई और उन पर विनाशकारी हमले किए गए. इसी भावना के साथ डेविड ह्यूम ने जोरदार ढंग से यह घोषणा की कि ‘‘यदि हम अपने हाथ में कोई भी मात्रा लेते है, उदाहरण के लिए, देवत्व या स्कूल तत्वमीमांसा, आइए हम पूछें, क्या इसमें मात्रा या संख्या से संबंधित कोई अमूर्त तर्क है?
नहीं, क्या इसमें तथ्य और अस्तित्व के विषय में कोई प्रयोगात्मक तर्क शामिल है? नहीं, इसे आग की लपटों के हवाले कर दो, क्योंकि इसमें कुतर्क और भ्रम के अलावा कुछ नहीं हो सकता.’’
लेकिन यह एक अतिवादी और झूठा रुख था और उस युग के दार्शनिक यह भूल गए कि मानव जाति सदियों से धार्मिक और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के साथ जी रही है और मानव इतिहास के बेहतरीन पात्र इन पारंपरिक विरासतों और आध्यात्मिक विरासतों के अग्रदूत रहे हैं. पश्चिम में विज्ञान और धर्म का टकराव चर्च और अपने-अपने क्षेत्रों में उभरते विज्ञान की जिद के कारण और भी बढ़ गया.
जब वैज्ञानिक नई खोज कर रहे थे और ज्ञान के नए रास्ते खोल रहे थे, पोप और पादरी ने बिना किसी कारण और तुकबंदी के उनका विरोध किया, जिससे अंततः मध्ययुगीन यूरोप में विज्ञान और धर्म के बीच समझौता न हो सकने वाला समझौता हो गया.
पादरी वर्ग के हाथों टाइको ब्राहे, गैलीलियो और अन्य वैज्ञानिकों के भाग्य-निर्णय ने वैज्ञानिक समुदाय को कठोर बना दिया और वे धर्म और पारंपरिक मूल्यों के विरोध में और भी आगे बढ़ गए. लेकिन ये यूरोप के लिए विशिष्ट परिस्थितियां थीं और यह विज्ञान बनाम धर्म विभाजन विशेष रूप से एक यूरोपीय घटना थी.
पूर्व में - भारत और इस्लामी भूमि में, सबसे बड़े वैज्ञानिक कारनामे अक्सर उन लोगों द्वारा किए जाते थे, जो गहरे धार्मिक थे और उन्हें अपने धार्मिक विश्वासों और उनकी नई खोजों के बीच किसी भी तरह के मतभेद का सामना नहीं करना पड़ा था. इस प्रकार पूर्व कुल मिलाकर ‘मन-पदार्थ, शरीर-आत्मा, पवित्र-अपवित्र, दैवीय-सांसारिक संघर्ष’ से मुक्त था, जिसने सदियों से पश्चिम पर आक्रमण किया था.
हालांकि, हमारे जीवन में विज्ञान की प्रचुरता और विज्ञान की अभिव्यक्तियों की बहुलता के साथ, पूर्व में पारंपरिक मूल्य भी ढहने लगे हैं और विज्ञान की छाप के तहत उभर रहे नए दर्शन पारंपरिक मूल्यों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं.
वैज्ञानिक भौतिकवाद के चक्कर में लोग तेजी से अपने सदियों पुराने मूल्यों और गुणों तथा मुनाफाखोरी और भौतिकवाद को त्याग रहे हैं. धर्म के बारे में यह गलतफहमी कई कारणों से हुई है, जिसे अब हम संबोधित करने का साहस कर रहे हैं और ऐसा करते हुए विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य के संबंध में आगे का रास्ता रेखांकित करते हैं.
धर्म और विज्ञान के बीच संबंधों पर चर्चा करते समय जिस प्राथमिक तथ्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वह है ‘नॉन-ओवरलैपिंग मैजेस्ट्रिया’ का सिद्धांत. यह सिद्धांत मानता है कि जहां विज्ञान अपनी तथ्यात्मक सामग्री के साथ भौतिक ब्रह्मांड की चिंता करता है, वहीं धर्म का विषय आध्यात्मिक ब्रह्मांड है, जिसमें मूल्यों, सौंदर्यशास्त्र, नैतिकता और समान सामग्री शामिल है.
इस प्रकार ये डोमेन ओवरलैप नहीं होते हैं और जबकि भौतिक और धार्मिक विज्ञान अपने वैध डोमेन में काम करना जारी रख सकते हैं, उन्हें अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और इस तरह अराजकता और भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए. यदि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए, तो ‘धर्म-विज्ञान’ के झगड़े के कारण उत्पन्न होने वाले अधिकांश भ्रम को दूर किया जा सकता है.
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर विशेष उल्लेख की आवश्यकता है, वह यह है कि धार्मिक ग्रंथ, चाहे वह कुरान हो या वेद, प्रतीकात्मक और रूपक भाषा में लिखे गए हैं और इसलिए ऐसे ग्रंथों को शाब्दिक रूप से पढ़ने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए. यह आम लोगों की धर्मग्रंथों को अक्षरशः पढ़ने की प्रथा ही है, जो वैज्ञानिक और अन्यथा दोनों तरह से बहुत सारी परेशानी लाती है.
उल्लेख योग्य तीसरा तथ्य यह है कि विज्ञान की अंतिमता का कोई दावा नहीं है और इसके सभी परिणाम अनंतिम हैं और परिवर्तन और समीक्षा के अधीन हैं. इस प्रकार हम अपने नैतिक दृष्टिकोण को किसी ऐसी प्रणाली पर आधारित नहीं कर सकते हैं, जिसकी नींव अभी भी हिल रही है और जिसने अभी तक अपने स्वयं के नुकसान को परिभाषित नहीं किया है. इस संबंध में, यह व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक आवाज के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम नैतिकता की प्रणालियों के प्रति वफादार रहें, जो हमें हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा सौंपी गई हैं और जैसा कि वे सदियों से प्रचलित हैं.
एक नई प्रवृत्ति भी क्षितिज के आसपास है और यह प्रवृत्ति विज्ञान और आध्यात्मिकता के क्षितिज को एक गहरे संश्लेषण में मिलाने की कोशिश करती है, जिसकी समानता अब तक संतों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए अज्ञात रही है. बोह्र, पाउली, श्रोडिंगर, फ्रिथजॉफ कैप्रा, रूपर्ट शेल्ड्रेक, दीपक चोपड़ा, अमित गोस्वामी और अन्य वैज्ञानिकों के कार्यों और प्रेरणाओं के बाद, वैज्ञानिक अब विज्ञान और रहस्यवाद के बीच समानताएं तलाश रहे हैं, जो अब तक अज्ञात बने हुए थे.
क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और अन्य ब्रह्माण्ड संबंधी और प्राथमिक कण मॉडल में हाल की प्रगति हमें ब्रह्मांड की उसी तस्वीर की ओर ले जा रही है, जैसा कि युगों और देशों में ऋषियों, संतों और रहस्यवादियों द्वारा प्रचारित किया गया है. यह न केवल नियमित आस्तिक के लिए सांत्वना है, बल्कि इस अर्थ में फायदेमंद है कि विज्ञान, एक लंबी यात्रा के बाद उन्हीं निष्कर्षों पर वापस आ रहा है, जिन पर सहस्राब्दियों पहले धर्म और आध्यात्मिकता पहुंची थी. जैसे-जैसे विज्ञान में प्रगति हो रही है, न केवल वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि जीवन और चिकित्सा के पारंपरिक तरीके, जैसे योग और आयुर्वेद, एलोपैथी की प्रचलित यांत्रिक प्रणालियों की तुलना में कहीं अधिक फायदेमंद साबित हो रहे हैं.
हम रोमांचक समय में रह रहे हैं, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता के पास एक-दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है और इन दोनों के पास मिलकर मानवता को देने के लिए बहुत कुछ है. हमारा कार्य युग की चुनौतियों और अवसरों के प्रति खुला रहने और प्रत्येक वैज्ञानिक और धार्मिक परंपरा में जो सर्वोत्तम है, उसे आत्मसात करना है.
यदि मानवता का कोई भविष्य है, तो धर्म और आध्यात्मिकता का भी, लेकिन चुनौती प्रत्येक विचार प्रणाली को निष्पक्षता से अपनाने और मानव जीवन और अनुभव को रास्ते में आने वाले सर्वोत्तम से समृद्ध करने में है. वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्षितिज के संलयन में मानव जाति का भविष्य छिपा है - वह भविष्य जो उज्ज्वल, भौतिक रूप से संतुष्टिदायक और आध्यात्मिक रूप से संतुष्टिदायक है.