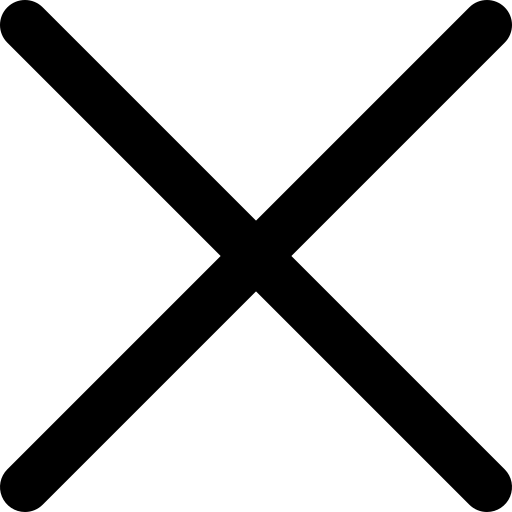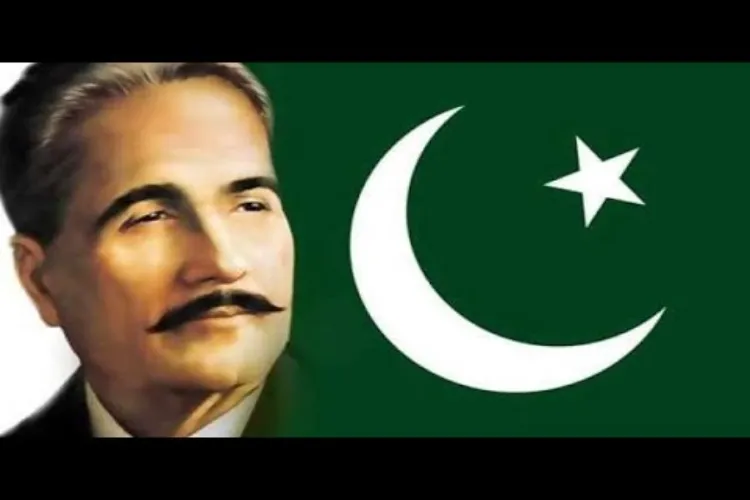
डॉ. फैयाज अहमद फैजी
भारत में विगत कुछ वर्षों से ऊर्दू दिवस मनाने का प्रचलन बढ़ रहा है. यह सर्व विदित है कि उर्दू का जन्म एवं विकास भारत देश में ही हुआ है. लेकिन हैरतअंगेज बात यह कि भारत में उर्दू दिवस का आयोजन पाकिस्तान के वैचारिक पिता अल्लामा इकबाल के जन्मदिन के जश्न के रूप में किया जा रहा है.
इकबाल वो पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान तहरीक की वैचारिकी उस समय प्रस्तुत की, जब बड़े से बड़े अशराफ लीडर के अंदर यह साहस नहीं था कि वो भारत के विभाजन के विचार को सार्वजनिक रुप से जाहिर कर पाएं.
यह उनके 29 दिसंबर 1930 में प्रयागराज (इलाहाबाद) में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण से स्पष्ट होता है. वो इतने कट्टर मुस्लिम लीगी और कांग्रेस विरोधी थे कि मौलाना थानवी की तरह उनकी भी यही राय थी कि कांग्रेस में मुसलमानों का बिना शर्त शामिल होना इस्लाम और मुसलमानों दोनों के लिए हानिकारक है. उनके द्वारा लिखित कुछ काव्य पंक्तियों के आधार पर उनकी अशराफवादी मानसिकता को समझा जा सकता है.
अपनी एक प्रसिद्ध कविता ‘वतनियत’ में इकबाल देश के बटवारे से उत्पन्न होने वाले स्थानांतरण को इस्लाम के प्रवर्तक के मक्का से मदीना स्थानांतरण से जोड़कर महिमा मंडन करते हुए लिखते हैंः
है तर्के वतन सुन्नते महबूबे इलाही
दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही
अर्थात अपने देश को छोड़ना ईश्वर के प्रिय (मुहम्मद) का आचरण है, तू भी इस प्रोफेटहुड की सच्चाई की गवाही दे, यानी उनकी तरह अपना देश छोड़कर निकल जाने को तैयार रह.
इकबाल की प्रारंभ की कविताओं में जरूर देश प्रेम झलकता है, लेकिन बाद की अपनी कविताओं में वो स्पष्ट रूप से राष्ट्र के स्वरूप को ही नकारते हुए वैश्विक इस्लामी राज्य का समर्थन करते हैंः
‘‘इन ताजा खुदाओं में, बड़ा सबसे वतन है
जो पैरहन (परिधान) उसका है, वो मजहब का कफन है’’
‘‘बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है
इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है’’
‘‘नज्जारा-ए-देरिना जमाने को दिखा दें
ऐ मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दें’’
अर्थात तुम्हारे हाथ एकेश्वरवाद की शक्ति के कारण शक्तिशाली है, इस्लाम ही तुम्हारा देश है, क्योंकि तू मुस्तफा (मुहम्मद का एक अन्य नाम) का अनुयायी है. यह पुराना अनुभवी दर्शन तू दुनिया को दिखा दे, ऐ मुहम्मद के अनुयायी - इस मूर्ति (राष्ट्र) को मिट्टी में मिला दें.
अपने ही द्वारा लिखित देश और देशभक्ति की भावपूर्ण कविता ‘सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा’ को रद्द करते हुए उसी बहर में इस्लामी राज्य के भाव को दर्शाती कविता यह हैः
‘‘चीन-व-अरब हमारा, हिन्दुस्तां हमारा,
मुस्लिम हैं हम वतन हैं, सारा जहां हमारा.’’
एक और कविता में वो लिखते हैंः
‘‘क्या नहीं और गजनवी कारगह-ए-हयात में बैठे, हैं कब से मुंतजिर अहल-ए-हरम के सोमनाथ.’’
अर्थात जीवन रूपी कार्यक्षेत्र में क्या अब और गजनवी (रूपी मूर्तिभंजक) नहीं हैं? क्योंकि अहले हरम (काबा, जहां पर पहले मूर्तियां थीं) के सोमनाथ इस इंतजार में हैं (कि उन्हें कब तोड़ा जाये.)
लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट उसकी सामाजिक और आर्थिक स्तिथि के निरपेक्ष बराबर होता है. इकबाल को इस बात से बहुत परेशानी थी और वो लोकतंत्र के इस स्वरूप पर व्यंग करते हैंः
‘‘जम्हूरियत (लोकतंत्र) इक तर्ज-ए-हुकूमत (शासन व्यव्स्था) है कि जिसमें,
बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते.’’
एक और कविता में वो लिखते हैंः
‘‘इलेक्शन मेम्बरी कौंसिल सदारत
बनाये हैं खूब आजादी ने फन्दे’’
‘‘मियां नज्जार भी छीले गए साथ
निहायत तेज है यूरोप के रन्दें’’
‘‘उठा के फेक दो बाहर गली में
नई तहजीब के अण्डे हैं गन्दे’’
इन पंक्तियों में लोकतंत्र के विभिन्न घटकों को फांसी के फंदे से उपमा देते हुए यह बताते हैं कि लोकतांत्रिक आजादी एक तरह से समाज की मौत की तरह है.
तथाकथित कामगर जाति नज्जार (बढ़ई) को रुपक के रूप में प्रयोग करते हुए वंचित समाज की तरफ इंगित करते हुए कहते है कि यूरोप के आधुनिक विचार लोकतंत्र, स्वतंत्रता, शिक्षा रूपी रन्दा से ये लोग भी छील दिए गए हैं.
मतलब इनका भी बहुत नुकसान हुआ है या होने वाला है, जबकि सच्चाई यह है कि इन आधुनिक विचारों का सबसे अधिक लाभ वंचित समाज को ही हुआ है. आखिर की दोनों पंक्तियों से साफ जाहिर होता है कि इकबाल आधुनिक विचारों यानी लोकतंत्र एवं आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे. वो अलग बात है कि स्वयं के बेटे को विदेश भेजकर आधुनिक शिक्षा दिलवायी थी, जो आगे चलकर पाकिस्तान का मुख्य न्यायधीश बना.
निम्नलिखित पंक्तियों से इकबाल के महिला विरोधी विचार स्पष्ट रूप से सामने आ जाते हैंः
‘‘न पर्दा, ना तालीम (शिक्षा) नई हो कि पुरानी
निस्वानियते जन का निगहबां है फकत मर्द.’’
(महिला के स्त्रीत्व का संरक्षक केवल पुरुष है)
‘‘जिस कौम ने इस जिन्दा हकीकत को ना माना,
उस कौम का खुर्शीद (सूरज) बहुत जल्द हुआ जर्द.’’
(जर्द माने पीला पड़ जाना, पतन हो जाना)
‘‘जिस इल्म (शिक्षा) की तासीर (प्रभाव) से जन (स्त्री) होती है बेजन (स्त्रीत्व खो देना)
कहते हैं इसी इल्म को अरबाबे नजर (विचारक) मौत.’’
लड़कियों के अंग्रेजी शिक्षा पर व्यंग करते हुए लिखते हैंः
‘‘लडकियां पढ़ रहीं हैं अंग्रेजी
ढूंढ ली कौम ने फलाह (भलाई) की राह.’’
‘‘रवीश मगरबी (पश्चिमी संस्कृति) है मद्दे (सामने) नजर
वज-ए-मशरिक (पूरबी संस्कृति यानि इस्लामी संस्कृति) को जानते हैं गुनाह’’
‘‘यह ड्रामा दिखाएगा क्या सीन
पर्दा उठने को मुंतजिर (प्रतीक्षारत) है निगाह.’’
इन कविताओं की पंक्तियों से इकबाल के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विचारक, अलोकतांत्रिक, राष्ट्र विरोधी, आधुनिकता विरोधी और महिला विरोधी विचार, जिसे एक शब्द में कहें, तो अशराफवादी विचार स्पष्ट रूप से सामने आ जाते हैं.
पकिस्तान में ‘इकबाल डे’ का आयोजन तो समझ में आता है कि वो पाकिस्तान के राष्ट्र कवि एवं वैचारिक निर्माता हैं, लेकिन भारत भूमि पर उर्दू की आड़ में इकबाल को एक राष्ट्रवादी, देशभक्त, गंगा-जमुनी तहजीब का वाहक, हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बताते हुए उनका महिमा मण्डन करके उनके जन्म दिन को उर्दू दिवस के रूप में मनाना, उसी अशराफवादी मानसिकता का द्योतक प्रतीत होता है, जिसने प्यारे भारत देश को टुकड़ों में बांट दिया.
एक तरफ तो यह तर्क दिया जाता है कि उर्दू किसी धर्म विशेष की जुबान नहीं है, यह भारत भूमि में जन्मी और फली-फूली एक भारतीय भाषा है और दूसरी ओर उसके उपलक्ष्य में दिवस का आयोजन एक ऐसे व्यक्ति की याद में किया जा रहा है, जिसने मजहबी संप्रदायकिता के आधार पर भारतभूमि के बटवारा को न सिर्फ उचित ठहराया, बल्कि जीवनपर्यंत समर्पित भी रहा.
ऐसा मालूम होता है कि द्विराष्ट्र सिद्धान्त रूपी अलगाववाद की मानसिकता को उर्दू के बहाने जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है. यह सर्व विदित है कि अशराफवादी मानसिकता के लोगों द्वारा उर्दू को मुसलमानों की जुबान बताकर इसे एक राजनैतिक टूल के रूप में पहले भी इस्तेमाल किया गया था और आज भी किया जाता रहा है.
उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र, राज्य या जनसमूह की भाषा न होने के बाद भी उर्दू पाकिस्तान की राज्य भाषा है और भारत का मुसलमान भी बंगाली-तेलगु आदि भाषाएं बोलने के बाद भी उर्दू को अपनी मातृभाषा समझता है.
यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ही उर्दू दिवस का आयोजन होना है, तो यह उन व्यक्तियों के नाम पर होना चाहिए, जिनका उर्दू भाषा एवं साहित्य के पालन-पोषण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इस सूची में भारत देश में जन्मे कई एक महान व्यक्तित्व मिल जायेंगे, जिनमें से कुछ के नाम यहां दर्ज कर देना उचित मालूम होता है.
उर्दू के प्रथम दीवान (काव्यसंग्रह) के लेखक चन्द्रभान जुन्नारदार (जनेऊधारी), पंडित रत्न लाल शर्शार, मुंशी ज्वाला प्रसाद बर्क, मुंशी नौबत राय नजर, पंडित बृज नारायण चकबस्त, पंडित आनंद नारायण मुल्ला, मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र और गोपीचंद नारंग या फिर उर्दू के लिए भूख हड़ताल कर अपना जीवन बलिदान करने वाले देव नारायण पांडेय एवं जय सिंह बहादुर.
पसमांदा आंदोलन की यह स्पष्ट मांग रही है कि उर्दू दिवस को इकबाल के जन्मदिवस के अवसर पर नहीं मनाया जाए, क्योंकि यह उर्दू को एक विदेशी एवं मजहबी साम्प्रदायिक रंग दे रहा है. बल्कि ऊपर लिखित उर्दू के महान साहित्यकार रहे देशज व्यक्तित्वों में से किसी के नाम पर हो, ताकि उर्दू पर एक मजहब विशेष की भाषा होने के आरोप से मुक्ति मिल सके. और भविष्य में फिर कोई उर्दू का इस्तेमाल मुस्लिम सांप्रदायिकता भड़काने के लिए न कर सके.
अब वह उचित समय आ गया है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को किसी भी रंग-रूप में पनपने न दिया जाय. ताकि इस देश से साम्प्रदायिकता का समूल उन्मूलन हो सके और सभी धर्मों के लोग आपस में मिल-जुलकर सामाजिक समरसता एवं सौहार्द से जीवन यापन कर सकें.
(लेखक अनुवादक, स्तंभकार, मीडिया पैनलिस्ट, पसमांदा सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से चिकित्सक हैं.)
ये भी पढ़ें : दीपावली: उर्दू शायरों का पसंदीदा विषय
ये भी पढ़ें : क्या उर्दू, हिन्दी दो प्यारी बहनें हैं ?