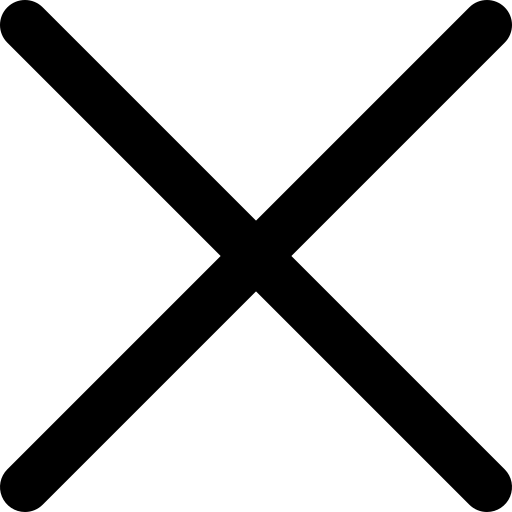.jpg)
दस्तावेज़/ ज़ाहिद ख़ान
अहमद नदीम क़ासमी एक हरफ़नमौला अदीब थे. उनके चाहे अफ़साने देख लीजिए, चाहे गज़ल़-नज़्में इनमें पंजाब की देहातों की सुंदर अक्कासी दिखलाई देती है.
उन्होंने शुरुआत में रूमानी ग़ज़लें लिखीं, लेकिन बाद में ज़िंदगी की तल्ख़ सच्चाईयों को अपने अदब का मौजू़ बना लिया. उनकी शायरी जहां इंसानी दोस्ती का जज़्बा जगाती है, तो वहीं उसमें आने वाले कल की खू़बसूरत तस्वीर भी है.
अफ़साना-निगारी में वे प्रेमचंद के बाद एक बड़े अफ़साना-निगार के तौर पर उभरे. वहीं शायरी में उनका अहम कारनामा उर्दू अदब की रिवायत को क़ाइम रखते हुए, उसमें तरक़्क़ीपसंद नज़रिया लाना था. वे अपनी रिवायत और मिट्टी से हमेशा जुड़े रहे. उर्दू अदब की क़दीम रिवायत के अलावा उन्होंने जदीद ग़ज़ल को न सिर्फ़ अपनाया, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया.
अहमद नदीम क़ासमी ने हर अंदाज की नज़्में लिखीं. उनके अदबी सरमाये में एक से बढ़कर एक नज़्में हैं. अविभाजित भारत में पंजाब प्रांत के अंगह तहसील, जिला खोशाब में 20नवम्बर, 1916को एक सूफ़ी परिवार में पैदा हुए अहमद नदीम क़ासमी ने छोटी उम्र से ही शे’र कहना शुरू कर दिया था.
अल्लामा इक़बाल, अल्लामा शिबली, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, जोश मलीहाबादी के अदबी कारनामों ने उन्हें काफ़ी मुतास्सिर किया. अहमद नदीम क़ासमी ने आगे चलकर ग़ज़लें, नज़्में लिखना शुरू कर दीं. उनकी ये रचनाएं मुख़्तलिफ़ रिसालों में शाया होने लगीं.
ग़ज़ल-नज़्म लिखते-लिखते उनकी दिलचस्पी अफ़साने में भी पैदा हुई. उनका पहला अफ़साना ‘बुत तराश’ साल 1934में उस ज़माने के मशहूर रिसाले ‘हुमायूं’ में शाया हुआ. ये अफ़साना काफ़ी पसंद किया गया.
सआदत हसन मंटो भी इस अफ़साने की तारीफ़ करने से अपने आप को नहीं रोक पाए. एक-दूसरे के अदब के जानिब यह एहतिराम और तारीफ़ का जज़्बा आगे चलकर दोस्ती में तब्दील हो गया. यह दोस्ती, मंटो की मौत तक बरकरार रही.
अफ़साना निगारी में मिली इस कामयाबी के बाद अहमद नदीम क़ासमी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. थोड़े से ही अरसे में अहमद नदीम क़ासमी की पहचान तरक़्क़ीपसंद अफ़साना निगार के तौर पर बन गई. वे सआदत हसन मंटो, राजिंदर सिंह बेदी और कृश्न चंदर की सफ़ में खड़े हो गए. उनकी शुरुआती अफ़सानों में रूमानियत दिखलाई देती है. एक अलग तरह का रोमांटिसिज्म है.
अपने बगावती तेवर और समझौताविहीन राजनीति के चलते अहमद नदीम क़ासमी को कई मर्तबा ज़ेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने इंक़लाबी तेवर नहीं बदले. मुल्क के बंटवारे के बाद अहमद नदीम क़ासमी पाकिस्तान में ही रहे.
साल 1948में लाहौर से उन्होंने ‘नुकूश’ निकाला. आज़ाद मुल्क में भी अहमद नदीम क़ासमी की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुईं. वामपंथी ख़याल के चलते साल 1951में पाकिस्तानी हुक़ूमत ने उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद कर दिया. लेकिन हुक़ूमत का ज़ोर-ओ-जु़ल्म और टेढ़ी निग़ाह भी उनकी कलम को रोक नहीं पाई. कभी अदब तो कभी सहाफ़त के ज़रिए वे अपना काम, उसी मुस्तैदी से करते रहे.
सहाफ़त में अहमद नदीम क़ासमी की शुरुआत कॉलम निगारी से हुई थी, कुछ अरसे के बाद ही उन्हें ‘इमरोज’ की इदारत मिल गई. उन्होंने छह साल तक इस अख़बार का कामयाबी से संपादन किया. अपने अख़बार में वे पाकिस्तानी हुक़ूमत की बेख़ौफ होकर सख़्त तन्क़ीद किया करते थे. बाद में वे दीगर अख़बारों से भी कॉलम निगार की हैसियत से जुड़े रहे.
अहमद नदीम क़ासमी ने अदबी रिसाले ‘अदब-ए-लतीफ़’, ‘सबेरा’, ‘नुकूश’ और ‘फ़नून’ की एडीटिंग भी की. अपने इन अख़बारों और पत्रिकाओं से उन्होंने अदब को कई बेहतरीन अदीब दिए. उनकी रहनुमाई की. उर्दू अदब में अहमद नदीम क़ासमी का यह एक बड़ा कारनामा है, जिसे फ़रामोश नहीं किया जा सकता.
अहमद नदीम क़ासमी के अफ़सानों का पहला मजमुआ साल 1939में, तो ग़ज़लों-नज़्मों का पहला मजमुआ साल 1942में प्रकाशित हुआ. उनके ज़्यादातर अफ़साने देहात के मौज़ू और किरदारों पर मब्नी हैं. प्रेमचंद ने जहां अपने अदब में उत्तर प्रदेश के ग्राम्य जीवन, किसानों के दुःख-दर्द, आशा-निराशा, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न को विषय बनाया, तो अहमद नदीम क़ासमी भी पंजाब के किसानों के दुःख-दर्द को अपनी आवाज़ देते रहे.
अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद और सामंतवादी निज़ाम में किसानों का किस तरह से शोषण हो रहा है ?, उन्होंने इसे अपने अफ़सानों के ज़रिए बतलाया. भारत-पाक बंटवारे का खूनी मंज़र और दूसरी आलमी जंग में फ़ौजियों के परिवारों की दुर्दशा अहमद नदीम क़ासमी ने अपनी आंखों से देखी थी. लिहाज़ा इन मसलों को जब उन्होंने अपनी कहानियों का मौज़ू बनाया, तो एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज अफ़साने सामने निकलकर आए.
यही नहीं हिंदुस्तान से अलग हुए नये मुल्क पाकिस्तान में मुहाजिरों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, इसे मौजू़ बनाकर भी उन्होंने कई बेहतरीन कहानियां लिखीं. ‘अलहम्द-लिल्लाह’, ‘गंडासा’, ‘परमेश्वर सिंह’, ‘हिरोशिमा के पहले और बाद’ उनकी बेमिसाल कहानियां हैं. अफ़साना ‘हिरोशिमा के पहले और बाद’ जंग के ख़िलाफ़ लिखा उनका एक अज़ीमतरीन दस्तावेज है.
अफ़साने के बैकग्राउंड में दूसरी आलमी जंग के हालात हैं.‘‘भूख भी तो जंग होती है, गुलामी की भी जंग होती है, इंतिज़ार की भी एक जंग होती है, जंग हर जगह हो रही है, रंगून में भी हो रही है, हमारे गांव में भी हो रही है, यह नित्य और अनादिकालीन जंग.’’
अहमद नदीम क़ासमी ने बंटवारे, इक़्तिसादी मसाइल पर बहुत अच्छी कहानियां लिखीं. बंटवारे पर ‘परमेशर सिंह’ उनका बेहतरीन अफ़साना है. बंटवारे के पसमंज़र में जब सरहद के इस तरफ और उस तरफ लोग एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे हैं. ऐसे माहौल में भी परमेशर सिंह इंसानियत का दामन नहीं छोड़ता. अपनी जान की परवाह किए बिना, वह उस बच्चे को पाकिस्तान की सीमा में छोड़ने जाता है, जो बंटवारे की भगदड़ में अपने परिवार से बिछड़ कर, हिंदुस्तान जा पहुंचता है. परमेशर सिंह को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है.
दूसरी आलमी जंग का दुनिया के कई हिस्सों में असर पड़ा. ख़ास तौर पर भारत पर. हज़ारों हिंदुस्तानी इस जंग में मारे गए और उनके परिवार तबाह हो गए. अहमद नदीम क़ासमी उर्दू अदब में अकेले ऐसे अफ़साना निगार हैं, जिन्होंने इस मौज़ू पर अनेक संवेदनशील कहानियां लिखीं. ‘सिपाही बेटा’, ‘बाबा नूर’, ‘आतिशे गुल’ और ‘ममता’ वगैरह जंग के बाद इंसान की ज़िंदगी में आई अनेक तरह की जंग के बेजोड़ अफ़साने हैं.
अहमद नदीम क़ासमी जितने आला अफ़साना निगार थे, उतने ही बेहतरीन शायर भी थे. शायरी में भी उनका कोई जवाब नहीं. अहमद नदीम क़ासमी इंसान दोस्त शायर थे. उनकी शायरी में इंसानियत और भाईचारे का पैग़ाम है.‘‘दावरे-हश्र ! मुझे तेरी कसम/उम्र भर मैंने इबादत की है/तू मेरा नामा-ए-आमाल तो देख/मैंने इंसां से मुहब्बत की है.’’
वहीं नज्म ‘रज्अत परस्ती का नारा’ की शुरुआती लाइनें अहमद नदीम क़ासमी की शायरी के अंदाज़, उनके शालीन लहज़े और सोच की बेहतरीन मिसाल है, ‘‘अंधियारे में रहने वालो, अंधियारे के राज न खोलो/कांच से सपने टूट न जाएं, आहिस्ता-आहिस्ता बोलो .’’
अहमद नदीम क़ासमी गुलाम मुल्क में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम को बराबर बेदार करते रहे. शायरी में कभी मुख़र होकर, तो कभी इशारों में उन्होंने अपनी बात कही. ‘‘हुक्मरानों ने उकावों का भरा है बहु रूप/भोली चिड़ियों को जगाना भी तो फ़नकारी है/खेत आबाद हैं, देहात हैं उजड़े-उजड़े/इस तफ़ाबुत को मिटाना भी तो फ़नकारी है .’’
मुल्क का बंटवारा एक बड़ी ट्रेजडी थी. जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए. फ़िरक़ावाराना दंगों में हज़ारों लोग मारे गए. इंसानियत और सदियों का भाईचारा शर्मसार हुआ. पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में जब फ़िरक़ावाराना दंगे फैले, तो अहमद नदीम क़ासमी ख़ामोश तमाशाई नहीं बने रहे. उन्होंने अपनी नज़्मों में इंसानियत मुख़ालिफ़ इन वहशी हरकतों की सख़्त मज़म्मत की.
नज़्म ‘आज़ादी के बाद’ में उनका दर्द कुछ इस तरह से ज़बान पर आया, ‘‘रोटियां बोटियों से तुलती हैं इस्मतों से सजी दुकानों पर/पेट भरने के बाद नाचता है ख़ून का जायका ज़बानों पर.’’
अहमद नदीम क़ासमी ने ग़ज़ल और नज़्म दोनों ही अधिकार के साथ लिखीं. उनकी ग़ज़लें अपने ज़माने में तो मशहूर हुईं, आज भी ये ग़ज़ल उसी तरह पसंद की जाती हैं.
अहमद नदीम कासमी की ग़ज़ल की मक़बूलियत के पीछे सादा अंदाज़ था. बिना किसी भारी भरकम अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किए बिना, वे ऐसी बातें कह जाते थे, जो सीधे दिल में उतर जाती हैं. ‘‘कौन कहता है, मौत आएगी तो मर जाऊंगा/मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा.’’
अहमद नदीम क़ासमी ने बेशुमार लिखा. नज़्म, ग़ज़ल, रुबाई, कतआ, अफ़साने, ड्रामें, मजाहिया कॉलम और सैकड़ों मज़ामीन. उनकी किताबों की तादाद तकरीबन पचास के आस-पास होगी. ‘चौपाल’, ‘बगोले’, ‘तुलू व गुरुब’, ‘सैलाब’, ‘गरदाब’, ‘आंचल’, ‘आसपास’, ‘कपास के फूल’, ‘दरो-दीवारी’, ‘सन्नाटा’, ‘बाजारे हयात’, ‘बर्गे हिना’, ‘घर से घर तक’, ‘नीला पत्थर’, ‘कोहे पैमा’, ‘पतझड़’ समेत उनके अफ़सानों की सतरह किताबें और ग़ज़लों-नज़्मों की ‘रिमझिम’, ‘धड़कनें’ ‘जलाल-ओ-जमाल’, ‘शोला-ए-गुल’, ‘दश्ते वफ़ा’, ‘अर्ज-ओ-समा’, ‘लौह ख़ाक’ समेत आठ किताबें शाया हुई हैं.
अहमद नदीम क़ासमी की कहानियों और शायरी के तजुर्मे देशी ज़बानों हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, सिंधी के अलावा दुनिया भर की ज़बानों अंग्रेज़ी, रूसी, चीनी, जापानी वगैरह में भी हुए हैं. पाकिस्तान के शिखर सम्मान ‘इम्तियाज़े पाकिस्तान’ के अलावा उन्हें तमाम अदबी सम्मानों से नवाज़ा गया.
10जुलाई, साल 2006को लाहौर में नब्बे साल की उम्र में अहमद नदीम क़ासमी ने यह कहकर, इस जहान-ए-फ़ानी से अपनी आखिरी रुख़्सती ली,‘‘ज़िंदगी शम्अ की मानिंद जलाता हूँ ‘नदीम’/बुझ तो जाऊँगा मगर सुबह तो कर जाऊँगा.’’