1990 के दशक की शुरुआत में, जब दहेज और भव्य विवाहों को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक माना जाता था, एक धारणा जो दुर्भाग्यवश आज भी सामाजिक स्थिति के मापदंड के रूप में विद्यमान है, मेरे दिवंगत पिता, अब्दुल मजीद अदीब अंसारी, और उनके कुछ सामाजिक रूप से जागरूक साथियों ने एक असहज लेकिन आवश्यक सवाल उठाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद कमिश्नरेट में पासमंडा मुसलमानों के बीच प्रचलित दहेज, दिखावटी शादियों और आर्थिक शोषण जैसे गहरे नकारात्मक सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी। यह पहल एक भावनात्मक नारे या क्षणिक जोश की नहीं थी; बल्कि यह एक सुविचारित सामाजिक हस्तक्षेप था, जो नैतिकता और इस्लामी चेतना पर आधारित था।
उनका उद्देश्य क्रांति नहीं, बल्कि सुधार था। वे विवाह को इसके मूल इस्लामी स्वरूप में पुनः स्थापित करना चाहते थे, जहां निकाह जिम्मेदारी और समानता का समझौता हो, न कि एक सौदाबाजी की जगह; जहां एक बेटी को बोझ न समझा जाए और एक पिता पर कर्ज का भारी दबाव न हो; जहां विवाह खुशी का स्रोत हो, न कि डर का। इस्लाम स्पष्ट रूप से दुल्हन के परिवार से उपहार या संपत्ति की मांग को हतोत्साहित करता है, इसे न्याय और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों के खिलाफ मानता है। इसके बजाय, कुरान और हदीस में महर की व्यवस्था की जाती है, जो एक अनिवार्य उपहार होता है जो दूल्हा अपनी दुल्हन को देता है, और यह महिला के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है। पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने सरल शादियों को बढ़ावा दिया और कहा कि सबसे अच्छा निकाह वही है जो सबसे आसान, सीधा और बिना किसी अनावश्यक बोझ और extravagance के हो।
गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ने इस पहल को तुरंत स्वीकार किया। उनके लिए यह कोई विचारधात्मक बहस नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की वास्तविकता में राहत थी। उन परिवारों के लिए जिनके लिए बेटी की शादी एक चिंता, अपमान और जीवनभर के कर्ज से जुड़ी हुई थी, यह पहल एक सम्मान की राह के रूप में सामने आई। यह आंदोलन गरीबों में सफल हुआ, क्योंकि यह सीधे उनके दैनिक संघर्षों से जुड़ा था।
लेकिन जैसे ही यह सवाल संपन्न वर्ग तक पहुंचा, सुधार की गति धीमी हो गई। जिनके पास संपत्ति, प्रभाव और सामाजिक प्रभुत्व था, वे सुधार की भाषा बोलने लगे, लेकिन जैसे ही यह उनके आराम, उनके सामाजिक प्रदर्शन और उनके विशेषाधिकारों को खतरे में डालने लगा, वे पीछे हट गए। सुधार तब तक स्वीकार्य था जब तक यह दूसरों पर लागू होता था, स्वयं पर नहीं। यह आंदोलन विचारधारात्मक कमजोरी के कारण असफल नहीं हुआ; बल्कि यह असफल हुआ क्योंकि जिनके पास संसाधन थे, उनमें नैतिक साहस की कमी थी। मेरे पिता अपने समय से बहुत आगे थे क्योंकि उन्होंने समाज को जैसा था वैसा नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसे जैसा होना चाहिए था, वैसे देखने का चुनाव किया।
समय बीतता गया, पीढ़ियाँ बदल गईं, और ऐसा लगा जैसे समाज ने कुछ सीखा हो। फिर भी भारतीय संस्कृति में, समुदायों के बीच शादियाँ, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, लंबे समय से भव्य उत्सवों के रूप में जानी जाती हैं, जो आतिथ्य, परिवार की इज्जत और सामाजिक प्रदर्शन की परंपराओं से आकारित होती हैं। भव्य समारोह, elaborate भोज, और उपहारों का आदान-प्रदान, प्रतिष्ठा के विचारों से गहरे जुड़ गए हैं, जो प्रायः प्राचीन रीति-रिवाजों और आधुनिक उपभोक्तावाद के मिश्रण के रूप में होते हैं। भारतीय मुसलमानों के बीच, इसने दहेज प्रथा को भी बनाए रखा है, जो दुल्हन के परिवार से उपहार के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो अक्सर स्वेच्छा से होते हैं लेकिन वास्तव में दहेज की तरह काम करते हैं, परिवारों पर भारी दबाव डालते हैं और इस्लामी शिक्षाओं के स्पष्ट विपरीत होते हैं।
हाल ही में, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जमात-उल-कोरेश द्वारा दहेज उन्मूलन और साधारण शादियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। मंच से दिए गए भाषण प्रभावशाली थे। कार्यालयधारियों ने एकमत से घोषणा की कि जो भी इन सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा, उसे न केवल निंदा किया जाएगा, बल्कि ऐसी शादियों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समुदाय ने वास्तव में आत्मचिंतन के लिए साहस जुटाया हो।
लेकिन इतिहास हमें बार-बार सिखाता है कि घोषणाएँ करना आसान है, जबकि बलिदान करना कठिन है।
इसी संदर्भ में, जमात-उल-कोरेश के अध्यक्ष ने मुझे उनके भतीजे की शादी की रिसेप्शन में आमंत्रित किया। उस दिन मैं शहर से बाहर था और मैंने अपने नहीं आने की सूचना शिष्टता से दी। जो बाद में सामने आया, वह सिर्फ निराशाजनक नहीं था, बल्कि गहरे अस्वस्थ करने वाला था। उस रिसेप्शन में कई राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया, जिनकी उपस्थिति में उन सिद्धांतों को बढ़ावा देने की शपथ ली गई थी, जो पहले बैठक में साधारण शादियों और दहेज का विरोध करने पर केंद्रित थे। विडंबना बिल्कुल स्पष्ट थी। जिस सम्मेलन में उन सिद्धांतों की निंदा की गई थी, उसी आयोजन में उन्हीं सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। वही शानो-शौकत, वही भव्यता और वही सामाजिक प्रदर्शन, जिसे मंच से नकारा गया था, पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि यह शादी उसी आईआईसीसी परिसर में हुई, जहां जमात-उल-कोरेश ने सामाजिक बुराइयों और साधारण शादियों के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किया था।
यह कोई विरोधाभास नहीं है; यह संस्थागत ढोंग है।
हम गरीबों से सादगी अपनाने की अपील करते हैं, जबकि चुपचाप संपन्नों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। हम बार-बार नैतिकता का बोझ कमजोर कंधों पर डालते हैं और सत्ता के सामने चुप रहते हैं। इस तरह के दोहरे मानक केवल सुधार को कमजोर नहीं करते, बल्कि इसे पूरी तरह से नैतिक वैधता से ही лишित कर देते हैं। ऐसा नेतृत्व जो अपने घोषित सिद्धांतों को निजी जीवन में लागू नहीं कर सकता, वह नेतृत्व नहीं, बल्कि प्रदर्शन है। जो लोग अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं करते, वे किसी भी नैतिक दावे के हकदार नहीं हो सकते।
यदि हम वास्तव में सादगी और इस्लामी मूल्यों में विश्वास करते हैं, तो विवाह की पूरी संरचना बदलनी चाहिए। इसका मतलब है एक साधारण निकाह, एक संयमित वलीमा और दहेज तथा फिजूल दिखावे का पूरी तरह से विरोध। वलीमा, जैसा कि सुन्नत में बताया गया है, दूल्हे के परिवार द्वारा एक साधारण भोज होता है, जो खुशी के साथ विवाह की घोषणा करता है, न कि संपत्ति या प्रभाव का प्रदर्शन। भारतीय संदर्भ में, जहां सांस्कृतिक दबाव भव्यता को बढ़ाता है, संसाधनों को सामुदायिक कल्याण की दिशा में पुनर्निर्देशित करना इस्लामी ज़कात सिद्धांतों और सामाजिक भलाई के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
अत्यधिक खर्च से बचाया गया धन दुल्हन की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए या सामूहिक कल्याण में निवेश किया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, छात्रवृत्तियाँ और सामाजिक सहायता शामिल हैं। यहीं से उपदेश नीति में बदलते हैं और नैतिक आग्रह जीवन में अभ्यास में परिणत होते हैं।
बांद्रा, मुंबई में अमरोहा कुरेशियों द्वारा आयोजित एक सामूहिक विवाह इस दृष्टिकोण का एक जीवित उदाहरण है। वहाँ कोई मंच नहीं था, कोई संपत्ति का प्रदर्शन नहीं था, केवल गरिमा, समानता और सामूहिक जिम्मेदारी थी। इसने यह दिखाया कि सुधार केवल प्रभावशाली भाषणों से नहीं, बल्कि सचेत निर्णयों से आता है।
असल सवाल यह नहीं है कि दहेज और भव्य शादियाँ अन्यायपूर्ण या इस्लामिक हैं या नहीं। हम पहले ही जानते हैं कि ये हैं। असल सवाल यह है कि क्या हम सत्य की सेवा में अपने आपको असुविधा देने के लिए नैतिक अनुशासन रखते हैं। जब तक हम उस साहस को नहीं जुटाते, तब तक हमारे भाषण हमारे कार्यों से जोर से आवाज़ करेंगे, हमारे संकल्प हमारी इच्छाओं से कमजोर होंगे, और हमारे सुधार आंदोलनों में कुछ भी ठोस नहीं होगा, केवल छल-प्रपंच होगा, जो सुंदर भाषा में लिपटा होगा।
सच्चा सुधार तब शुरू होता है जब हम उन नियमों को खुद पर लागू करने के लिए तैयार होते हैं, जो हम दूसरों के लिए निर्धारित करते हैं, जो इस्लामी मूल्यों की सादगी, समानता और जवाबदेही पर आधारित होते हैं, यहाँ तक कि भारत की जीवंत और चुनौतीपूर्ण सांस्कृतिक वास्तविकताओं में भी।












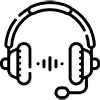

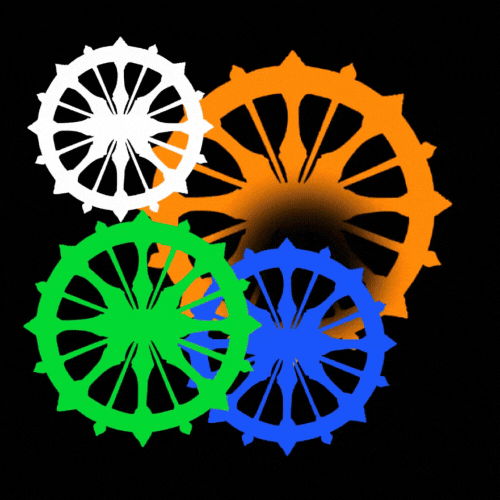
.jpg)

.jpg)




.webp)
.png)




_(1).jpg)
