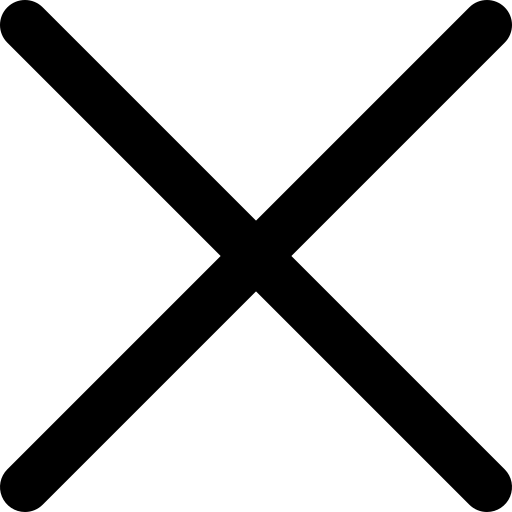इस्लामाबाद. बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए न सुलझने वाली गुत्थी बनता जा रहा है. प्रांत में अलगववादी चरमपंथियों की कार्रवाईयों ने सरकार को हिला कर रख दिया है. इस प्रदेश में बढ़ती हिंसा न सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी पाकिस्तान को बड़ा जख्म दे सकती है. चीन ने यहा बड़े पैमाने पर निवेश किया है लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि हाल की हिंसक घटनाओं के बाद क्या बीजिंग अपने कदम पीछे खींच सकता है.
पाकिस्तान के भूमि क्षेत्र का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान का है. यह अफगानिस्तान और ईरान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है.
इस प्रांत केवल 5% कृषि योग्य है. यह अत्यंत शुष्क रेगिस्तानी जलवायु के लिए जाना जाता है लेकिन इसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर माना जाता है. इसके बावजूद विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है.
इस प्रांत में तांबा, सोना, कोयला और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, जो पाकिस्तान की खनिज संपदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया को जोड़ने वाली अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण, बलूचिस्तान न एक भू-राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहमियत रखता है.
बलूचिस्तान की भू-रणनीतिक अहमियत के कारण चीन की मत्वकांक्षी परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) का एक बड़ा हिस्सा इसी प्रांत में है. सीपीईसी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 'बेल्ट एंड रोड' पहल का हिस्सा है और ग्वादर शहर का बंदरगाह इस प्रोजेक्ट के लिए बेहद अहम मान जाता है. यह एक परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के अरब सागर तट के माध्यम से चीन को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है.
अरब सागर पर स्थित ग्वादर बंदरगाह इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख व्यापार द्वार साबित हो सकता है. हालांकि बड़ी संख्या में बलूच लोग यह मानते हैं कि ये निवेश बाहरी शोषण का एक रूप है. पाकिस्तानी सरकार सीपीईस को गेम-चेंजर के रूप में पेश करती है लेकिन स्थानीय लोगों की दलील है कि इन विशाल परियोजनाओं से बहुत कम लाभ होता है.
चीनी कंपनियों और श्रमिकों की आमद ने स्थानीय लोगों की नाराजगी को और गहरा कर दिया है क्योंकि वे बेरोजगारी और अपर्याप्त सामाजिक सेवाओं से जूझ रहे हैं.
वैसे बलूचिस्तान के शोषण का मुद्दा काफी पुराना है. स्थानीय लोग दशकों से आरोप लगाते रहे हैं कि प्रांतीय और केंद्र सरकारें यहां के प्राकृतिक संसाधनों को दोहन का भारी मुनाफा कमाती रही हैं लेकिन इलाके में विकास को पूरी तरह उपेक्षा की जाती रही है. प्रांत में बलूच राष्ट्रवादियों ने आजादी के लिए 1948-50, 1958-60, 1962-63 और 1973-1977 में विद्रोह किए हैं.
बलूचिस्तान में कई अलगाववादी समूह सक्रिए हैं जिनमें से बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) सबसे बड़ी चुनौती बन कर उभरा है. पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस को किडनैप कर इस समूह ने अपनी ताकत जता दी है.
चीन के लिए, सीपीईसी की कामयाबी बलूचिस्तान में स्थिरता पर निर्भर करती है. हालांकि, अलगाववादी समूहों का निरंतर प्रतिरोध इसके निवेश के लिए एक गंभीर चुनौती है. यदि संघर्ष आगे बढ़ता है, तो यह क्षेत्र में बीजिंग की महत्वकांक्षाओं को खतरे में डाल सकता है.
पाकिस्तान में सीपीईसी परियोजनाओं में वर्तमान में लगभग 30,000 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं. बीजिंग के लिए अपने नगारिकों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल खासतौर से बलूचिस्तान में. बलूच विद्रोही पाकिस्तान से आजादी की मांग करने के अलावा, इस क्षेत्र में चीनी परियोजनाओं का भी मुखर विरोध करते रहे हैं.
कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन प्रांत में अपनी सेना तैनात करने की मंशा रखता है हालांकि पाकिस्तान इसके लिए तैयार होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता है. लेकिन इन अटकलों ने इतना तो बता दिया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच अविश्वास की दरारें गहरी होती जा रही है. अगर पाकिस्तान ने चीन की सुरक्षा चिंताओं को दूर नहीं किया तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा.