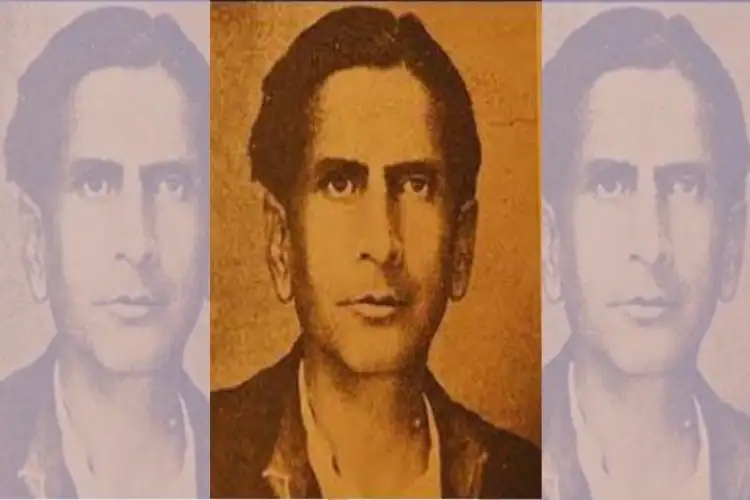
ज़ाहिद ख़ान
शे'र-ओ-अदब की महफ़िल में जब भी ग़ज़लों-नज़्मों का ज़िक्र छिड़ता है, मजाज़ लखनवी का नाम ज़रूर आता है. उनके समूचे कलाम में दिलों के अंदर उतर जाने की जो कैफ़ियत है, वह बहुत कम लोगों को नसीब हुई है. मजाज़ की ख़ूबसूरत, पुर-सोज़ शायरी के पहले भी सभी दीवाने थे और उनकी मौत के इतने सालों बाद भी यह दीवानगी जरा सी कम नहीं हुई है.
फ़िराक़ गोरखपुरी की नज़र में, ‘‘अल्फ़ाज़ों के इंतिख़ाब और संप्रेषण के लिहाज़ से मजाज़, फै़ज़ के बजाय ज़्यादा ताक़तवर शायर थे.’’ एक दौर था, जब मजाज़ उर्दू अदब में आंधी की तरह छा गए थे. आलम यह था कि जब वे अपनी कोई नज़्म लिखते, तो वह प्रगतिशील रचनाशीलता की एक बड़ी परिघटना होती.
लोग उस नज़्म पर महीनों चर्चा करते. मजाज़ जिस दौर में लिख रहे थे, उस दौर में फै़ज़ अहमद फ़ै़ज़, अली सरदार जाफ़री, मख़्दूम, जज़्बी आदि भी अपनी शायरी से पूरे मुल्क में धूम मचाए हुए थे. लेकिन वे इन शायरों में सबसे ज़्यादा मक़बूल और दिलपसंद थे. मजाज़ की ग़ैर मामूली शोहरत के बारे में मशहूर अफ़साना निगार इस्मत चुग़ताई ने लिखा है, ‘‘जब उनकी क़िताब ‘आहंग’ प्रकाशित हुई, तो गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां इसे अपने सरहाने तकियों में छिपाकर रखतीं और आपस में बैठकर पर्चियां निकालती थीं कि हम में से किसको मजाज़ अपनी दुल्हन बनाएगा.’’
मजाज़ की ज़िंदगानी में उनकी नज़्मों का सिर्फ़ एक मजमूआ ‘आहंग’ (साल 1938) छपा, जो बाद में ‘शबाताब’ और ‘साज—ए-नौ’ के नाम से भी शाए हुआ. ‘आहंग’ में मजाज़ की तक़रीबन 60नज़्में शामिल हैं और सभी नज़्में एक से बढ़कर एक. ‘‘मुझ से मत पूछ ’’मिरे हुस्न में क्या रक्खा है’’/आँख से पर्दा-ए-ज़ुल्मात उठा रक्खा है/.....मुझ से मत पूछ ’’तिरे इश्क़ में क्या रक्खा है’’/सोज़ को साज़ के पर्दे में छुपा रक्खा है.’’
लखनऊ के एक पुराने कस्बे रुदौली में 19अक्टूबर, 1911को असरार-उल-हक़ यानी मजाज़ की पैदाइश हुई. उनकी शुरुआती तालीम लखनऊ में ही हुई. उसके बाद उन्होंने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया. आगरा में उस्ताद शायर फ़ानी बदायुनी, अहसन मारहरवी और मयकश अकबराबादी की शायराना संगत मिली. या यूं कहें इन उस्ताद शायरों की शार्गिदी में वे शायरी का हुनर सीखे. मजाज़ ने अपनी इब्तिदाई शायरी में उनसे ज़रूरी इस्लाह ली.
सच बात तो यह है कि फ़ानी बदायुनी ने ही उन्हें ‘मजाज़’ का तख़ल्लुस दिया. कॉलेज में जज़्बी और आले अहमद सुरूर उनके दोस्त थे. ज़ाहिर है इस माहौल में मजाज़ के अंदर भी शायरी की ज़ानिब मोहब्बत जागी. अदबी महफ़िलों में शिरकत करने के साथ-साथ वे भी शे’रगोई करने लगे.
दीगर शायरों की तरह मजाज़ की शायराना ज़िंदगी की इब्तिदा, ग़ज़लगोई से हुई. शुरुआत भी लाजवाब, ‘‘तस्कीन-ए-दिल-ए-महज़ूँ न हुई वो सई-ए-करम फ़रमा भी गए/इस सई-ए-करम को क्या कहिए बहला भी गए तड़पा भी गए/इस महफ़िल-ए-कैफ़-ओ-मस्ती में इस अंजुमन-ए-इरफ़ानी में/सब जाम-ब-कफ़ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए.’’
लेकिन चंद ही ग़ज़लें कहने के बाद, मजाज़ नज़्म के मैदान में आ गए. आगे चलकर नज़्मों को ही उन्होंने अपने राजनीतिक सरोकारों की अभिव्यक्ति का वसीला बनाया. अलबत्ता बीच-बीच में वे ज़रूर ग़ज़ल लिखते रहे. ‘‘कुछ तुझ को ख़बर है हम क्या क्या ऐ शोरिश-ए-दौराँ भूल गए/वो ज़ुल्फ़-ए-परेशाँ भूल गए, वो दीदा-ए-गिर्यां भूल गए.’’
अपनी शायरी से थोड़े से ही अरसे में मजाज़ नौजवानों दिलों की धड़कन बन गए. उनके शे’र, हर एक की ज़बान पर आ गए. ऐसे ही उनके ना भुलाए जाने वाले कुछ मशहूर शे’र हैं, ‘‘जो हो सके, हमें पामाल करके आगे बढ़/न हो सके, तो हमारा जवाब पैदा कर.’’, ‘‘सब का मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर न सके/सबके तो ग़रीबां सी डाले अपना ही ग़िरेबां भूल गए.’’
‘आवारा’ वह नज़्म है, जिसने मजाज़ को एक नई पहचान दी. मजाज़ का दौर मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद का दौर था. बरतानवी हुकूमत की साम्राज्यवादी नीतियों और सामंतवादी निज़ाम से मुल्क में रहने वाला हर बाशिंदा परेशान था. ‘आवारा’ पूरी एक नस्ल की बेचैनी की नज़्म बन गई. नौजवानों को लगा कि कोई तो है, जिसने अपनी नज़्म में उनके ख़यालात की अक्कासी की है.
‘आवारा’ नज़्म पर यदि ग़ौर करें, तो इस नज़्म की इमेजरी और काव्यात्मकता दोनों रूमानी है, लेकिन उसमें एहतिजाज और बग़ावत के सुर भी हैं. यही वजह है कि वे नौजवानों की पंसदीदा नज़्म बन गई. आज भी यह नज़्म नौजवानों को अपनी ओर उसी तरह आकर्षित करती है. ‘‘शहर की रात और मैं नाशाद—ओ-नाकारा फिरूं/जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं/गै़र की बस्ती है कब तक दर-ब-दर मारा फिरूं/ए-ग़मे-दिल क्या करूं ऐ वहशत—ए-दिल क्या करूं.’’
‘आवारा’ पर उस दौर की नई पीढ़ी ही अकेले फ़िदा नहीं थी, मजाज़ के साथी शायर भी इस नज़्म की तारीफ़ करने से अपने आप को नहीं रोक पाए. उनके जिगरी दोस्त अली सरदार जाफ़री ने लिखा है, ‘‘यह नज़्म नौजवानों का ऐलान—नामा थी और आवारा का किरदार उर्दू शायरी में बग़ावत और आज़ादी का पैकर बनकर उभर आया है.’’ इस नज़्म के अलावा मजाज़ की ‘शहर—ए-निग़ार’, ‘एतिराफ़’ वगैरह नज़्मों का भी कोई जवाब नहीं.
फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मजाज़ की ‘ख़्वाब—ए—सहर’ और ‘नौजवान ख़ातून से ख़िताब’ नज़्मों को सबसे मुक़म्मिल और सबसे कामयाब तरक़्क़ीपसंद नज़्मों में से एक मानते थे. फ़ैज़ की इस बात से फिर भला कौन नाइत्तेफ़ाकी जतला सकता है. ‘नौजवान ख़ातून से ख़िताब’ नज़्म, है भी वाक़ई ऐसी, ‘‘हिजाब-ए-फ़ित्ना-परवर अब उठा लेती तो अच्छा था/ख़ु़द अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था/....दिल-ए-मजरूह को मजरूह-तर करने से क्या हासिल/तू आँसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था/....तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही ख़ूब है लेकिन/तू इस आंचल से इक परचम बना लेती तो अच्छा था.’’
इस नज़्म में साफ़ दिखलाई देता है कि मजाज़ औरतों के हुक़ू़क़ के हामी थे और मर्द-औरत की बराबरी के पैरोकार. मर्द के मुक़ाबले वे औरत को कमतर नहीं समझते थे. उनकी निग़ाह में मर्दों के ही बराबर औरत का मर्तबा था. मजाज़ शाइर—ए-आतिश नफ़स थे, जिन्हें कुछ लोगों ने जानबूझकर रूमानी शायर तक ही महदूद कर दिया. यह बात सच है कि मजाज़ की शायरी में रूमानियत है, लेकिन जब उसमें इंक़लाबियत और बग़ावत का मेल हुआ, तो वह एक अलग ही तर्ज़ की शायरी हुई. ‘‘बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना/तिरी जुल्फ़ों का पेच—ओ-ख़म नहीं है/....ब-ईं सैल-ए-ग़म ओ सैल-ए-हवादिस/मिरा सर है कि अब भी ख़म नहीं है.’’
मजाज़ ने दीगर तरक़्क़ीपसंद शायरों की तरह ग़ज़लों की बजाए नज़्में ज़्यादा लिखीं. उन्होंने शायरी में मुहब्बत के गीत गाये, तो मज़दूर-किसानों के जज़्बात को भी अपनी आवाज़ दी. मजाज़ ने अपनी नज़्मों में दकियानूसियत, सियासी गुलामी, शोषण, साम्राज्यवादी, सरमायादारी और सामंतवादी निजाम, सियासी गुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई.
उनकी नज़्मों में हमें आज़ादख़याली, समानता और इंसानी हक़ की गूंज सुनाई देती है. ‘हमारा झंडा’, ‘इंक़लाब’, ‘सरमायेदारी’, ‘बोल अरी ओ धरती बोल’, ‘मज़दूरों का गीत’, ‘अंधेरी रात का मुसाफ़िर’, ‘नौजवान से’, ‘आहंगे-नौ’ वगैरह उनकी नज़्में इस बात की तस्दीक़ करती हैं. मजाज़ ने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की और रेडियो के रिसाले ‘आवाज़’ के सब एडीटर भी रहे. हार्डिंग लायब्रेरी में असिस्टेंट लायब्रेरियन के तौर पर काम किया. कुछ दिन मुंबई भी रहे, जहां उस वक़्त उनके कई दोस्त काम कर रहे थे, लेकिन वे कहीं टिककर नहीं रहे. साल 1936 में मजाज़ ने अपनी नायाब नज़्म ‘नज्र-ए-अलीगढ़’ लिखी.
किसी भी शायर के लिए इससे ज्यादा फ़ख्र की क्या बात होगी कि जिस यूनिवर्सिटी से वह पढ़कर निकला, उसी यूनिवर्सिटी का यह तराना, कुलगीत बन जाए. आज भी यह नज़्म यूनिवर्सिटी में गायी जाती है. ‘‘सरशार-ए-निगाह-ए-नर्गिस हूँ पा-बस्ता-ए-गेसू-ए-सुम्बुल हूँ/ये मेरा चमन है मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ.’’मजाज़ को बहुत कम उम्र मिली.
यदि उन्हें और उम्र मिलती, तो वे क्या हो सकते थे ?, इसके बारे में शायर-ए-इंक़लाब जोश मलीहाबादी ने अपनी आत्मकथा ‘यादों की बरात’ में लिखा है, ‘‘बेहद अफ़सोस है कि मैं यह लिखने को ज़िंदा हूं कि मजाज़ मर गया. यह कोई मुझसे पूछे कि मजाज़ क्या था और क्या हो सकता था. मरते वक़्त तक उसका महज़ एक चौथाई दिमाग़ ही खुलने पाया था और उसका सारा कलाम उस एक चौथाई खुले दिमाग़ की खुलावट का करिश्मा है. अगर वह बुढ़ापे की उम्र तक आता, तो अपने दौर का सबसे बड़ा शायर होता.’’
