

सबीहा फ़ातिमा बेग़म
कुछ कहानियाँ मनोरंजन के लिए नहीं होतीं। वे दर्शक को सहज महसूस कराने के बजाय बेचैन करती हैं, सवालों से घेरती हैं और फ़िल्म खत्म हो जाने के बाद भी मन में गूंजती रहती हैं। शाह बानो की कहानी ऐसी ही है। यह केवल एक कानूनी मुक़दमा नहीं था, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के लिए नैतिक आत्मपरीक्षा का क्षण था, जब भारत आस्था, क़ानून, राजनीति और मानवीय गरिमा के बीच खड़ा था। जब सिनेमा इस इतिहास को फिर से गढ़ता है, अदालत के तीखे संवादों, क़ुरआन की आयतों और एक बुज़ुर्ग औरत की पीड़ा के साथ, तो वह सिर्फ़ फ़िल्म नहीं रह जाता, बल्कि समाज को दिखाया गया एक आईना बन जाता है।
इस पूरी कथा के केंद्र में एक बेहद साधारण लेकिन झकझोर देने वाली सच्चाई है कभी-कभी न्याय क्रूरता से नहीं, बल्कि समझौते से मारा जाता है। फ़िल्म के संवाद पुराने घावों की तरह उभरते हैं, जो कभी पूरी तरह भरे ही नहीं। “कभी-कभी मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, हमें इज़्ज़त भी चाहिए।” यह एक पंक्ति शाह बानो के पूरे संघर्ष को समेट लेती है। वह धर्म के ख़िलाफ़ नहीं थीं। वह त्याग और अपमान के ख़िलाफ़ थीं।
चालीस वर्षों से अधिक समय तक विवाहित रहने के बाद, एक बुज़ुर्ग महिला को घर से निकाल दिया गया, तीन तलाक़ के ज़रिए रिश्ता तोड़ दिया गया और जीवनयापन के लिए न्यूनतम सहायता से भी वंचित कर दिया गया। शाह बानो की पीड़ा कोई असामान्य घटना नहीं थी; वह दुखद रूप से आम थी।
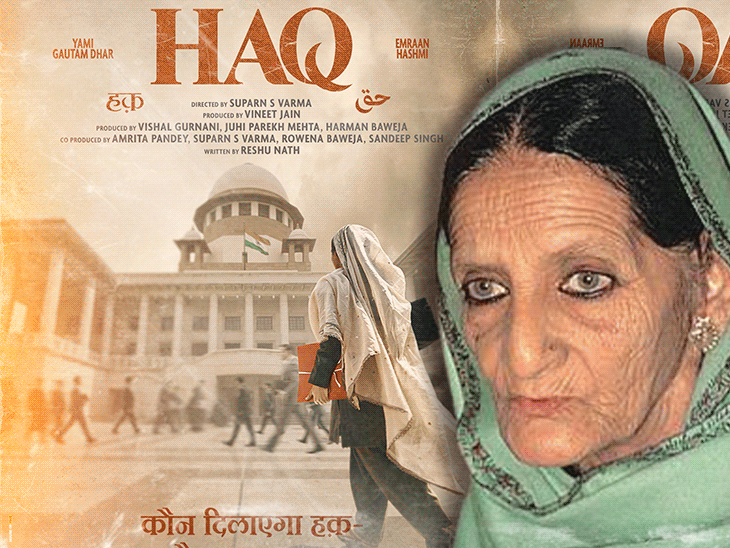
असाधारण यह था कि उन्होंने हार मानने के बजाय अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत केवल पाँच सौ रुपये मासिक गुज़ारे की मांग की। न वह किसी आंदोलन की नेता थीं, न किसी सुधार की प्रतीक। वह एक बूढ़ी, असहाय और भूखी औरत थीं, जो बस यह चाहती थीं कि उन्हें मरने के लिए अकेला न छोड़ दिया जाए।
लेकिन एक निजी याचना जल्द ही राष्ट्रीय बहस में बदल गई। फ़िल्म के अदालत वाले दृश्य, विशेषकर वे संवाद जो मुस्लिम पहचान की चिंता को स्वर देते हैं, उस गहरी असुरक्षा को उजागर करते हैं जो उस समय भारतीय मुसलमानों के भीतर मौजूद थी। जब कहा जाता है कि यह मुक़दमा केवल मेंटेनेंस का नहीं, बल्कि मुस्लिम पहचान का है, तो यह डर साफ़ झलकता है। डर पाँच सौ रुपये का नहीं था। डर यह था कि अगर यहाँ सेक्युलर क़ानून मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हावी हो सकता है, तो समुदाय की स्वायत्तता और विशिष्ट पहचान का क्या होगा।
विभाजन के बाद से ही भारतीय मुसलमानों को लगातार अपनी देशभक्ति और निष्ठा साबित करनी पड़ी थी, उस विभाजन के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे उन्होंने चुना ही नहीं था। ऐसे संवेदनशील माहौल में शाह बानो का फ़ैसला बहुतों को एक और छीना जाना लगा—पैसे का नहीं, बल्कि अधिकार और आत्मनिर्णय का। इसी कारण बहस जल्द ही कठोर खांचों में बंट गई—पर्सनल लॉ बनाम सेक्युलर लॉ, पहचान बनाम समानता, सामुदायिक अधिकार बनाम महिलाओं की आज़ादी।
लेकिन फ़िल्म और इतिहास दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि असली टकराव धर्म और न्याय के बीच नहीं था। यह टकराव सत्ता और असहायता के बीच था। क़ुरआन स्वयं कहता है कि तलाक़शुदा महिलाओं को इंसाफ़ के साथ गुज़ारा दिया जाना चाहिए। इस्लाम परित्याग की शिक्षा नहीं देता; वह करुणा और ज़िम्मेदारी की बात करता है। फिर भी, धार्मिक सिद्धांतों और सामाजिक व्यवहार के बीच कहीं न कहीं इंसानियत खो गई और उसकी जगह नियंत्रण और पितृसत्ता ने ले ली।
1985 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला, मोहम्मद अहमद ख़ान बनाम शाह बानो बेग़म, भारतीय न्यायिक इतिहास का एक साहसी क्षण था। अदालत ने साफ़ कहा कि किसी महिला का गरिमा के साथ जीने का अधिकार धार्मिक तकनीकीताओं पर निर्भर नहीं हो सकता। यह निर्णय इस्लाम विरोधी नहीं था; यह मनुष्यता के पक्ष में था। इससे पहले भी बाई ताहिरा और फ़ज़लुंबी जैसे मामलों में अदालत यह स्पष्ट कर चुकी थी कि केवल मामूली मेहर देकर कोई पति अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। न्यायपालिका वही कर रही थी जो क़ानून का मूल उद्देश्य होता है सबसे कमज़ोर की रक्षा करना।
लेकिन अदालत का न्याय हमेशा राजनीति के मैदान में जीवित नहीं रह पाता। 1986 में, राजीव गांधी सरकार ने रूढ़िवादी धार्मिक दबावों के आगे झुकते हुए मुस्लिम महिला (तलाक़ पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर दिया। इस क़ानून ने शाह बानो के फ़ैसले को लगभग निष्प्रभावी कर दिया और मेंटेनेंस को केवल इद्दत की अवधि तक सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, संसद ने वह छीन लिया। यह धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, बल्कि राजनीतिक सुविधा के आगे समर्पण था।
फ़िल्म इस विश्वासघात को बेहद मार्मिक ढंग से सामने रखती है। सेक्युलरिज़्म के नाम पर किए गए इस समझौते ने शाह बानो को वोट-बैंक की राजनीति का शिकार बना दिया। जिन नेताओं ने मुस्लिम पहचान की रक्षा का दावा किया, उन्होंने उसी पहचान की एक बुज़ुर्ग महिला की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे पीड़ादायक पक्ष न तो क़ानूनी है और न ही राजनीतिक, बल्कि व्यक्तिगत है।
जब पूरा देश उनके मुक़दमे पर बहस कर रहा था, शाह बानो अकेली थीं। उन्हें धमकियां मिलीं, सामाजिक दबाव झेलना पड़ा और उन पर यह आरोप लगाया गया कि वह इस्लाम को बदनाम कर रही हैं। उनसे केस वापस लेने को कहा गया। आख़िरकार, उन्होंने संघर्ष के बजाय ख़ामोशी को चुना। यह न्याय में अविश्वास का संकेत नहीं था, बल्कि वर्षों की थकान के बाद शांति की तलाश थी। उन्होंने कभी आंदोलन नहीं चाहा था। वह बस गरिमा के साथ जीना चाहती थीं। फिर भी, परिस्थितियों ने उन्हें एक आंदोलन का चेहरा बना दिया।
फ़िल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह एक कानूनी मिसाल के पीछे छिपे इंसान को फिर से सामने लाती है। अदालतों और बहसों के बीच कैमरा लगातार उस महिला को याद दिलाता है, जो इस पूरे विवाद के केंद्र में थी। वह कोई प्रतीक नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवित इंसान थी। जब फ़िल्म में कहा जाता है कि तलाक़ एक गाली बन चुका है, तो यह साफ़ हो जाता है कि हर वैचारिक बहस की कीमत किसी न किसी महिला को चुकानी पड़ती है। और जब निकाह को केवल अनुबंध नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी बताया जाता है, तो फ़िल्म यह सवाल उठाती है कि अगर आस्था कमज़ोरों की रक्षा नहीं कर सकती, तो वह किसकी रक्षा कर रही है।
2001 में, शाह बानो की मृत्यु के कई वर्षों बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के क़ानून की पुनर्व्याख्या की और यह स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाओं को जीवनभर के लिए न्यायसंगत और वाजिब गुज़ारा पाने का अधिकार है। क़ानून अंततः उनके पक्ष में लौटा, लेकिन वह इसे देखने के लिए जीवित नहीं थीं। यही इस कहानी की सबसे क्रूर विडंबना है।
यह फ़िल्म और शाह बानो की कथा केवल अतीत की बात नहीं है। यह आज के भारत से सीधे संवाद करती है, जहां समान नागरिक संहिता, धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों पर वही बहसें आज भी ज़िंदा हैं। इससे मिलने वाला सबक समय से परे है। किसी राष्ट्र की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि वह परंपराओं की रक्षा कितनी ज़ोर से करता है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमज़ोर नागरिकों की रक्षा कितनी ईमानदारी और संवेदनशीलता से करता है।
शाह बानो ने कभी क्रांति की मांग नहीं की। उन्होंने सिर्फ़ जीवन और गरिमा की मांग की। उन्होंने इस्लाम को चुनौती नहीं दी, उन्होंने अन्याय को चुनौती दी। और ऐसा करके उन्होंने भारत को उस सवाल से रूबरू कराया, जिससे वह आज भी जूझ रहा है—क्या कोई समाज नैतिक महानता का दावा कर सकता है, अगर वह पहचान की रक्षा के नाम पर महिलाओं की क़ुर्बानी देता रहे? यही सवाल, और इसी सवाल को उठाने का साहस, शाह बानो की सबसे बड़ी विरासत है।
