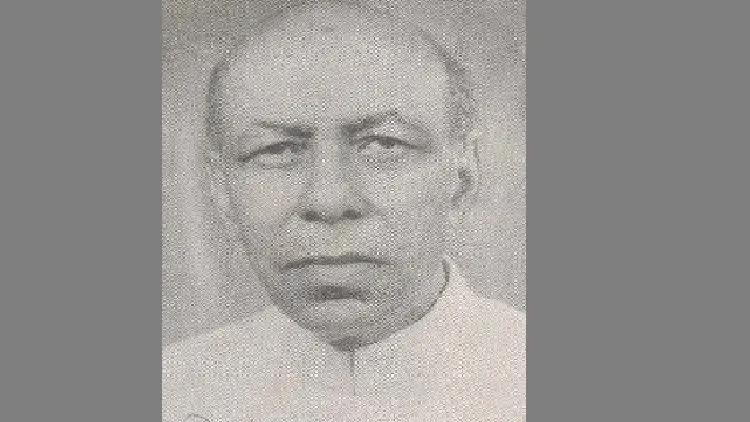
-ज़ाहिद ख़ान
तरक़्क़ीपसंद तहरीक से जो शायर इसकी इब्तिदा से ही जुड़े हुए थे, उनमें एक आला नाम मुईन अहसन जज़्बी का भी है. तरक़्क़ीपसंद शायरी के वे अलमबरदार थे. उनका नाम मजाज़, फै़ज़, मख़दूम और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे शायरों के साथ एहतिराम से लिया जाता था. अंजुमन तरक़्क़ीपसंद मुसन्निफ़ीन के क़याम से पहले ही वे अपनी मशहूर ग़ज़ल‘‘मरने की दुआएं क्यूं मांगू जीने की तमन्ना कौन करे’’ लिख चुके थे. इस ग़ज़ल ने उन्हें खूब शोहरत दी.
आलम यह था कि अपने जमाने में उनकी शायरी हसरत मोहानी से लेकर जिगर मुरादाबादी तक पसंद करते थे. जिगर मुरादाबादी ने तो उनको अपने बाद के दौर का अकेला शायर बतलाया था. खुद जज़्बी भी जिगर की शायरी के बड़े मद्दाह थे. उनकी शायरी में जो ज़बान की रवानगी दिखाई देती है, वह उन्होंने जिगर मुरादाबादी से ही सीखी है. जज़्बातियत, जज़्बी की शायरी की अहम शनाख़्त है. उन्होंने एक से बढ़कर जज़्बातियत और दर्द में डूबी ग़ज़लें लिखीं. ‘‘इंतिहा-ए-ग़म में मुझको मुस्कराना आ गया/हाथ इख़्फाए-मुहब्बत का बहाना आ गया.’’ वहीं नज़्म ‘ख़्वाब-ए-हस्ती’ में उनकी कैफ़ियत है, ‘‘वो ज़माने और थे जब तेरा ग़म सहता था मैं/जब तिरे होंटों की रंगीनी से कुछ कहता था मैं.’’
मुईन अहसन जज़्बी दरअसल रोमानी शायर थे. हुस्नो-इश्क़, जो ग़ज़ल की पहचान है, उस पर उन्होंने अनेक ग़ज़लें लिखीं. ग़ज़ल के यह ख़ूबसूरत अशआर भी उन्हीं के हैं,‘‘जब कभी किसी गुल पर जरा निखार आया/कम निगाह ये समझे कि मौसमे-बहार आया.’’ आशिक-माशूक की दिल-आवेज़ हरकतें, आपस में रूठना-मनाना, शिकवे-शिकायत जज़्बी की शायरी में हैं. गोकि उनकी शायरी में रंगीन-बयानी है, तो ख़ुश-लहज़ा भी है. उनका ये अंदाज देखकर, पढ़ने वालों को यकीन ही नहीं होता कि यह भी जज़्बी का कारनामा है.‘‘तुझ से नज़र मिला कर दीवाना हो गया मैं/कुछ राज़ बन गया कुछ अफ़्साना हो गया मैं.’’ अपनी एक दूजी ग़ज़ल में वे एलान करते हैं,‘‘अपनी निगाह-ए-शौक़ को रुस्वा करेंगे हम/हर दिल को बे-क़रार-ए-तमना करेंगे हम.’’ मुहब्बत की चाश्नी में डूबी उनकी इन ग़ज़लों के क्या कहने. उर्दू अदब में उन जैसे ग़ज़ल-सरा बहुत कम हुए हैं.
21 अगस्त, साल 1912 को सूबा उत्तर प्रदेश के मुबारकपुर, जिला आज़मगढ़ में जन्मे मुईन अहसन जज़्बी ने नौ-दस साल की मासूम उम्र से ही शेर-ओ-शायरी शुरू कर दी. उनकी इब्तिदाई तालीम मुबारकपुर में ही हुई. इंटर की तालीम के लिए वे जब आगरा के सेंट जॉन्स कालेज पहुंचे, तो वहीं उनकी पहली मुलाकात मजाज़ और ‘फानी’ बदायुनी से हुई. मैकश अकबराबादी से भी उनकी मुलाक़ातें रहीं. मजाज़ और ‘फानी’ बदायुनी की सोहबत और मैकश अकबराबादी की रहनुमाई में मुईन अहसन जज़्बी की शायरी बराबर संवरती-निखरती रही. जज़्बी की आगे की तालीम लखनऊ और दिल्ली में हुई. वे जब साल 1939 में लखनऊ पहुंचे, तो यह तरक़्क़ीपसंद मुसन्निफ़ीन का मरकज़ बना हुआ था.
अली सरदार जाफ़री और सिब्ते हसन से नजदीकियां बढ़ीं, तो वे भी तरक़्क़ीपसंद तहरीक से जुड़ गए. यहां तक कि अंजुमन तरक़्क़ीपसंद मुसन्निफ़ीन के सरगर्म मेंबर बन गए. जाफ़री और सिब्ते हसन के साथ उन्होंने अंजुमन के रिसाले ‘नया अदब’ में काम किया. अलीगढ़ में एम.ए. की पढ़ाई के दौरान प्रगतिशील लेखक संगठन में उनकी सक्रियता बनी रही. अलीगढ़ में उनके हमराह अली सरदार जाफ़री, मजाज़, सिब्ते हसन के अलावा जां निसार अख़्तर, ख़्वाजा अहमद अब्बास और हयातुल्लाह अंसारी आदि थे.
मुईन अहसन जज़्बी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ अरसे तक दिल्ली में मासिक पत्रिका ‘आजकल’ में अस्टिंट एडीटर के तौर पर खि़दमत दी. कुछ मुद्दत तक मुंबई रहे. मुईन अहसन ‘जज़्बी’ के स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू से बहुत अच्छे तआल्लुक थे. उन्हीं की पहल पर जज़्बी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में फैलोशिप मिली और उन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की. साल 1945 में वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गए और यहीं से रिटायर हुए.
उर्दू अदब में मुईन अहसन जज़्बी का आग़ाज़ धमाकेदार रहा. साल 1934 में लाहौर से छपने वाले मासिक रिसाले ‘हुमायूं’ में जब उनकी ग़ज़ल ‘‘मरने की दुआएं क्यूं मांगू’’ शाया हुई, तो इसने हंगामा कर दिया. ग़ज़ल खूब मक़बूल हुई. इतनी कि यह ग़ज़ल जज़्बी की पहचान बन गई. दर्द में डूबी इस ग़ज़ल के जज़्बात, हर नौजवान को अपने से लगे. ‘‘मरने की दुआएं क्यूं मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे/ये दुनिया हो या वो दुनिया अब ख़्वाहिश-ए-दुनिया कौन करे.’’ जज़्बी ने कम लिखा, मगर मानीखेज लिखा. उनके बेश्तर अश्आर और मिस्रे, मुहावरों का दर्जा रखते हैं. साल 1960 के बाद तो उनकी बहुत कम रचनाएं सामने आईं. शायरी में वे हमेशा इस बात के कायल रहे, जब तक शायरी अंदर से न आए, शायर के जज़्बात उसे लिखने पर मजबूर न करें, तब तक उस पर हाथ न आजमाया जाए.
मुईन अहसन जज़्बी की एक और ग़ज़ल ‘मौत’ भी काफी मक़बूल हुई. इस ग़ज़ल के फ़ै़ज़ भी मुरीद थे. यह लंबी ग़ज़ल है और इस ग़ज़ल का एक-एक शे’र नायाब है. आज भी इसको सुनने से अलग ही नशा तारी हो जाता है. ‘‘अपनी सोई हुई दुनिया को जगा लूं तो चलूं/अपने ग़मखाने में एक धूम मचा लूं तो चलूं.’’ जज़्बी उर्दू अदब की क्लासिकी रिवायत की नुमाइंदगी करते हैं. रवायती अल्फ़ाज, अलामात और इस्तिआरों को उन्होंने नये मायने दिए. उन्हें आगे बढ़ाया.
ग़ज़ल की रवायत से वाबस्ता रहते हुए सियासी मौजुआत को इस तरह पेश किया कि ग़ज़ल की खूबसूरती भी बरकरार रही और अपनी बात का इज़हार भी कर दिया. नज़्म की बजाय मुईन अहसन जज़्बी ने ग़ज़ल ही ज्यादा लिखी. उनकी इन ग़ज़लां में बला का हुस्न नजर आता है. मशहूर तंकीद निगार एहतेशाम हुसैन अपनी क़िताब ‘उर्दू-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’ में मुईन अहसन जज़्बी के कलाम के मुताल्लिक लिखते हैं,‘‘उनकी ग़ज़लें बेहद दिलचस्प और जज़्बात से लबालब होती हैं. वे इंसानी ग़म और दर्द को दुनियावी दर्द के तौर पर बड़े ही खूबसूरती से पेश करते हैं.’’
मुईन अहसन जज़्बी ने अपनी जिं़दगी के तजुर्बों से जो सीखा, उसे ही अल्फाजों में बयां किया है. उनकी शायरी में सिर्फ नाउम्मीदी और माज़ी के शिकवे-शिकायत ही नहीं है, मुस्तकबिल का एक ख़्वाब भी है. उम्मीद का एक चिराग है, जिसकी रोशनी पूरे जहां को मुनव्वर करती है. ‘‘ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी/शाम आई है तो आने दो सहर भी होगी.’’ दरअसल, अपनी पूरी जिं़दगानी में जज़्बी ने जो उतार-चढ़ाव देखे थे, वह तज़्किरा उनकी शायरी में बार-बार आता है. वे लोगों को इशारों-इशारों में कुछ बातों की तरफ आगाह भी करते हैं.
‘‘हम दह्र के वीराने में जो कुछ भी नजारा करते हैं/अश्कों की जुबां में कहते हैं, आहों में इशारा करते हैं.’’ ‘फ़रोज़ां’, मुईन अहसन जज़्बी का पहला ग़ज़ल का मजमुआ है, जो साल 1943 में शाया हुआ था. इस क़िताब की भूमिका में उन्होंने साफ लहजे में कहा है,‘‘तरक़्क़ीपसंदी को मार्क्सी नुक्त-ए-नज़र के सिवा कुछ और समझना सख्त गलती होगी. लेकिन यह नुक़्त-ए-नज़र आसानी से पैदा नहीं होता. एक चीज को समझना उतना दुश्वार नहीं, जितना उसे अपनी वैचारिक आस्था का अंग बनाना दुश्वार है. यह एक दिन का काम नहीं है.’’ ‘सुखन-ए-मुख़्तसर’ (साल 1960) उनकी ग़ज़लों का दूसरा मजमुआ है. साल 1985 में आई ‘गुदाज़े शब’ मुईन अहसन जज़्बी की आखिरी क़िताब है. उन्होंने शाइरी के अलावा आलोचना की कई अहम क़िताबें भी लिखीं. उर्दू अदब की बेमिसाल खि़दमत के लिए मुईन अहसन जज़्बी को कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाज़ा गया.
मुईन अहसन जज़्बी इंसानियत के बड़े पैरोकार थे. किसी भी आर्ट को सीखने के लिहाज से वह इसका होना बेहद ज़रूरी मानते थे. उनका मानना था,‘‘अच्छा आदमी ही अच्छा शायर हो सकता है. जिन लोगों में इंसानियत नहीं है, वे कोई बड़ा काम नहीं कर सकते.’’ यही नहीं क्रिएटिव आर्ट के मुताल्लिक उनके ख़याल थे,‘‘क्रिएटिव आर्ट का ताल्लुक आपके बिलीफ से है, आपके बिलीफ जितने स्ट्रांग होंगे, उतनी आपके क्रिएशन में झलक होगी. बिलीफ अच्छे होने से जिं़दगी भी अच्छी गुज़रती है. जितने आप नेकी की तरफ बढ़ेंगे, उतने ही आपके रिएक्शंस सही होंगे. ये रिएक्शंस आपके क्रिएशन में काम आएंगे.’’ यानी जो आदमी नेक नहीं है, उसमें इंसानियत-सच्चाई नहीं है, उसके आर्ट में भी वह असर पैदा नहीं होगा. न ही वह आर्ट किसी को मुतासिर कर पाएगा. वहीं उनके तईं ‘‘ग़ज़ल में थॉट, कंटेंट असल चीज है.’’ उनकी यह बात सही भी है. बिना विचार के बेहतर नज़्म निगारी, नस्र निगारी कुछ भी नहीं हो सकता.
मुईन अहसन जज़्बी ने दीगर तरक़्क़ीपसंद अदीबों की तरह आज़ादी की तहरीक में अपनी सक्रिय हिस्सेदारी की. अपने कलाम से वे अवाम को बेदार करते रहे. एक लंबे संघर्ष के बाद मुल्क को आज़ादी मिली, मगर उसके साथ ही वह दो हिस्सों में बंट गया. पार्टीशन को मुईन अहसन जज़्बी मुल्क की सबसे बड़ी ट्रैजिडी मानते थे. इस घटनाक्रम पर उन्होंने उस वक्त ‘तक्सीम’ के उन्वान से एक नज़्म भी लिखी थी, जो काफी चर्चित रही. ‘‘क्या यही इंक़िलाब है, कल्ब इधर, जिगर उधर/नाला ए-बेकरार इधर, शोरिशे-चश्मे-तर उधर.’’ 13 फ़रवरी, साल 2005 को मुईन अहसन जज़्बी इस दुनिया से अलविदा कह गए. जज़्बी की दिली तमन्ना थी कि उनकी कुल्लियात उनके ज़ीते-जी छप जाए.
लेकिन अफ़सोस, वह हो न सका. जज़्बी के इंतिकाल के बाद साहित्य अकादमी, दिल्ली ने उनके सारे अदब को ‘कुल्लियात-ए-जज़्बी’ के नाम से शाया किया. इस कुल्लियात में ‘गुदाजे-शब’ के बाद लिखे गये उनके तमाम कलाम के अलावा कुछ अप्रकाशित रचनाएं भी शामिल हैं. कुल्लियात का अंग्रेजी तर्जुमा भी हो गया है. मुईन अहसन जज़्बी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था,‘‘यदि किसी की शायरी उसकी मौत के पचास साल बाद तक जिं़दा रह जाती है, तो मान लें कि वह शायरी है और शायर बड़ा है.’’ उनकी ग़ज़ल ‘‘मरने की दुआएं क्यों मांगू’’ साल 1934 और ‘‘अपनी सोई हुई दुनिया को जगा लूं’’ साल 1941 में आइंर् थी. इन ग़ज़लों को आये हुए आठ दशक से ज्यादा हो गए, मगर आज भी यह ग़ज़ल उसी तरह मकबूल हैं. इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मुईन अहसन जज़्बी अज़ीम शायर थे और उनकी शायरी माया-ए-नाज़ है.
