नई दिल्ली,
बड़े पर्दे पर शोले को देखना—गब्बर का खौफनाक अंदाज़ में “कितने आदमी थे” कहना, ट्रेन पर जय-वीरू की धुआंधार लड़ाई और ठाकुर बलदेव सिंह के दिल में सुलगती बदले की आग—सिनेमा के उस जादू को फिर से जीना है, जिसने पीढ़ियों को बांध रखा है। रमेश सिप्पी की यह कालजयी फिल्म अब अनकट संस्करण में सिनेमाघरों में लौटी है, वह भी 70 एमएम अनुभव के साथ—जहां ध्यान भटकाने को कुछ नहीं, सिर्फ परदे पर बहता सिनेमा।
इस बार कहानी का मूल क्लाइमैक्स भी है—वह अंत, जिसे आपातकाल के दौर में सेंसर बोर्ड के दबाव में बदला गया था। अब ठाकुर (संयमित अभिनय में संजीव कुमार) गब्बर को नहीं बख्शते; वह बदला पूरा करते हैं। अमजद ख़ान के विस्फोटक गब्बर का यह अंजाम दर्शकों को वर्षों बाद ‘क्लोज़र’ देता है—वह एहसास कि जो अधूरा था, वह पूरा हुआ।
पचास साल बाद भी ‘शोले’ हर उम्र के दर्शक को कुछ न कुछ देता है। थिएटर में एक ही साथ तीन पीढ़ियां—दादा-दादी, माता-पिता और बच्चे—हंसते, तालियां बजाते और संवाद दोहराते दिखते हैं। किसी के लिए यह पहली थिएटर मेमरी है, किसी के लिए टीवी/VHS/DVD पर देखी गई यादों का जीवंत रूप। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और गब्बर—सब फिर से बड़े परदे पर सांस लेते हैं।
फिल्म देखते हुए वही परिचित लम्हे लौटते हैं—आर.डी. बर्मन का गिटार-प्रधान बैकग्राउंड स्कोर, गब्बर का “वो दो और तुम तीन”, जय की शहादत पर नम आंखें। पर साथ ही दिखता है एक सांस्कृतिक स्मृतिलो—गांव की साझा ज़िंदगी, अज़ान की आवाज़, होली का जश्न, वह भारत जहां सामूहिकता रोज़मर्रा का सच है।
अनकट संस्करण में जोड़े गए कुछ छोटे मगर असरदार दृश्य—इमाम साहब के बेटे अहमद की हत्या, ठाकुर के जूतों में ठोंकी जाती कीलें, घोड़े पर सवार वीरू का एक डकैत को रस्सी से घसीटना—दर्शक फौरन पहचान लेते हैं। यही ‘शोले’ की दीवानगी है। छोटे किरदार भी अमर हैं—सांभा का “पूरे पचास हज़ार”, कालिया, हरिराम नाई, इमाम साहब—सब यादों में जिंदा।
हॉल के बाहर और भीतर ‘शोले’ ट्रिविया गूंजता है—गब्बर के पिता का नाम? ‘ये दोस्ती’ में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर? जवाब भी फौरन मिलते हैं। यह फिल्म सिर्फ बदले की कहानी नहीं; यह दोस्ती, प्रेम, नैतिकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का भारतीय पाठ है।
जब अंत में जय पूछता है—“ये कहानी तो नहीं भूलेगा न?”—थिएटर का सामूहिक जवाब आज भी वही है: नहीं। पचास साल हो गए, और ‘शोले’ अब भी उतना ही जिंदा है।












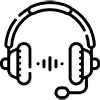
.webp)
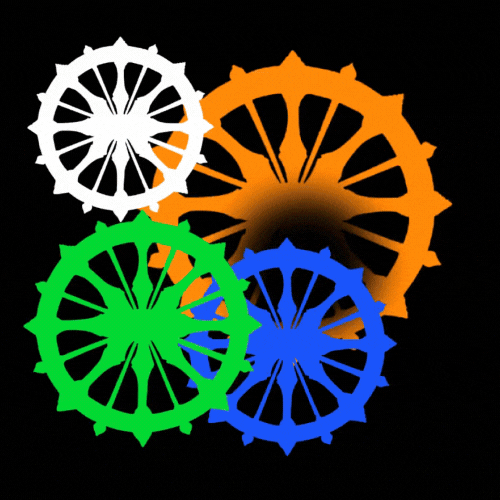
.jpg)



.webp)
.webp)
.webp)

.png)





