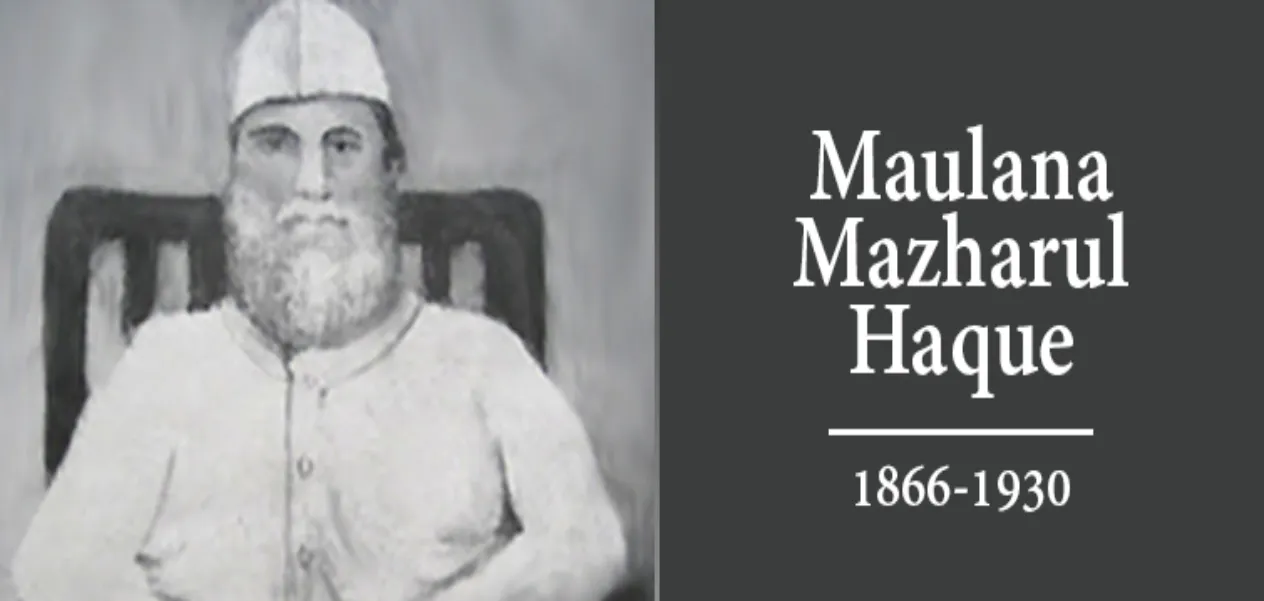
साक़िब सलीम
भारत के स्वतंत्रता इतिहास में 1917 का चंपारण सत्याग्रह वह मोड़ है जहाँ महात्मा गांधी पहली बार जन-आधारित राष्ट्रवादी राजनीति के अखिल भारतीय नायक के रूप में उभरे. परंतु इतिहास की सुर्ख़ियों ने धीरे-धीरे उस व्यापक मानवीय और संगठनात्मक ताने-बाने को धुंधला कर दिया जिसने इस आंदोलन को आकार दिया था. उन चुप पड़ गए नामों में सबसे महत्वपूर्ण है मौलाना मज़हरुल हक़—वह पुल जिसने दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी को बिहार की धरती, वहाँ के किसानों, स्थानीय नेतृत्व और राष्ट्रीय राजनीति की धड़कन से जोड़ा.
सच तो यह है कि चंपारण सत्याग्रह और मज़हरुल हक़ को अलग-अलग पढ़ना, इतिहास को अधूरा पढ़ना है.गांधी ने स्वयं लिखा कि मज़हरुल हक़ उन भरोसेमंद मददगारों में थे जिन पर वे हमेशा निर्भर कर सकते थे; वह महीने में एक-दो बार ज़रूर मिलते और जिस आत्मीयता से जुड़े रहते, उससे लगता था मानो वे हममें से ही एक हों.
हालाँकि उनकी आधुनिक, परिष्कृत जीवन-शैली किसी अनजान पर अलग छाप छोड़ती थी. यह टिप्पणी सिर्फ़ निजी स्नेह का नहीं, बल्कि राजनीतिक भरोसे का प्रमाण भी है.
चंपारण के साथ गांधी का रिश्ता राजकुमार शुक्ल और पीर मुनीस के सतत आग्रह से बना, पर बिहार की धरती पर उतरते ही जो पहला ठोस सहारा मिला वह था पटना निवासी मज़हरुल हक़.
गांधी उन्हें पहले से पहचानते थे—लंदन के दिनों से, जब हक़ बार-at-law की पढ़ाई कर रहे थे. 1915 की बॉम्बे कांग्रेस में, उस साल जब हक़ मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे, यह परिचय फिर से जीवित हुआ। यही पुराना भरोसा 1917 में ऐतिहासिक ठहरा.
नील की खेती से जुड़े शोषण, जबरी करारों और औपनिवेशिक दमन से त्रस्त चंपारण के किसान वर्षों से प्रतिरोध कर रहे थे. शेख गुलाब, शीतल राय, राजकुमार शुक्ल और पीर मुनीस जैसे स्थानीय नेताओं ने इस दुख को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने की कोशिश की.
अंततः गांधी ने किसानों से मिलने का निश्चय किया और 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुँचे. वहाँ वे शहर में केवल एक व्यक्ति को जानते थे—मज़हरुल हक़.
गांधी ने लिखा कि हक़ ने पहले ही उन्हें आमंत्रित किया था कि पटना आएँ तो उन्हीं के साथ ठहरें। यात्रा का उद्देश्य बताने वाला गांधी का पत्र मिलते ही हक़ स्वयं कार लेकर पहुँचे, आग्रह किया कि वे उनके अतिथि बनें; गांधी ने विनम्र धन्यवाद दिया और उनसे बस यह निवेदन किया कि उन्हें जल्द-से-जल्द गंतव्य के लिए ट्रेन पर बैठा दें—क्योंकि अपरिचित प्रदेश में रेलवे गाइड उनके किसी काम का नहीं था.
हक़ ने तत्काल राजकुमार शुक्ल से विचार विमर्श कर सलाह दी कि गांधी पहले मुज़फ्फ़रपुर जाएँ; उसी शाम की ट्रेन पकड़ी गयी और वहीं से चंपारण यात्रा का व्यावहारिक मार्ग खुला.
संगठनात्मक समर्थन की यह पहली कड़ी थी. आगे घटनाएँ तेज़ हुईं। 16 अप्रैल 1917 को मोतिहारी में गांधी को पुलिस द्वारा पहला नोटिस थमाया गया. यह नागवार चेतावनी ब्रिटिश राज की बौखलाहट दर्शाती थी.
इस समय मज़हरुल हक़ और मदन मोहन मालवीय उन दो प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में थे जिन्हें तुरंत संदेश भेजा गया. हक़ स्वयं मोतिहारी पहुँचना चाहते थे, पर उन्हें पटना में बने रहकर राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चों पर समन्वय करने की सलाह दी गई—क्योंकि वे कई प्रभावशाली पदों पर थे और उनकी रणनीतिक भूमिका निर्णायक थी.
चंपारण सत्याग्रह अचानक नहीं, बल्कि योजनाबद्ध सामूहिकता से आकार लिया. जीवनीकार डी. जी. तेंदुलकर लिखते हैं कि 18 अप्रैल को मज़हरुल हक़, ब्रजकिशोर बाबू, राजेंद्र बाबू (भविष्य के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद), बाबू अनुग्रह नारायण, शंभू शरण और पोलक मोतिहारी पहुँचे.
लंबी सलाह-मशविरा के बाद निर्णय हुआ कि आवश्यकता पड़ने पर ये सभी गांधी के साथ जेल जाने को तैयार रहेंगे. गांधी ने तुरन्त क्रम तय कर दिया: पहले हक़ और ब्रजकिशोर; फिर धामीधर और रामनवमी प्रसाद; उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, शंभू शरण और अनुग्रह नारायण.
संदेश स्पष्ट था—नेतृत्व गिरफ़्तार हो जाए तो भी किसान आंदोलन न टूटे. इस रणनीति के अनुरूप हक़ और ब्रजकिशोर अपने-अपने निजी मामलों को निपटाने पटना और दरभंगा लौटे ताकि 21 अप्रैल तक संघर्ष-स्थल पर वापस आ सकें.
इस बीच, वायसराय की विधान परिषद के सदस्य होने के नाते मज़हरुल हक़ ने चंपारण में unfolding घटनाओं की रिपोर्ट टेलीग्राम से वायसराय को भेजी—यह सूचना-राजनीति औपनिवेशिक प्रशासन पर नैतिक दबाव बनाने का एक सूझबूझ भरा तरीका था.
2 जून को पटना में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में, जहाँ अनेक कांग्रेस नेता उपस्थित थे, गांधी ने फिर स्पष्ट किया: अगर उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है तो चंपारण का किसान आंदोलन मज़हरुल हक़ के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा.
यह उद्घोष उन्हें आंदोलन की उत्तरदायी रीढ़ के रूप में स्थापित करता है. गांधी जानते थे कि किसान-आधारित जन-प्रतिरोध को टिकाए रखने के लिए धार्मिक-सामुदायिक सीमाओं को पार करता हुआ नेतृत्व अनिवार्य है—और हक़ उसकी जीवित मिसाल थे.
औपनिवेशिक अभिलेख इस साझेदारी को लेकर असहज थे. तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त एल. एफ. मोरशेड ने 19 अप्रैल 1917 को बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आशंका जताई कि मज़हरुल हक़ चाहते हैं गांधी जेल जाएँ—क्योंकि ऐसा होने पर देशव्यापी जनभावना भड़क उठेगी.
27 अप्रैल को बेतिया राज के प्रबंधक जे. टी. व्हिट्टी ने मोरशेड को लिखा कि गांधी की जाँच वस्तुतः इस प्रांत के ‘यूरोप-विरोधी तत्वों’ का संगठित प्रयास है; उनकी नज़र में गांधी ईमानदार हो सकते हैं.
पर दक्षिण अफ्रीका की सफलता ने उन्हें ‘थोड़ा गर्वित’ बना दिया है—और यही कारण है कि मज़हरुल हक़, हसन इमाम और ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे नेता उन्हें अपने उद्देश्य के लिए अत्यंत उपयोगी मानते हैं: निडर, अडिग, और जनता में लोकप्रिय; जिन्हें शहीद बनाना आसान और दबाना कठिन। औपनिवेशिक नज़रिए की यह बेचैनी इस तथ्य की गवाही है कि बहु-धर्मी, बहु-जातीय राष्ट्रवादी गठबंधन ब्रिटिश राज के लिए वास्तविक चुनौती बन चुका था.
यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि मज़हरुल हक़ कोई परिधि का चरित्र नहीं थे. वे बिहार के अग्रणी राष्ट्रवादी, प्रख्यात बैरिस्टर, शिक्षाविद, और सार्वजनिक जीवन के ऊर्जावान व्यक्तित्व थे.
लंदन की पढ़ाई ने उन्हें वैश्विक दृष्टि दी; कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मंचों पर उनकी सक्रियता ने भारतीय राष्ट्रवाद की समावेशी रेखा को मज़बूती दी। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा के अनुसार, जब कुछ कुलीन भारतीय मुसलमान ब्रिटिश समर्थक संगठन गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब हक़ ने उसका विरोध किया और सुनिश्चित किया कि प्रारंभिक मुस्लिम लीग संविधान में सरकार को बिना शर्त समर्थन देने जैसी कोई बात न लिखी जाए.
यह रुख़ आगे चलकर हिंदू-मुस्लिम सहयोग की ज़मीन तैयार करने में सहायक हुआ—वही सहयोग चंपारण की साझा राजनीति में चमका.फिर भी, सार्वजनिक स्मृति ने समय के साथ गांधी को तो राष्ट्रीय प्रतीक बनाया पर मज़हरुल हक़ जैसे सहयात्रियों को धुंधला कर दिया.
यह विस्मरण केवल व्यक्तियों का अन्याय नहीं; यह हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की बहुस्तरीय, बहुधर्मी प्रकृति को भी खोखला कर देता है. जब हम कहते हैं कि चंपारण ने गांधी को भारत का महात्मा बनाया, हमें उसी साँस में यह भी स्वीकारना चाहिए कि मज़हरुल हक़ ने गांधी को बिहार की धरती पर घर दिया, किसानों तक पहुँच दिलाई, राजनीतिक कवच दिया और नेतृत्व की रिले दौड़ की योजना बनाई—ताकि दमन की किसी भी चाल के बावजूद आंदोलन जीवित रहे। एक अर्थ में, उन्होंने उस परिस्थिति को संभव बनाया जिसमें गांधी महात्मा बनकर उभर सके.
आज, जब इतिहास के नाम पर विभाजनकारी आख्यान गढ़े जा रहे हैं, मज़हरुल हक़ की भूमिका को फिर से पढ़ना समय की मांग है. चंपारण सत्याग्रह की कथा हमें सिखाती है कि भारत का स्वाधीनता अभियान किसी एक महापुरुष का एकांकी अभिनय नहीं था; यह साझा संकल्प, साझी पीड़ा और साझी नैतिकता की सामूहिक पटकथा थी. उस पटकथा में मौलाना मज़हरुल हक़ की स्याही अब भी गीली है—बस हमें पन्ना फिर से पलट कर पढ़ना होगा.
